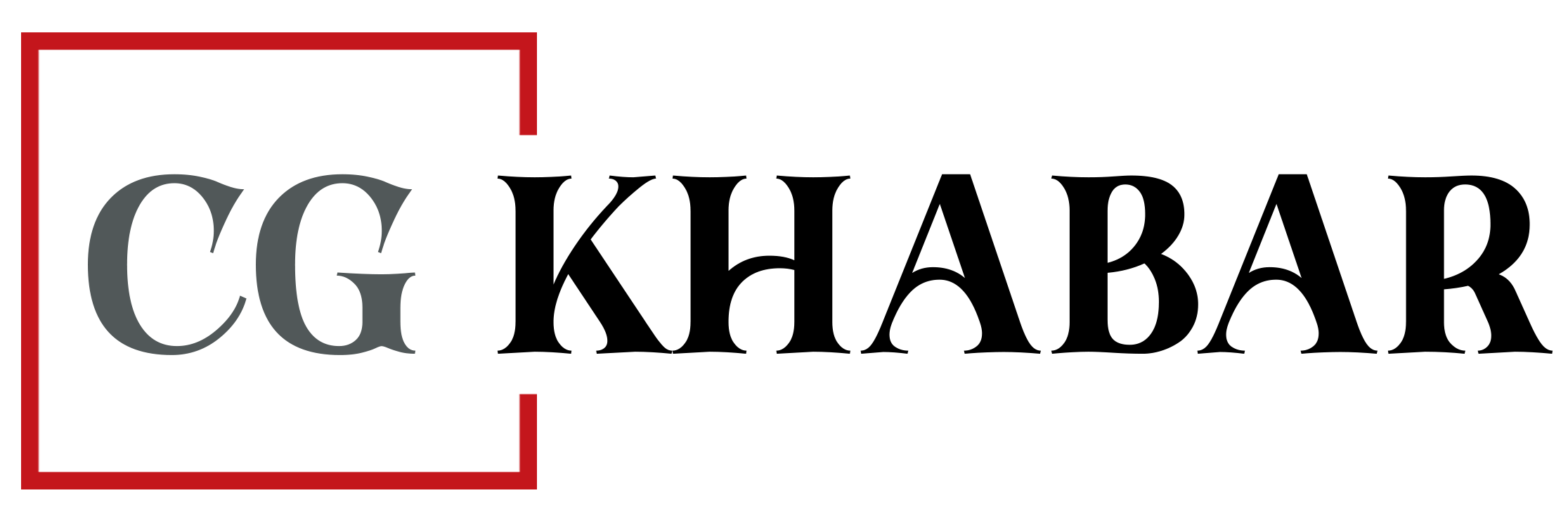इस mediocrity को पहचानते हैं आप?
डॉ. विक्रम सिंघल
पिछले सप्ताह राहुल गाँधी के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के भाषण में राजनीतिक चिंतन की एक झलक दिखाई दे रही है. यूं भी असाधारण समय में असाधारण हल ढूंढ़ने पड़ते हैं. भारतीय राजनीति जिस स्थिति में फँसी हुई है, उससे सामान्य राजनैतिक प्रक्रियाओं और प्रबंधन से नहीं निकला जा सकता. अक्सर जब कोई व्यवस्था लम्बे समय तक अपनी समस्याओं से बच कर निकलने की कोशिश करता रहता है तो छोटे-छोटे समझौते जुड़ते हुए, एक समय उसे पूरी तरह अपने रास्ते से दूर कर देते हैं और उसे निरर्थक बना देते हैं. हमारे राजतंत्र के साथ भी यही हुआ है.
अपनी सामाजिक विसंगतियों और औपनिवेशिक अवशेषों के बोझ को ढोते हुए एक संविधान और राजतंत्र का निर्माण किया गया और अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भरोसा जताते हुए, एक राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया गया. एक प्रबुद्ध और सत्यनिष्ठ नेतृत्व अपने समय के लिए तो ऐसे निर्णय ले सकता है लेकिन भविष्य पर इतनी आस्था कि वो उन समझौतों के पीछे की भावना को समझेंगे और लगातार उन विसंगतियों पर काम करेंगे, यह कई बार ऐसे ही
फलीभूत होती है.
बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान सभा को चेताया था कि वे जिस देश और समाज पर एक आधुनिक और नैतिक संविधान प्रेषित कर रहे हैं, शायद वह उसके लिए तैयार नहीं है और शायद गाँधी के सभी विरोधी, गाँधी की अपने देशवाशियों के नैतिक क्षमता पर दिखाए गए अद्वितीय विश्वास से सहमत नहीं थे वो खुद पर भी ऐसा बोझ लादना नहीं चाहते थे कि वो लोगों को उन उच्च संवैधानिक मूल्यों के पालन के लिए प्रोत्साहित करें.
राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आज हमारे देश में ऐसे लोग हैं, जो खुद को हर विषय का ज्ञाता मानते हैं. यहाँ तक कि यदि उनका सामना हो तो भगवान को भी ब्रम्हांड की संरचना पर सीख देना शुरू कर देंगे. इसमें सबसे पहला नाम हमारे प्रधानमंत्री का है.
ये अपने आप में विनोद और हास्य भाव में कहा गया लग सकता है पर उन्होंने इसके बाद जो कहा, वह हमारे वर्तमान का कार्य-कारण, दोनों का परिचायक है. उन्होंने कहा कि इसके जड़ में है ‘mediocrity’. यानी एक प्रवृत्ति, जो सुधार, उत्तमता, दक्षता इन सब से अनिभिज्ञ हो, अपने को एक स्थूल स्थायी जड़ अवस्था में ले जाये. ये अपने वातावरण और प्रकृत्ति में व्याप्त उन्नत और श्रेष्ठ तत्वों का संज्ञान नहीं लेते और स्वयं को संपूर्ण और श्रेष्ठ घोषित कर देते हैं.
भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर राहुल गांधी ने इसे कई व्यावहारिक पक्षों में परिभाषित किया. पहला आयाम है सुनने की कला का. इसके लिए अपने अहं को शून्य कर, सामने खड़े व्यक्ति के सच को स्थान देना और दूसरी परिभाषा थी बल और शक्ति में अंतर. जिसमें शक्ति सत्य का बिम्ब मात्र होता है और बल वह अवरोध है, जो सत्य के विस्तार को रोक कर ‘mediocrity’ को संरक्षित करती है.
ये दोनों परिभाषाएं इस स्वीकृति से विकसित होती हैं कि सत्य, जन, ज्ञान और शक्ति एक ही हैं. इसीलिए किसी के लिए भी सभी लोगों का, सभी ज्ञान का और सम्पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है. यह तभी संभव है, जब सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाए. शायद इसी को गांधीजी समुद्री तरंगों का विस्तार कहते थे. और यह तभी संभव है जब सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाये, शायद इसी को गांधीजी समुद्री तरंगों का विस्तार कहते थे. वे चाहते थे कि उनके घर में हर दिशा से हवाएं बहती हुई आएं.
यही वह नेतृत्व था, जिसने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्योंकि वह प्रगतिशील, ज्ञान के लिए प्रयासरत था और ‘mediocrity’ से ग्रसित नहीं थी. वह महायान थी, जो सब को अज्ञान के उस अँधेरे से सत्य की और ले जाना चाहती थी.
‘mediocrity’ से निगमित होता है संशय, भय, और घृणा. इसका एक रूप स्वयंमात्रावाद भी है, जिसे अंग्रेजी में ‘solipsism’ कहते हैं. यह विस्तृत होकर उग्र राष्ट्रवाद का निर्माण करती है और पूरे राष्ट्र को ही इस भंवर में खींच लेती है. कुछ साल पहले अरुंधति राय ने कहा था कि मोदी काल का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि पुरे राष्ट्र की सामूहिक बौद्धिकता का ह्रास हो गया है.
इस संशय ग्रस्त, भयभीत और घृणा से भरी mediocrity को किसी भी प्रकार के बल से प्रभावित करना बड़ा आसान है. चाहे बड़ी पूंजी का बल हो, या तंत्र का. स्वयं में सिकुड़ते इस चेतना को प्रश्न पसंद नहीं है. लेकिन इन सब के बीच सत्य अनवरत खड़ा है- ढका हुआ, नकारा हुआ पर सत्तावान. यहाँ से निदान के प्रश्न उभरते हैं.

राहुल ने रोग के लक्षण और कारण तो पहचान लिए हैं और शायद उपचार पर भी कोई योजना बनाई होगी पर उसकी औषधि की उपलब्धता पर विचार करना होगा.
दो
2010 में ESPN में प्रकाशित क्रिकेट से जुड़े एक लेख ‘Let’s give mediocrity its due‘ को पढ़ते हुए, पहली बार मेरा ध्यान इस ओर गया था. आनंद रामचंद्रन के इस लेख ने बेहद साधारण तरीके से, बहुत बड़ा सवाल उठाया था, जो उस वक़्त बचकाना लग रहा था.
इस लेख में सवाल था कि सभी बड़ी टीमें, जैसे भारत या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में कुछ औसत दर्जे के खिलाडी होते हैं, जिन्हें अपने समय के महान खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतार दिया जाता है क्योंकि सर्वोच्च स्तर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और घरेलू आयोजनों के बीच में और स्तरों के आयोजन नहीं होते, जहाँ ये औसत या यूँ कहें कुछ कम प्रतिभाशाली खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें.
लेख में इस बात को रेखांकित किया गया था कि शायद ये सामने वाली टीम से ज्यादा, अपनी टीम के उन बेहतर खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हैं क्योंकि तुलना तो उन्हीं से है और टीम में जगह के लिए भी यही देखा जायेगा. तर्क ये था कि अगर उम्र के आधार पर और लिंग के आधार पर आयोजन हो सकते हैं ताकि “लेवल प्लेइंग फील्ड” मिल सके तो फिर योग्यता के आधार पर क्यों नहीं? आखिर खेल का रोमांच तो बराबरी की टक्कर देखने में ही तो है! इससे आगे तो केवल देश या टीम का गौरव है, खेल नहीं.
यह बड़ा प्रश्न है और न्याय की अवधारणा से जुड़ा प्रश्न है. न्याय होता है समान लोगों के साथ समानता और असमान लोगों के साथ असमानता का व्यव्हार करना. सब को एक ही तराजू से तौलना न्याय नहीं, अन्याय है. अब इसका अर्थ दोतरफा है. या तो यह कि कमजोरों का पक्ष लिया जाये या यह कि शक्तिशाली को वरीयता मिले.
दूसरी अवधारणा कहती है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को उसके सर्वोच्च अर्थ तक पहुंचा सके, उस वस्तु पर उसी का अधिकार होता है. इसे यूं समझें कि खेत के सही अर्थ को सार्थक करता है किसान. उस पर अपनी मेहनत से फसल उगा कर. इसलिए खेत पर किसान का अधिकार होना चाहिए, न की जमींदार का.
यह अवधारणा गुण और श्रम से अधिकारिता के सृजन का है. इसके अनुसार खेल को सार्थक बनाने वाली श्रेष्ठ प्रतिभाओं को ही खेलने का अधिकार है. यह श्रेष्ठता का वर्चस्व स्थापित करता है.
तीसरी अवधारणा सर्वाधिक स्थापित और मान्य है. इसे ‘डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस’ या वित्रात्मक न्याय कहते हैं और इसके प्रतिपादक जॉन रॉल्स थे. यहाँ सामान अवसरों की बात होती है. इसके अनुसार प्रतिभा इस प्रदर्शन का आंकलन, अवसरों की समानता के बाद ही करना चाहिए.
सामाजिक न्याय की भी मुख्य दलील यही है कि सामाजिक असमानता से समान अवसर नहीं मिलते, इसलिए समान प्रतियोगिता नहीं हो सकती. वही “लेवल प्लेइंग फील्ड”, अब तो सभी न्याय के पथ पर हैं. कुछ खुद को अलग मानकर अलग वरीयता मांगते हैं, कुछ अपने प्रदर्शन का वस्तुनिष्ट मूल्यांकन मांगते हैं या यूँ कहें कि ‘मूल्य तटस्थ’ मूल्यांकन,
कुछ और हैं, जो सामाजिक, ऐतिहासिक, या अपने पूरे चेतन अस्तित्व की असमानता की भरपाई मांगते हैं. ऐसे सभी लोगों के भीतर यह धारणा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, या यह कि उनके साथ अन्याय की कोशिश या साज़िश की जा रही है. यही राजनीति का आधार है.
यहाँ तक की बहस तो स्थापित है और सर्वमान्य भी. इन तीनों समूहों के अपने-अपने वर्ग हैं, और उन्हें अपने वर्गों का संरक्षण और अलग-अलग स्तर पर बौद्धिक वैधता और सहानुभूति भी प्राप्त है. हमारी बहस इसके आगे की है.
जिन खिलाड़ियों के लिए आनंद रामचंद्रन ने यह लिखा था, वो ऐसे किसी वर्ग का दावा नहीं कर सकते थे. न तो उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त था, जैसे कि राजसाहेब का कप्तानी पर अधिकार सिद्ध है, चाहे उनके रनों की संख्या उनके रोल्स रॉयस की संख्या से कम हो. न ही ये किसी महान नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे, और ना ही किसी प्रकार के शोषण या विभेद के शिकार थे. इनके लिए न तो वैसी वैधता थी और न ही सहानुभूति. इनकी आत्मछवि क्या होगी, ये खुद को क्या समझाएं कि उनका न्यायोचित स्थान और अधिकारिता क्या है?
कुछ साल पहले FTII पुणे के छात्रों ने अपने नए निदेशक के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई महीनों का संघर्ष भी कि वो तो ‘सी ग्रेड’ फिल्मों के अभिनेता थे. नए निदेशक ने पलट कर पूछा कि ‘सी ग्रेड’ फिल्मों के लोगों के लिए क्या कोई स्थान नहीं है? वो कहाँ जाएँ और उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो?
यह निरंतर द्वन्द ऐसे लोगों या वर्ग को कटु और ‘नाइलीस्ट’ या शून्यवादी (बौद्ध मत से अलग) बना देता है. उन्हें लगता है कि समाज, व्यवस्था, तर्क, ज्ञान सभी कुछ उनके विरुद्ध है. वो इन सब को ख़ारिज कर देना चाहते हैं. “एंग्री यंग मैन” का किरदार ऐसे ही तो सुपर हिट फिल्मों का स्वयसिद्ध मंत्र नहीं बन गया.
हालाँकि हाल के वर्षों में आर्थिक उदारीकरण ने सपनों को बेचने की कोशिश की है लेकिन उसका असर भी उतर रहा है.
अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गाँधी सिविल परीक्षाओं के कुछ अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे. राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या वो जानते हैं कि सिविल सेवाओं के कुल पद, प्रतिभागियों की संख्या के अनुपात में 1% से भी कम होते हैं. ऐसे में शेष 99% क्या करेंगे? क्या वो अपने ऊपर उम्र भर, विफलता का भार लिए घूमेंगे? उनके पास न तो अपने लिए कोई उत्तर होगा और न ही परिवार के लिए. समाज से तो वैसे ही अलगाव पैदा हो जाता है. ये अलगाव मार्क्स के अलगाव से अलग है या नहीं यह कहना मुश्किल है पर अलगाव शायद एक ही भाव है, उसके कारण और रुप अलग हो सकते हैं.
उन खिलाडियों की तरह ये भी कुछ ही अंक नीचे थे. क्या ‘न्याय’ कभी उनके साथ न्याय कर सकेगा. या फिर कोई न्यायोत्तर नैतिक चिंतन की आवश्यकता होगी. व्यक्ति की विशिष्टता और अधिकारिता, क्या कभी इस गुत्थी को सुलझा पायेगी. क्योंकि, न्याय तो परस्पर प्रतिस्पर्धा में युक्त अस्मिताओं और सिद्धांतों के बीच होता है. इसमें तो हार और जीत होती है.
बहरहाल, ये तो समाधान से जुड़े सवाल हैं. अभी तो हम इस समस्या के विश्लेषण की दिशा में हैं. ‘mediocrity’ का जड़त्व, स्वयंमात्रवाद, भय और घृणा; क्या हमें अभी भी तर्कहीन और अज्ञेय प्रतीत हो रहे हैं? क्या यह चेतना का ऐसा भाग है जहाँ तक ज्ञान मीमांसा की पहुँच नहीं है? अब हार और जीत का फलितार्थ क्या हैं?
जीत आपको पद, प्रतिष्ठा और सफलता तो देती ही है, पर आपको अपनी क्षमता पर, अपने स्वामित्व पर और अपने निर्णय के अधिकार पर विश्वास देती है. यही अधिकार, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व बनकर आता है और नैतिक स्वायत्ता लाता है, लेकिन हार, अविश्वास, पराधीनता और कर्त्तव्य विमुखता ले कर आती है. चेतना जड़ हो जाती है, नैतिक निर्णयों से स्वयं को अलग कर लेती है; मानवीय गरिमा से परितक्त्य.
क्या हमने कभी सोचा है कि इतिहास और मिथक दोनों ही विजेता की विजय गाथा कहते रहते हैं, यहाँ तक कि लोक कथाएं भी. उस पराजित की बात कौन करेगा? उस सामूहिक चेतना तक हमारी ज्ञान और स्मृति भी नहीं पहुँचते. उससे हमारा कोई संवाद ही नहीं होता. बिना संवाद के ये चेतना और सिकुड़ती चली जाती है.
शायद ‘प्रेत’ योनि की संकल्पना यही है. जहाँ न वर्तमान है और न ही भविष्य, केवल भूत काल और उसमें जीने की बाध्यता. समय की धारा से मुक्त, एक अभिशप्त भूत में सीमित. नर्क से कहीं भयावह है यह स्थिति.
इस ‘mediocrity’ का यदि कोई आह्वान कर सके, कोई आवाज़ जो उस तक पहुँच जाये, जिसे अंदाज़ा हो उस शून्य (निहिलिस्म) के ताक़त का, जिसे विध्वंश का भय नहीं है. इतिहास में ऐसी कहानियों की कमी नहीं है. हिटलर ने हारे हुए जर्मन चेतना का आह्वान किया. रावण ने, तारकासुर ने, देवासुर संग्राम के पराजितों का आव्हान किया.
समय यहाँ बेमानी है. पीढ़ी दर पीढ़ी यह चेतना अपने उद्धार और मुक्ति (रिडेम्पशन) के लिए उसी हार की ओर देख रही है. उसे भविष्य को नहीं, भूत को जितना है. राहुल जब कहते हैं कि इस सब के आधार में ‘mediocrity’ है, तो वो इसे समझते हैं. उस आसुरी नेतृत्व को भी, जो इसका आह्वान करती है और उस पीड़ा को भी, जो इसे सह रही है.