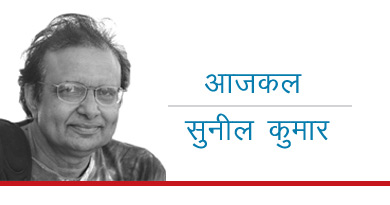सूक्तियों से मिले साहस
सुनील कुमार
बहुत से अखबारनवीसों से लेकर अखबारों में हर हफ्ते कॉलम लिखने वालों तक और सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या विचार के लिए अभियान चलाने वालों तक, कलम के सिपाहियों से लेकर कलम के भाड़े के हत्यारों तक, इनका हौसला थकता ही नहीं है. वे पूरे वक्त अपने मकसद के लिए, या कि अपने रोजगार के लिए जुटे रहते हैं, और ऐसा करते हुए वे सच और झूठ का फर्क करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते.
जब हिटलर के सूचना मंत्री से लेकर अब तक यह माना जाता है कि एक झूठ को अगर काफी बार दुहरा दिया जाए, तो वह सच में तब्दील होने लगता है, या कम से कम सच का एहसास तो कराने लगता है. नतीजा यह है कि लोग सोचे-समझे, मकसद भरे झूठ को बार-बार दुहरा कर उससे सच बनाने में लगे रहते हैं. लोग झूठ को पकड़ भी लेते हैं, तो भी उन्हें शर्म नहीं लगती, क्योंकि वे शर्मिंदगी के हकदार अकेले नहीं रहते, और उनकी तरह और बहुत से लोग इसी काम में लगे रहते हैं.
लेकिन सच के बारे में यह कहा जाता है कि उसे अपने अस्तित्व को साबित करने में देर लगती है, खासी देर लगती है, बड़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन फिर भी वह साबित तो हो ही जाता है, और आखिर में वह खड़ा रहता है. सवाल यह है कि यह खासी देर कितनी लंबी होती है, और इस बीच में झूठ की फसल जंगल की घास की तरह कितनी फैल चुकी रहती है, और आम लोग उस घास में कितने उलझते चलते हैं, उसके आरपार सच को देखने में उन्हें कितना वक्त लग जाता है, ये तमाम बातें परेशान करती हैं.
फिर दूसरी बात यह भी कि झूठ का कारोबार करने वालों के पास झूठों की फौज की एक वर्दी भी होती है, और टोली की ताकत भी. ऐसी गिरोहबंदी के मुकाबले सच बोलने वाले अक्सर किसी हमलावर मकसद के बिना होते हैं, उन्हें किसी वर्दी की ताकत भी नहीं होती, और न ही किसी गिरोह से उन्हें हिफाजत मिली होती है. नतीजा यह होता है कि सच का झंडा लेकर चलने वाले अक्सर अकेले दिखते हैं, और बहुतों को यह भी लगता है कि उनमें कोई दिमागी नुक्स है कि वे चैन से बैठने के बजाय यूं बेचैन फिरते हैं. आमतौर पर सच के लिए लडऩे वाले ऐसे लोग दुनिया में अकेले पडऩे लगते हैं, और बहुत से मामलों में सच की तकलीफ का बोझ उठाते परिवार के भीतर भी वे अकेले होने लगते हैं.
जिस तरह विज्ञान कथाओं की कुछ फिल्मों में मशीनी मानव दिखाए जाते हैं कि किस तरह वे गिनती में बढ़ते चलते हैं, और फौज सरीखे होकर इंसानों पर टूट पड़ते हैं, कुछ उसी तरह झूठ के भाड़े के हत्यारे फायदा पाते हुए इन दिनों सोशल मीडिया पर हमलावर बने हुए हैं, और पैसों की ताकत से उनकी गिनती बढ़ती चल रही है. इंटरनेट और सोशल मीडिया ने मिलकर विचारों के मुकाबले को ऐसा बना रखा है कि स्टेडियम में बैठे, मुकाबला देखते लोगों की गिनती फरेब की तरह बढ़ाकर दिखाई जा सकती है, और जनमत के आकार को अंधाधुंध बड़ा या छोटा साबित किया जा सकता है. यह कुछ उसी तरह का है जिस तरह कि कसरत की कुछ मशीनों, या शरीर को किसी आकार में ढाल देने का दावा करने वाले खाने-पीने के सामानों के इश्तहार होते हैं, जो कि हकीकत से परे हसरत की तस्वीरें दिखाते हैं, और ग्राहक जुटाते हैं.
सच और झूठ पर भरोसा रखने वाले लोगों की अलग-अलग गिनती भी मुमकिन नहीं होती, क्योंकि झूठ का झंडा लेकर चलने वाले बहुत से लोगों को भी इस बात का एहसास होता है कि असल में सच क्या है. वे झंडे के झूठ पर सचमुच ही खुद भरोसा नहीं करते, लेकिन एक पेशे की तरह, या कि एक नफरतजीवी मकसद के चलते वे उस झूठ को सच करार देते हुए एक अभियान चलाते हैं. ऐसे लोगों को झूठ पर भरोसा रखने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे झंडा तो झूठ का लिए चलते हैं, लेकिन अपने मन के भीतर उन्हें हकीकत का सच भी मालूम होता है. इसलिए सोशल मीडिया पर जो दिखता है, या कि आज के मीडिया के टीवी स्क्रीन पर, अखबारी पन्नों पर जो दिखता है, जरूरी नहीं है कि लिखने और लिखाने वाले लोगों का खुद का उस पर भरोसा हो.
यह बात सही है कि मीडिया के एक बड़े तबके के लिए प्रॉस्टीट्यूट जैसी गाली जोड़कर, प्रेस को प्रेस्टीट्यूट करार देने का काम मोदी सरकार के एक बड़बोले फौजी बददिमागी मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने किया था, लेकिन आज मीडिया और सोशल मीडिया की जो हालत है, उसमें यह शब्द बहुत नाजायज नहीं है, यह एक अलग बात हो सकती है कि कौन सा तबका इस शब्द का ज्यादा बड़ा हकदार है. यह तमगा उन लोगों पर बेहतर सजता है जो रोज झूठ का गुब्बारा फुलाने के कारोबार में लगे हुए हैं.
अभी मुझे इस बात का ठीक-ठीक अंदाज नहीं है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सच और झूठ को देख और सुनकर पाठकों और दर्शकों का कितना हिस्सा झूठ-सच का फर्क कर पाता है, और कितना झांसे में आ जाता है. यह अंदाज इसलिए आसान नहीं है कि विचारधारा को समर्पित, नफरतजीवी, किसी नामौजूद दुश्मन के खिलाफ लडऩे को आमादा लोग जब किसी झूठ को सच मानते हुए दिखते हैं, तो यह समझ नहीं पड़ता कि वे झूठ को सचमुच सच मान रहे हैं, या कि वे उसे सच मानते हुए दिखना भर चाहते हैं. यह पूरा सिलसिला कुछ जटिल है, और कुछ उलझा हुआ है, बदनीयत से लदा हुआ है, और अनुपातहीन अधिक ताकत से लैस भी है. इसलिए किसी संक्रामक रोग की तरह, किसी कम्प्यूटर वायरस की तरह, गणेश के दूध पीने की अफवाह की तरह, झूठ पर जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे, सच की तरह, सच मानकर भरोसा करने वाले लोगों के बीच फर्क कर पाना नामुमकिन सा है.
लेकिन इंसानी सोच में जो एक आम बात है, उसके मुताबिक नफरत लोगों को बड़ी रफ्तार से जोड़ लेती है. मोहब्बत जब तक प्रेम का ढाई आखर लिख पाती है, तब तक नफरत झूठ के पर्चे छापकर शहर के हर चौराहे पर बांट चुकी होती है. सच को सोशल मीडिया की जंग के लिए मानो 80 रूपए लीटर का पेट्रोल मिलता है, और झूठ को अपनी लड़ाई के लिए 31 रूपए लीटर मिल जाता है जो कि दुनिया के बाजार में उसकी कीमत है.
यह गैरबराबरी की लड़ाई कई बार सच का हौसला पस्त करती है, और वैसे में सच को लेकर कही गई सूक्तियां काम आती हैं जो हौसले को चार कदम और चलने को कहती हैं. लेकिन सच यह है कि ऐसे चार कदम उस डॉक्टरी दिलासे की तरह रहते हैं जो कि चार हफ्ते बाद कटने वाले प्लास्टर को लेकर मरीज को बस कुछ दिन और का भरोसा दिलाते चलते हैं. गैरबराबरी की यह लड़ाई अंतहीन भी दिखती है, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है कि कोई लड़ाई कभी अंतहीन नहीं होती.
* लेखक वरिष्ठ पत्रकार और शाम के अख़बार छत्तीसगढ़ के संपादक हैं.