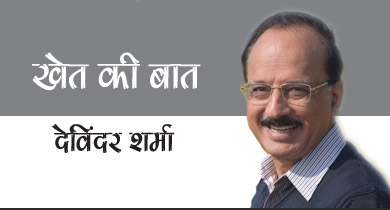किसानों को क्यों नहीं मिलती क़ीमत
देविंदर शर्मा
अंततः हरियाणा सरकार किसानों को सूरजमुखी की ‘उचित’ कीमत अदा करने पर सहमत हो गयी है. कुछ समय पूर्व किसान इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, और सरकार इसे देने से साफ इनकार करती रही थी. किसानों ने विरोध जताने के लिए चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे को बाधित किया, यातायात खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया. आंदोलनकारी किसानों ने सूरजमुखी की फसल के उचित भाव की मांग को लेकर एकजुटता दर्शायी.
असल में हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि वह भावांतर भरपाई स्कीम के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति दे रही थी लेकिन किसान पूर्व घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही फसल की खरीद किये जाने पर अड़े हुए थे.
बतौर न्यूनतम समर्थन मूल्य 6400 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय किसानों को अपनी फसल 4200 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बेचने को मजबूर किया जा रहा था. यहां तक कि राज्य सरकार के वादे के मुताबिक प्रति क्विंटल एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति मिलने के बाद भी किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपये या उससे कहीं अधिक का घाटा था.
इससे सूरजमुखी उत्पादकों में वाजिब गुस्सा था. सूरजमुखी की समर्थन मूल्य पर खरीद से शुरुआती इनकार, फिर किसानों के सड़कों पर उतर आने के बाद, ‘उचित’ मूल्य भुगतान का समझौता सरकारों के पूर्वाग्रह को ही दर्शाता है.
हालांकि इसकी जड़ें 1930 के दशक में उन दिनों तक जाती हैं, जब उद्योगपतियों का एक बॉम्बे क्लब नामक समूह कभी यह भरोसाबनाने की दिशा में काम करता था कि खाद्य पदार्थों की कीमतें कम रखी जाएं ताकि वेतन कम रखे जा सकें.
दरअसल बरसों से कृषि को दरिद्र बनाए रखकर खाद्य कीमतों को कम रखने की यही आर्थिक सोच हावी रही है. इसलिए आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाए रखने को या कहें कि कंपनियों को मुनाफा कमाने की इजाजत देने के लिए कृषि को दांव पर लगाया जा रहा है.
हरियाणा का घटनाक्रम समझ से परे है कि पहले तो किसानों की उपयुक्त दर की न्यायोचित मांग को नकार दिया गया और फिर सड़कों पर हंगामे के बाद सही कीमत देने को राजी भी हो गये. यह शुरू में ही क्यों नहीं किया गया? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का हक है. यदि सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया होता तो कोई वजह ही नहीं थी कि किसान राजमार्ग पर आकर विरोध प्रदर्शन करते.
सच कहूं तो मैंने आज तक कभी किसी कॉरपोरेट दिग्गज को अपने बेड लोन की माफी को लेकर नई दिल्ली के जंतरमंतर पर प्रदर्शन करते नहीं देखा. यह भी कि दस वर्षों के 12 लाख करोड़ रुपये के बीमार कॉर्पोरेट ऋण को बिना किसी विरोध बैंक के रजिस्टर से कैसे हटा दिया गया?
इतना ही काफी नहीं, आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के लिए ‘समझौता निपटान’ की इजाजत दी है, जिनके पास भुगतान सामर्थ्य है लेकिन वे नहीं करते ताकि एक वर्ष बाद नए सिरे से लोन ले सकें. जबकि कृषि कर्ज पर डिफ़ॉल्टर हो जाने पर किसानों को नियमित तौर पर सलाखों के पीछे भेजा जाता है.
जाहिर है आरबीआई चहेते पूंजीपतियों के लिए ‘कवच’ का काम करता है. मुझे ख़ुशी है, ऐसे में जब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री इस विकृति को लेकर साफ तौर पर चुप हैं, बैंक संघ खुले तौर पर आरबीआई की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं.
यह भेदभाव आर्थिक विश्लेषण में भी स्पष्ट दिखता है.
बीती 14 जुलाई को एक अंग्रेजी दैनिक में एक लेख ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली वृद्धि सरकार द्वारा एक सख्त कदम है’ प्रकाशित हुआ जिसमें दो अर्थशास्त्रियों ने 2023-24 विपणन सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 7 प्रतिशत की अतिरिक्त मामूली बढ़ोतरी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य टोकरी के लिए भारित औसत की गणना की है.
लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि विपणन सत्र अभी शुरू होना है, और यह देखते हुए कि साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल 14 फीसदी फसलें खरीदी जाती हैं, कीमतों में वृद्धि को पूरी फसल से जोड़ना जल्दबाजी होगी. शेष 86 फीसदी फसलों का ज्यादातर कारोबार न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर होगा. इसका मतलब यह भी कि चुनाव पूर्व वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य मूल्य वृद्धि के जरिये देखी गई बड़ी बढ़ोतरी भी गलत थी.
दूसरी ओर, जो लोग किसानों को दोषी ठहराते हैं कि वे बिना सोचे-विचारे जल्दबाजी में राजमार्गों और रेल पटरियों को बाधित करके बैठ जाते हैं, उन्हें भी अपना पूर्वाग्रह त्याग देना चाहिए.
सोशल मीडिया जैसे मंचों पर सक्रिय आलोचक अक्सर प्रदर्शनकारी किसानों पर भड़कते हैं. जैसे कि किसानों को हाइवे जाम करके दूसरों को सताने में खुशी मिलती हो. ऐसी आलोचना अनुचित ही होगी, और इससे शहर में जन्मे-पले लोगों की ग्रामीण देहात के बारे में समझ का पता चलता है.
देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शनों की मामला-दर-मामला जांच करें, और आप देखेंगे कि उनके साथ कैसे ज्यादती हुई. वे एक आर्थिक षड्यंत्र के शिकार हैं. जिसका मकसद असल में उन्हें ज़मीन से बेदखल करना है. मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों और नौकरशाही ने शायद ही कभी किसानों की भूमिका को भूमि बैंक और श्रम बैंक से परे देखा हो. दरअसल, पैदावार के सही दाम प्राप्ति के लिए किसानों के पास लट्ठ का सहारा लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प कम ही है.
यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि नीति निर्माताओं में किसानों को गारंटीशुदा कीमत प्रदान करने को लेकर अनिच्छा क्यों हैं?
इसका एक बड़ा कारण तो यही है कि कॉलेज पाठ्यक्रम में इकोनॉमिक 101 यानी अर्थशास्त्र की शुरुआती मूल अवधारणाओं ने हमें यह यकीन करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया है कि बाजार के तहत ही सर्वोत्तम कीमत प्राप्त होती हैं. वास्तव में, निराशाजनक ही है जब कुछ जनमत बनाने वाले भी किसानों को सही कीमत का आश्वासन प्रदान करने की जरूरत को चुनौती देते हैं.
यदि किसानों के लिए सूरजमुखी के लिए 6,400 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय 4,800 रुपये प्रति क्विंटल बाजार भाव प्राप्त करना ठीक है, तो इसी तर्ज पर अगर शीर्ष नौकरशाहों को जूनियर अधिकारियों के बराबर वेतन दिया जाएगा तो वे उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे. इसी तरह, अगर सेना के सबसे वरिष्ठ अफसरों को दो रैंक से नीचे के अधिकारियों के बराबर वेतन मिले, तो जोरदार विरोध होगा.
दरअसल किसान भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं. उन्हें भी तो अपने परिश्रम के बदले पर्याप्त भुगतान की आवश्यकता है, वह भी इतना तो होना चाहिये जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर व्यवहार्य और लाभकारी आमदन प्राप्त हो सके.
1970 से 2015 तक के 45 वर्ष की अवधि में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 120 से लेकर 150 गुणा तक बढ़ोतरी हुई वहीं इसके मुकाबले, यदि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को संकेतक मान लिया जाये, कृषि आय में वृद्धि केवल 19 गुना ही हुई है. आमदनी में यह भारी अंतर उस सोचे-समझे प्रयास की ओर इशारा करता है जिसके तहत कृषि आय को व्यापक आर्थिक संकेतकों के दायरे में रखा गया.
दूसरे शब्दों में, खाद्य मुद्रास्फीति कम रखने के लिए खाद्यान्न कीमतों को कम रखकर किसान पारंपरिक तौर पर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का बोझ उठाते रहे हैं. इसे बदले जाने की जरूरत है.
आखिरकार, किसान को भी तो आय समानता की जरूरत है. यह तभी संभव है, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा दिया जाये, यह आश्वासन कि इस मानक कीमत से कम पर कोई लेन-देन नहीं होगा.