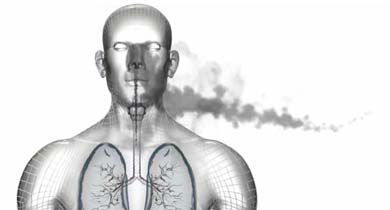सिलिकोसिस का कहर
सिलिकोसिस जैसी कामकाजी रोगों को लंबे समय से नजरंदाज किया जा रहा है. यह धीमी मौत देने वाली बीमारी है. अनुमान है कि भारत में इसकी चपेट में 30 लाख से एक करोड़ मजदूर हैं. इसके बावजूद इस पर जरूरी ध्यान नहीं दिया जा रहा. हाल ही में ओडिशा में एक श्रम अदालत ने उन 16 परिवारों को मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया जिनके कमाई करने वाले प्रमुख सदस्य को इस बीमारी ने अपनी जद में ले लिया था.
इस घटना से पता चलता है कि धीमी मौत देने वाली इस बीमारी को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है. क्योंझर जिले के मदारंगोजोड़ी गांव के इन 16 लोगों की मौत सिलिकोसिस से हुई. ये एक ऐसी इकाई में काम कर रहे थे जहां ये सिलिका कण सांस के जरिए ले रहे थे. जबकि इन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी. समय के साथ उनके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई. क्योंकि सिलिकोसिस का कोई इलाज नहीं है. उन्होंने अपने पीछे ‘विधवाओं का गांव’ छोड़ दिया. एक स्थानीय संस्था ने इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने उठाया. तब जाकर यह बात तय हो पाई कि इनकी मौत सिलिकोसिस की वजह से हुई है. जहां वे काम कर रहे थे, अगर वहां के प्रबंधन ने कुछ सावधानी बरती होती तो उनकी जान नहीं जाती. उन्हें सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं दिए गए थे. अदालत ने ओडिशा सरकार को यह आदेश दिया है कि वे इनके परिवारों को 46 लाख रुपये का मुआवजा दे.
यह फैसला इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 2016 में उच्चतम न्यायालय ने भी एक ऐसा ही फैसला दिया था. यह फैसला गुजरात के गोधरा और बालसिनोर में क्वार्टज कारखाने में काम करने वाले 238 श्रमिकों की मौत के मामले में आा था. इनकी मौत भी सिलिकोसिस की वजह से हुई थी. ये लोग मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले के आदिवासी गांवों के थे. ओडिशा के मजदूरों के तरह इन्हें भी पता नहीं चला कि इनकी सांसों के जरिए जहर उनके शरीर में आ रहा है. क्योंकि इसके कण गंधहीन होते हैं. यहां भी एक गैर सरकारी संस्था ने इस मसले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने का काम किया. अदालत ने इस मामले में कड़ा फैसला दिया. गुजरात सरकार को जान गंवाने वाले 238 मजदूरों के परिजनों को 7.14 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को कहा गया और मध्य प्रदेश सरकार को इस बीमारी से पीड़ीत 304 लोगों का पुनर्वास करने को कहा गया.
दोनों मामलों में यह बात समान है कि मजदूर अस्थाई तौर पर काम कर रहे थे. इसका मतलब यह हुआ कि कानून के तहत जो सुविधा उन्हें मिलती, उससे वे वंचित थे. इनमें भी कई गरीब मजदूर दूसरे राज्यों से आए थे. वे जहां काम कर रहे थे, उन कारखानों ने सुरक्षात्मक उपाय अपनाने पर कोई निवेश नहीं किया. जब सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी तो उन्हें कोई मेडिकल सहायत भी नहीं मिली. उनके स्वास्थ्य की जांच की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस बात को सिद्ध करना मुश्किल रहा कि उनकी यह हालत कामकाजी परिस्थितियों की वजह से हुई है. जब वे काम करने में पूरी तरह से अक्षम हो गए तो अपने गांव में लौट आए और धीरे-धीरे करके मौत की ओर बढ़ते गए.
कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 और कामगार मुआवजा कानून, 1923 के तहत सिलिकोसिस को कामकाजी रोग माना गया है. लेकिन इन कानूनों का फायदा संगठित क्षेत्र के मजदूरों को ही मिल पाता है. ऐसे रोगों की खतरों से जूझ रहे अधिकांश मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं. जहां न तो वे अपनी मजदूरी को लेकर मोलभाव कर सकते हैं और न ही कामकाजी परिस्थितियों को लेकर. सिलिकोसिस को कई बार टीबी समझकर इसका उपचार किया जाने लगता है. जब अगर कोई सिलिकोसिस से मरता है तो यह सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि मौत की वजह सिलिकोसिस है. इसलिए सिलिकोसिस और ऐसे ही दूसरे रोगों की वजह से मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है, वह काफी कम दिखता है.
ये कामकाजी रोग सिर्फ भारत में ही नहीं हैं. ब्रिटेन में इन रोगों से बचाव के लिए कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे. इनमें न सिर्फ बचाव वाले उपकरण शामिल हैं बल्कि वे उपाय भी हैं जिनसे जोखिम कम होता है. साथ ही वहां मजदूरों की नियमित स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था है. सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी पकड़ में नहीं आती. इसलिए नियमित जांच की वजह से इसे शुरुआती स्तर में पकड़ने में सुविधा होती है और उस हिसाब से इससे बचाव के उपाय किए जाते हैं. क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं है.
दोनों मामलों में आए अदालती निर्णय राज्यों को गरीबों को प्रभावित करने वाली इस समस्या की ओर ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करते हैं. 1984 में भोपाल त्रासदी के बाद फैक्ट्री कानून में 1987 में संशोधन किया गया था. इसके तहत खतरनाक प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है और जरूरी चिकित्सीय व्यवस्था की बात भी की गई है. लेकिन ये प्रावधान सिर्फ कागजों में ही हैं. जो इसके हकदार हैं, उनके लिए भी ये जमीन पर नहीं उतर पाए हैं. दूसरी तरफ खदानों और अन्य कारखानों में काम कर रहे मजदूर एक ऐसी दुनिया के लिए अपना खून-पसीना बहा रहे हैं जिसके लिए उनका अस्तित्व ही अदृश्य है.
1966 से प्रकाशित इकॉनामिक एंड पॉलिटिकल विकली के नये अंक का संपादकीय