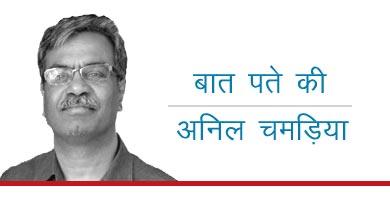एससीएसटी एक्ट और मोदी सरकार
अनिल चमड़िया
डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले (क्रिमिनल अपील नंबर 416/2018) के बहाने सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) कानून 1989 को लेकर 20 मार्च 2018 को जो दिशा-निर्देश जारी किया है, उसकी पृष्ठभूमि पर गौर करना जरूरी है.
पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के बहाने दलित आदिवासी उत्पीड़न विरोधी इस कानून के प्रावधानों की नई व्याख्याएं पेश की हैं. एक मामले के बहाने पूरे कानून पर सवाल खड़ा करने की मिसालें इन दिनों बढ़ रही हैं. खासतौर से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण से जुड़े कानूनों के साथ यह देखा जा रहा है. दलित आदिवासी उत्पीड़न विरोधी कानून से पहले सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं दो जजों की बेंच ने महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी कानून की भी लगभग इसी तरह व्याख्या की थी.
सुप्रीम कोर्ट कोई टापू पर बैठी संस्था नहीं है. फैसले अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों की कड़ी होते हैं. जिस तरह से एक लंबे समय तक राजनीतिक, सामाजिक आंदोलनों के दबाव में आकर संसद को इस तरह का कानून बनाना पड़ा था, ठीक उसी तरह उसके उल्टा राजनीतिक, सामाजिक दबावों में वंचितों की सुरक्षा व हितों में बनाए गए प्रावधानों पर हमले हो रहे हैं. ये राजनीतिक, सामाजिक दबाव क्या है? यह दबाव क्या समाज के वंचित वर्गों के हितों की सुरक्षा का है या फिर ये दबाव वंचितों के हितों से नाराज होने वाले समाज के वर्चस्ववादी समूहों का दबाव है?
घटना क्या है : 2009 में महाराष्ट्र के कराड स्थित सरकारी फार्मेसी कॉलेज में एक दलित कर्मचारी द्वारा प्रथम श्रेणी के दो अधिकारियों के खिलाफ उक्त कानून की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराने का है. डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी ने उसकी जांच की और चार्जशीट दायर करने के लिए आला अधिकारियों से लिखित निर्देश मांगा. उस संस्थान के प्रभारी डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और चार्जशीट दायर नहीं की जा सकी. तब उक्त दलित कर्मचारी ने डॉ. महाजन के खिलाफ शिकायत दर्ज की. डॉ. महाजन ने हाईकोर्ट में उस एफआईआर को रद्द करने की मांग की जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया. इसके बाद डॉ. महाजन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इस तरह उत्पीड़न का शिकार होने वाले कर्मचारी के बजाय यह मामला सरकार बनाम डॉ. महाजन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया.
फैसले के वक्त केन्द्र में जो भी पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार उस दौरान सत्ता की पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है. नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के बाद दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं. वंचित वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के आरक्षण के प्रावधानों को लगातार कमजोर होते महसूस किया जा रहा है. यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों को इस तरह से कर दिया है कि वंचित वर्गों में असुरक्षा की भावना और बढ़ गई है. इन सब हालातों के बीच रखकर ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की समीक्षा की जा सकती है.
कानून की सुरक्षा करने में सरकार की विफलता
इस मामले में केन्द्र सरकार के एडीशनल सॉलीसिटर जनरल ने अपनी दलीलें जिस तरह से पेश की है, उसमें इस मुकदमे के प्रति सरकार की संजीदगी का आकलन किया जा सकता है. दरअसल एक कानून जब बनता है तो उसके लिए तथ्यों को आधार बनाता है और संविधान के दर्शन के मुताबिक समाज के दबे- कुचले लोगों के पक्ष में उन तथ्यों की व्याख्या की जाती है लेकिन इस समय की सच्चाई यह है कि दलितों- आदिवासियों के उत्पीड़न की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं लेकिन उन शिकायतों पर सरकार कार्रवाइयां करने में विफलता हासिल कर रही है और सरकार की यह विफलता शिकायतों को फर्जी साबित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस में 2016 में की गई शिकायतों का एक आंकड़ा और उसके नतीजों का हवाला दिया है कि दलितों के उत्पीड़न का कुल मामलों में 5347 मामले और आदिवासियों के उत्पीड़न की शिकायतों के मामलों में 912 शिकायतें झूठी पाई गई. 2015 में 15638 मुकदमों में 11024 मुकदमों में सजा नहीं हुई या आरोप मुक्त कर दिया गया. 495 मामले वापस लिये गए. केवल 4119 मामलों में सजा हुई.
इन तथ्यों की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है कि इन वर्षों में दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई के मामले में सत्ता का तंत्र ढीला पड़ा है या फिर वह तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक गोलबंदी के आगे झुका हुआ है. यह आंकड़े शिकायतों के फर्जी होने से ज्यादा सत्ता की मशीनरी पर सवाल खड़े करती है लेकिन मजेदार बात यह दिखती है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिन आंकड़ों की व्याख्या अपने फैसले के अनुकूल करने की कोशिश की है, उसी तरह से सरकार के वकील की दलीलें भी उन व्याख्याओं को मजबूत करने में मदद पहुंचाई है.
सरकार के वकील ने भी कहा कि 2015 के 75 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया व उन्हें वापस ले लिया गया. 15-16 प्रतिशत मामलों में पुलिस अधिकारियों ने मुकदमे को बंद करने की रिपोर्ट पेश की.
कमजोर वर्गों के लिए प्रावधानों की व्याख्या
इसी तर्क के आधार पर क्या उन कानूनों की भी व्याख्या कर सकते हैं जिसमें सत्ता की मशीनरी अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार इस्तेमाल करती है और वे आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो पाते हैं, तो क्या उन कानूनों व प्रावधानों को भी समाप्त कर देना चाहिए? दलितों व आदिवासियों का उत्पीड़न बहुस्तरीय होता है और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के भी बहुस्तरीय ढांचे मौजूद है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में हवाला दिया है कि कैसे समाज के प्रभावशाली लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत शिकायतें दर्ज करायी जाती है लेकिन उत्पीड़न तो बराबर समाज पर वर्चस्व रखने वाला समूह, समुदाय व संस्कृति ही करती है?
राजनीतिक स्थितियां यह तय करती हैं कि किन आंकड़ों की किस तरह से व्याख्या की जाए. समाज के कमजोर वर्गों के लोकतांत्रिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों पर हमला करने की दृष्टि से कानून समेत उन तमाम प्रावधानों की व्याख्याएं की जा रही हैं जिसे लंबे संघर्षों के बाद वंचितों ने हासिल किया है. यह संयोग नहीं है कि महिलाओं और वंचितों, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है. दरअसल इस तरह के फैसले असुरक्षा की भावना को और तेज करते हैं. दलित उत्पीड़न कानून को ही जातिवाद बढ़ाने वाले कानून के रुप में देखा गया है जबकि यह जातीय उत्पीड़न के विरुद्ध कानून के रूप में सामने आया है.
इस फैसले में कई मजेदार पहलू है, उनमें एक प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण के एक हिस्से को भी उद्धृत किया गया है. आमतौर पर जिस तरह से डॉ. अम्बेडकर से लेकर मानवाधिकार घोषणा पत्र की व्याख्या वर्चस्ववादी राजनीतिक-सामाजिक समूह इन दिनों करता है लगभग उन्हें उसी तरह से इस फैसले में दोहराया गया है. यह न्यायालयों के नहीं बल्कि न्यायाधीशों द्वारा फैसलों के लिखे जाने में सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक उदाहरण के रुप में यह फैसला याद किया जाएगा.