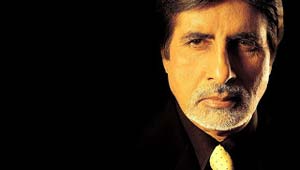उत्सव और आक्रोश के बीच कन्हैया
संजय अग्रवाल
इस मुल्क में राजनीति अवाम के लिए सहज ही उपलब्ध मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन गई है. सिनेमा या क्रिकेट के तमाशे से भी ज्यादा मनोरंजक. ऐसे में कन्हैया एक अनचाहा व्यवधान ही तो है. जाहिर है, सर्वाधिक व्यस्त समय के मनोरंजन में खलल भीड़ के रहनुमाओं को रास नहीं आ सकता था. लिहाजा लोकप्रिय राजनीति के नुमाइंदे नहीं चाहते कि कोई ‘कन्हैया’ अवाम को स्वप्ननिद्रा से जगाने की हिमाकत करे.
जेल से रिहा होने के बाद जेएनयू परिसर में दिए अपने भाषण में कन्हैया एक ठोस वैचारिक भाषण के साथ जरूरी सवालों और चीजों की पड़ताल कर रहे थे. पूरी ताजगी और ऊर्जा के साथ. महज अटठाइस बरस के इस युवा का भाषण काफी सराहा भी गया.
मगर यह उत्सवप्रेमी देश है. तमाम विपरीत हालात में भी यहां उत्सव की गुंजाइश बन ही जाती है. और उत्सव का मतलब ही है पीड़ा और उलझन से मुक्त हो जाना. दिलचस्प यह है कि भारतीय अवचेतन में जो कन्हैया गहरे समाया हुआ है, उसके चारों तरफ गोपियां होती हैं. और वह बीच में बासुरी बजा रहा होता है. वह रासलीला भी करता है. गायें भी उसकी एक आवाज पर दौड़ती चली आती हैं.
हमारे सामूहिक अवचेतन में महाभारत का ‘कन्हैया’ नहीं है. जिसमें संजय राजा धृतराष्ट्र को ‘युद्धभूमि’ का आंखो देखा हाल सुनाते हुए कहते हैं, कन्हैया ही लड़ रहा है. वही मार रहा है और वही मर भी रहा है. बाकी तो भीड़ का हिस्सा मात्र हैं. (शायद यह लाइव कमेंट्री की शुरुआत थी)
महाभारत काल से आज की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हैं. मार्क्स ने विषमता के खिलाफ दुनिया को समाजवाद का एक आदर्श दृष्टिकोण दिया था. जिसमें कहा गया कि धर्म अफीम है. मगर यहां तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था में अफीम-भांग सब मिल चुकी है. सार यह है कि भ्रमित और चकाचौंध करने के सारे सामान मौजूद हैं.
बाजारवाद ने तंत्र के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसमें अवाम के एक छोटे से हिस्से के लिए रोज दीवाली है. और बहुत बड़ा तबका अभाव में जी रहा है. मगर कमाल यह है कि अभाव को अपनी आदत बना चुका तबका तो इस रोजाना होने वाले उत्सव का उपभोक्ता नहीं है, दर्शक मात्र है. उसमें अपने इस ‘साक्षी भाव’ को लेकर कोई बेचैनी या आक्रोश नहीं है.
दरअसल अमरीका की विज्ञान फंतासी ने सुपरमैन रचा, तो हमारे भारतीय सिनेमा में अकेला नायक पूरी व्यवस्था से लड़ता है. और अंत में उसका जीतना भी तय है. याद कीजिए इमरजेंसी के दौर के आसपास ‘आक्रोशित युवा’ के किरदार ने अमिताभ बच्चन को फिल्मी परदे पर सफल बना दिया. जिसमें अकेला निहत्था हीरो दस-बीस गुंडों की पिटाई करता है और दर्शक ताली बजाते हैं. अवाम ने मान लिया कि फिल्मी एंग्री यंग मैन ने परदे पर दरअसल उसके आक्रोश को ही जीवंत किया. इस तरह अवाम के अपने भीतर के आक्रोश का शमन हो जाता है.
मगर क्या आज का ‘यंग इंडिया’ वाकई एंग्री है? सवाल कठिन है. पर जवाब तो चाहिए. बेगूसराय या फिर जेएनयू या फिर हैदराबाद उस जैसे कुछ छोटे छोटे दीपों में ही आक्रोश की कुछ हलचल दिखती है. बाकी तो राष्ट्रवादी उन्माद के शोर तले सहनशील बहुमत के पास या तो ‘मस्ती मंत्र है’ या ‘मौन मंत्र’.
हम चाहते हैं कि कन्हैया या रोहित जैसे युवा हमारे लिए लड़ें. मगर हमारे लड़के उन जैसे हों यह हम नहीं चाहते. यह तटस्थता हमारा जमीनी सच है.
इस देश में मिट्टी और पसीने की खुशबू का बखान किया जाता है. परंतु अब कोई डीयो परफ्यूम बेचने वाली कंपनी विज्ञापन के माध्यम से युवाओं को लगातार यह समझा रही है कि पसीने में बदबू है. डॉलर के सपने देखने वाली युवा पीढ़ी ने इसे सच भी मान लिया है. इस छोटे से उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि दरअसल चीजें किस हद तक उलट पलट गई हैं.
कन्हैया समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं. इन सारे विरोधाभासों को उन्होंने देखा-समझा होगा. निश्चित ही उन्होंने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का भी उन्होंने गहराई से अध्ययन भी किया होगा, क्योंकि वे वैचारिक लड़ाई के पक्षधर हैं.
सहूलियत की राजनीति के दौर में सरोकार की राजनीति का झंडा उठाये कन्हैया ने इतना तो बता ही दिया कि अब तक की सबसे मजबूत सरकार होने का दावा करने वाले असल में कितने डरे हुए और कमजोर हैं. कन्हैया जरूरी सवालों पर अपने सार्थक विचारों से उम्मीद जगाते हैं. मगर इस दौर की कड़वी सच्चाई यही है कि अंततः हम तमाशबीन ही हैं.