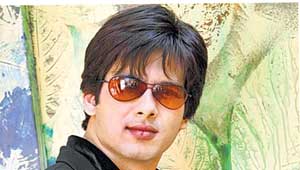फेसबुक के नाम गगन गिल का पत्र
चाहता था इन गलियों से बेदाग निकल जाऊं! – कुँवर नारायण
ऐसी इच्छा हम सभी की होती होगी, पुरुष हो या स्त्री.
मैं फेस बुक पर नहीं हूं, आप लोग जानते हैं. मुझे मेरी अजीज़ ने कुछ स्क्रीन शॉट्स भेजे तो पता चला, आप लोग चौपाल में व्यस्त हैं. इस बीच आप कुछ और बूढ़े हो गए होंगे, इस पृथ्वी पर आपका समय कुछ और खत्म हो गया होगा. क्या आपने वक्त की टिकटिक सुनी? मैं इतने बरसों से उसी को सुनती चुपचाप अपना काम कर रही हूँ. शायद कभी- कभी आपको मेरा लिखा दिख जाता हो, चौपाल की फुर्सत के बाद.
मुझे खेद है, विमल कुमार जी, दिविक रमेश जी, मैं अपनी चुप्पी में से समय नहीं निकल पायी. आप लोगों से संवाद में कितना कुछ सीख सकती थी लेकिन मुझे अपना एकांत ही पसंद था.
आभारी हूँ, विमल कुमार जी, कि आपको यह लक्षित करना याद रहा, मैं इतने बरसों में कभी किसी दरबार में नहीं गयी, न गुट में.
ऐसा नहीं, कि मैंने आप हिंदी समाज के लोगों से जान-बूझ कर बात नहीं की. मैं अपने अध्ययन कक्ष में ही इतना व्यस्त रही, मेरी रुचियां ही इतनी अलग थीं, कि मुझे ध्यान नहीं रहा, आखिर आप लोग हैं तो मेरे समुदाय के, अनदेखे किये जाने के सब्र की भी कोई हद होती है.
लेकिन क्या इस तरह ध्यान आकर्षित करना था आप सब को? चौपाल लगा कर?
कितना अच्छा होता, अगर मैं सारी बात इशारे से कह देती. किसी का नाम न लेती. किसी को दुःख न पहुंचता. आज आप सब की सभा में शिकायत रख रही हूँ साफ़-साफ़. हो सके तो न्याय करियेगा, नहीं तो चौपाल तो है ही.
सबसे पहले, मुद्दे की बात. जिन अनिल जनविजय के साथ मेरे नाम को लेकर हंगामा हो रहा है, वह हमेशा से एक बीमार आदमी थे. मेरा दुर्भाग्य, कि उनसे मेरा परिचय कॉलेज की कविता प्रतियोगिताओं में हुआ था, करीब चालीस बरस पहले. सत्रह अट्ठारह बरस की भोली उम्र में. तब मुझे मालूम नहीं था, मैं महादेवी के बाद की सबसे उल्लेखनीय कवि कहलाऊँगी.
वह उस समय भी शोहदे व्यक्ति थे, और अब भी. मैंने उन्हें कई बरसों से देखा नहीं, कि पता चले, बीमारी कितनी बढ़ गयी है.
उस समय,1977 में, मैं छोटी उम्र की ज़रूर थी लेकिन समझती सब थी, जैसा दिविक जी ने कहा. अनिल को तब कोई नहीं जानता था. वह फटेहाल रहते थे, सौतेली मां की कुछ बात करते थे. बाद में उन्होंने जेएनयू में जुगाड़ बैठाया, मास्को चले गए, आदि.
आजकल वह फेसबुक पर सब तरह के वरिष्ठों की गलबहियां करते दिखते हैं. इस दुर्घटना के दौरान ही मैंने फेसबुक पर उनके ‘सादा जीवन उच्च विचार’ की झांकी देखी है. इतनी उठा-पटक में उन्होंने लिखा क्या, सोचा-समझा क्या, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पायी. न यह पता चल पाया कि इस बीच वह अट्ठारह बरस की उम्र से बड़े हुए कि नहीं! क्या पता, उन्होंने काल को मात कर दिया हो और मुझ तक खबर न पहुंची हो!
दरअसल 1978 के आसपास पश्यन्ति के संपादक स्वर्गीय प्रभात मित्तल से उनका परिचय मैंने ही करवाया था. अनिल की जुगाड़ू काबिलियत यह कि बाद में वह कई अन्य हापुड़ वालों की किताबें भी ढोते रहे. यह सब इतना पुरातन समय है मेरे लिए कि अब सब धुंधला है.
मुझे नहीं मालूम था, चालीस बरस से एक पुरानी जोंक अभी भी मेरे साथ चिपकी हुई है, वह अभी भी मेरा नाम भुना कर लहू पी रही है.
अनिल ने उन बरसों में जब मेरे नाम से श्री स्वप्निल श्रीवास्तव की किसी चार पन्ने की पैम्फलेट में कुछ छपाया व मुझे दिखाया तो मैं सतर्क हुई. यह तब की बात है, जब मैं अभी कच्चा लिख रही थी. आज की गगन गिल नहीं हुई थी. एक दिन लौटेगी की कविताओं से पहले के दिन.
जो लोग शोध करना चाहें, वह इस बात पर भी ध्यान दें कि लेखन में मैं उनकी वरिष्ठ थी, तब भी, आज भी.
उन बरसों में अनिल जनविजय को हम सब ने कई बार डाँट लगायी, प्रभात जी ने भी, एक बार अमृता भारती ने उन्हें अपने घर से ही निकाल दिया था, कोई कविता इस लेखिका को समर्पित करके छपा कर दिखाने लाये थे. लेकिन अनिल ढीठ निकले. जैसा अब देख रही हूँ, हैरानी और अविश्वास से.
अगर कोई बीमारी चालीस बरस पुरानी हो जाये, तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते. आप लोग चाहें, तो मिल जुल कर उनका इलाज ढूंढ़ सकते हैं.
यह सब इतना लंबा कैसे खिंच गया? मुझे सबसे ज़्यादा इसी पर हैरानी है. लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. क्या इसलिए, कि हर बार अनिल जनविजय धृष्टता के बाद माफीनामे भेजते रहे व मैं रफा-दफा करती रही? हो सकता है, विमल कुमार भी उन्हीं दिनों अनिल का कोई माफीनामा लेकर आये हों, मुझे याद नहीं.
सच तो यह है, मेरी दुनिया ही दूसरी थी, मैं अमृता प्रीतम सहित कई बेहतरीन साहित्यिकों की सोहबत में थी, समीक्षाएं एवं अनुवाद कर रही थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी, मुझे किसी की नालायकी पर सोचने की फुर्सत न थी. और ऐसा तो होता नहीं कि लोग सुधरते नहीं, अनिल जनविजय से मेरा विश्वास अभी पूरी तरह टूटा न था.
इस परिचय का सबसे बड़ा फंदा अनिल ने तब डाला, जब मैं 1990 में निर्मल जी के साथ यूरोप घूमने जा रही थी, जर्मनी में उनकी एक कांफ्रेंस के बाद. मेरी टिकट एरोफ्लोट की सस्ती टिकट थी. संयोग से उन्हीं दिनों श्रीमान भारत आये और जब पता चला कि मास्को से ही गुज़र रही हूँ तो कहा, दो दिन रुक कर देख क्यों नहीं लेती. मेरी मूर्खता का यह हाल कि मेरी सोच में भी नहीं आया, यह एक फंदा है.
क्या आप एक साइकोपैथ एट वर्क देख पा रहे हैं? सुना है, इस दौरे की कीमती स्मृतियां भी उन्होंने छपाई हैं!
मेरी इस प्रकरण को भाग 2 तक ले जाने में दिलचस्पी नहीं, हालाँकि अनिल की पत्नी नादया उन दिनों पर ज़्यादा रोशनी डाल सकती हैं. अनिल का उन्हीं दिनों नादया की छोटी बहन के साथ चोरी छिपा संबंध चल रहा था. बाद में उनके और भी मुखौटे उतरे होंगे. क्या ऐसा ही कोई आदमी हमारे परिचय में नहीं होता, जो विश्वास की आड़ में हमारे घर आने का रास्ता बनाता है और एक दिन हमारी बच्ची का शिकार करता है? क्या आप लोग इस चरित्र को पहचानते हैं? इसका विकृत रूप देख सकते हैं?
कुछ अपने बारे में भी. एक अति प्रतिष्ठित परिवार में जन्म होने के कारण मैं सभ्य सुसंस्कृत लोगों के बीच ही बड़ी हुई. मेरी माँ कालेज में प्रिंसिपल थीं, पिता गुरबाणी के विद्वान. मेरा दुर्भाग्य कि हिंदी लेखन में आ गयी. आज जो कीचड़ मैं देख रही हूँ, इसकी कोई कल्पना भी हमें नहीं थी. मेरे परिवारिक पृष्ठभूमि का कुछ ब्यौरा आपको मेरे पिता पर लिखे लेख में मिल सकता है, यदि आप उसे पढ़ें तो. उन दिनों के कॉलेज के मेरे कुछ परिचित उसी स्नेह और सद्भाव में हमारे यहाँ आते थे, घर भी हमारा यूनिवर्सिटी के करीब था. आदरणीय अजित जी, रामदरश जी के स्नेह की स्मृतियां उन्हीं दिनों की हैं.
महत्वाकांक्षा साधने की कोई ज़रूरत न मुझे तब थी, न आज. जिसे कहते हैं, मुंह में चांदी का चम्मच ले कर पैदा हुई थी. वैसे भी, मेरे माता-पिता ने मुझे इतनी तालीम दी है कि स्वाभिमान से अपनी रोटी कमा सकूँ. बाद के वर्षों में एक-दो बड़ी नौकरियां मुझे पलक झपकते ठुकरानी पड़ीं, इसलिए कि वहां काम करने की बौद्धिक आज़ादी नहीं थी, यह जॉइनिंग से पहले ही दिख गया था. इससे भी मैंने कुछ लोगों का दिल ज़रूर दुखाया होगा, विशेष कर जो मुझे घर पर न्योता देने आये थे.
अब श्री अनिल जनविजय के विषय पर. क्या उन बरसों में कभी भी उन्होंने या मैंने ऐसा कुछ कहा, जिसे हम निजी या प्राइवेट कह सकें? इतनी बड़ी गप्प उनकी किस कल्पना में से निकली? इस बीमारी की चपेट में और लोग आये न हों, ऐसा हो नहीं सकता.
बड़े होते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए, कितने लोगों से भेंट होती है, फिर सब अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं. वह क्यों नहीं गए?
आज सार्वजनिक तौर से मुझे उनसे पूछना है, क्या वह अपने आप घर चले जायेंगे? या आप में से कोई उन्हें पहुंचा कर आयेगा? या हमारी अगली पीढ़ी की लड़कियां और लड़के इसका जिम्मा लेंगे?
क्षमा कीजियेगा, इस बार मैं सचमुच महादेवी जी की पंक्ति में बैठने जा रही हूँ. क्या आप जानते हैं, एक कवि सम्मेलन में किसी अकिंचन कवि ने उन पर फब्ती कसी थी – मेरी गोद में बैठ जाओ! उसके बाद वह कभी किसी कवि सम्मेलन में नहीं गयीं. यह बात उन्होंने अपनी दोस्त सुभद्राकुमारी चौहान से कही थी. उन पर लिखी ऑक्सफोर्ड की बायोग्राफी में इसका ज़िक्र है.
मैं भी आपकी चौपाल में कभी नहीं आऊंगी. आप इस अभियुक्त का फैसला जो चाहें, करें.
गगन गिल
1 सितंबर, 2016