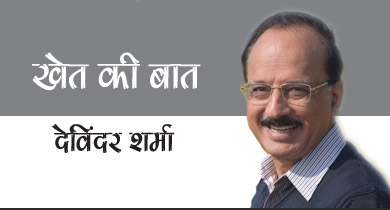किसानों को जीने का हक़ तो मिले !
देविंदर शर्मा
तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी का अचानक हुआ फैसला भारतीय कृषि के भविष्य पर पुनर्विचार, पुनर्रचना और नवाकार संबंधी मनन करने का मौका प्रदान कर रहा है, ताकि सदाबहार क्रांति की नींव रखी जा सके.
इसकी खुशियां मना लेने के बाद, राजनीतिक नेतृत्व के लिए जरूरी हो जाता है कि अर्थव्यवस्था का नया खाका इस उद्देश्य से हो कि कृषि को आर्थिक विकास का शक्तिपुंज बनाया जाए.
नवउदारवादी अर्थशास्त्री इसको लेकर हो-हल्ला मचाएंगे परंतु कृषि को मुनाफादायक, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ बनाना वक्त की जरूरत है.
ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और गैर-टिकाऊ भोज्य तंत्र का विकल्प जल्द तैयार करने की जागरुकता पैदा हो रही है, तब भारत के पास सामर्थ्य है कि खेती को पर्यावरण के हिसाब से सुरक्षित, लोगों एवं धरती के लिए स्वस्थकारी बनाने की रूपरेखा प्रदान करे.
भले देर से ही सही, किंतु कृषि में प्रस्तावित मंडी व्यवस्था को वापस लेने की साहसिक घोषणा करके प्रधानमंत्री ने सुधारात्मक कृषि की दिशा में आरंभिक कदम पहले ही उठा लिया है.
मैं सुधारात्मक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कृषि कानूनों में जो मंडी व्यवस्था प्रस्तावित थी, वे पहले ही बहुत से मुल्कों और महाद्वीपों में असफल सिद्ध हो चुकी है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और चिली से लेकर फिलीपींस तक के फैले विभिन्न देशों में. मुक्त बाजार व्यवस्था ने पहले से मौजूद कृषि संत्रास में केवल इजाफा ही किया है.
चाहे यह अमेरिका, कनाडा हो या कोई अन्य राष्ट्र, वहां-वहां मुक्त मंडी व्यवस्था ने कृषकों को या तो कर्जदार किया है या फिर खेती से बाहर धकेला है, साथ ही कृषि को ग्रीन उत्सर्जन का मुख्य अंशदाता भी बना डाला है. यह मानना कि वही मंडी व्यवस्था भारत में चमत्कार कर दिखाएगी, एक भ्रम है.
उत्तर अमेरिका में उच्च निवेश, नवीनतम तकनीकी खोज, उच्च उत्पादकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूल्य संवर्धन शृंखला सामर्थ्य होने के बावजूद खेती लगातार घटती गई है और यह अधोगति पिछले 150 सालों से जारी है.
वर्ष 2018 में अमेरिकी कृषि विभाग ने हिसाब लगाया था कि कृषि उत्पाद खरीदने को उपभोक्ता द्वारा चुकाए प्रत्येक डॉलर में किसान तक पहुंचने वाला हिस्सा गिरकर महज 8 सेंट तक जा पहुंचा है, लिहाजा उनका वजूद लगातार घटता जा रहा है.
चाहे कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला आगामी चुनावों के मद्देनजर लिया हो या किन्हीं आर्थिक कारणों से, यह जानने के बाद कि मुक्त मंडियां खेती से होने वाली आमदनी बढ़ाने में असफल रही हैं, सार्वजनिक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि तथाकथित सुधारों को दरकिनार कर दिया गया है, इस कदम ने कृषि में नई जान फूंकने और खेती के काम में वापस इज्जत लाने की राह प्रशस्त की है.
आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली की सीमा पर सालभर से, मौसम की तमाम दुश्वारियां झेलते हुए जिस तरह की दृढ़ता दिखाई है, उसने देश का ध्यान कृषक समुदाय की दयनीय हालत की ओर खींचा है. यह वक्त है कि नई नीतियां इस तरह बनाई और पुनर्निधारित की जाएं, जिससे कि ऐसी स्वस्थ कृषि व्यवस्था बने जो, सतत और टिकाऊ रहे.
नये कृषि कानून वापस लेने का फैसला यानी आधी लड़ाई जीतना है. इनको निरस्त करने का मतलब है यथास्थिति पुनः बनना, अर्थात् जिस मौजूदा गंभीर कृषि संकटों के बीच किसान की जिंदगी बीत रही है, उसमें कोई राहत न होना. बेशक आंदोलन के पहले दौर में यह एक जीत है, लेकिन दौड़ अभी बाकी है.
जब तक किसानों को जीने लायक आमदनी का भरोसा न मिल जाए और फसल की कीमत तय करने में मांग-आपूर्ति के ढर्रे वाले सिद्धांत, जिसे बहुत से अर्थशास्त्री किसानों की दुर्दशा का जिम्मेवार ठहराते हैं, को न बदला जाए, वह यूं ही कृषकों का शोषण करता रहेगा. कृषि आय सुनिश्चित किए बगैर भोजन तंत्र का रूपांतर संभव नहीं है. यह वे बदलाव हैं, जिनकी दरकार न केवल भारत, वरन् पूरी दुनिया को बेसब्री से है.
किसान को 23 फसलों पर अपनी उपज का भाव घोषित सरकारी न्यूनतम खरीद मूल्य से लगभग 40 फीसदी कम मिलता है, इससे तो लागत तक नहीं निकलती. जब किसान कोई फसल बोता है, तो उसे यह तक अहसास नहीं होता कि वास्तव में वह घाटा उगा रहा है.
केवल उन इलाकों को छोड़कर, जहां गेहूं, चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था लागू है, बाकी देश में किसानों को यहां तक मालूम नहीं है कि उन्हें किस चीज़ से महरूम रखा जा रहा है.
यह बात वही है, जो आर्थिक सर्वे 2016 ने खुद मानी है, जिसमें बताया गया है कि 17 राज्यों में, यानी लगभग आधे भारत में, किसान की सालाना औसत आय महज 20,000 रुपये है. वस्तुस्थिति आकलन सर्वे-2019 ने हिसाब लगाया है कि फसल उगाकर होने वाली औसत आय महज 27 रुपये प्रतिदिन बैठती है.
न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का कानूनी हक बनाने का मतलब है कि इस निर्धारित भाव से कम किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त न होने पाए, और यही वह असली सुधार है, जिसकी जरूरत भारतीय कृषि को शिद्दत से है. किसान के हाथ में ज्यादा पैसा आने पर न सिर्फ खेती आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनेगी बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पादकता सूचकांक में भी बढ़ोतरी होगी.
इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा, शहरों में रोजगार मुहैया करवाने पर दबाव कम होगा, गांवों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग काफी बढ़ेगी, लिहाजा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिर से जान आएगी. यही समय है, उस गलत धारणा पर टिकी अर्थनीति को उलटने का, जो उद्योगों की एवज में कृषि की बलि देने पर टिकी है. इसकी जगह ऐसी अर्थव्यवस्था बनायी जाए जो लोगों की खातिर काम करे, इसके लिए मानव-पूंजी में निवेश करने की जरूरत है.
हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के बावजूद काफी संख्या में कृषक बाहर छूट जाएंगे. वह छोटे और हाशिए पर आने वाले किसान, जिनके पास बेचने लायक ज्यादा उपज नहीं बचती, लेकिन जो अपने परिवार की अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राहत राशि में सापेक्ष बढ़ोतरी की जाए.
भारत के मौजूदा किसान आंदोलन, जो शायद विश्व का सबसे लंबा चला और विशाल आंदोलन है, ने दुनियाभर का ध्यान खींचा है. किसानों ने पुरानी पड़ चुकी उस आर्थिक सोच को चुनौती देने का साहस किया है, जो खेती को गरीब बनाए रखने पर टिकी है.
यह अपने आप में कोई कम उपलब्धि नहीं है. यदि ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाए तो यह ‘सदाबहार क्रांति’ का बीज बोने का सामर्थ्य रखती है. यह संज्ञा डॉ. एमएस स्वामीनाथन की दी हुई है, इसके तहत कृषि उत्पादन प्रणाली में रिवायती ज्ञान, उपलब्ध जैव विविधता और खेती-बाड़ी के वह तरीके, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, इस्तेमाल किए जाते हैं.
खेती व्यवस्था की पुनर्संरचना करने को मंडियां किसान के पास लाकर ऐसा खाद्य वितरण तंत्र विकसित करना होगा जो किसी परिवार के लिए जरूरी पौष्टिकता सुरक्षा यकीनी बनाए. लेकिन यह प्राप्ति वे लोग नहीं कर सकते, जिन्होंने इस संकट को पैदा किया है.
इसके लिए नई सोच की जरूरत है. इसको संभव बनाने के लिए शुरुआत पहले किसान की जीने योग्य आमदनी बनाकर की जाए.