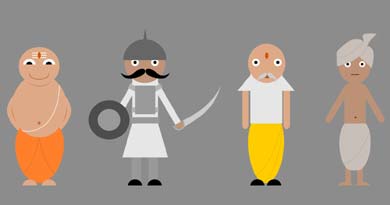जाति, साहित्य और प्रगतिशीलता
अशोक कुमार | फेसबुक : साहित्य वगैरह पर लिखने से बहुत दिनों से बचता हूँ. लेकिन आज लिख रहा हूँ. पिछले लम्बे समय से हिन्दी के साहित्यिक परिक्षेत्र में ऐसे पुरुषों-महिलाओं को देख रहा हूँ जो भीतर से जाति वादी, साम्प्रदायिक और कट्टर हिन्दुत्व के पोषक हैं. आप कुछ हफ्तों इन्हें फॉलो कीजिये और इनका चेहरा दिख जाएगा. लेकिन ऊपरी तौर पर ये प्रगतिशील बने रहते हैं. चूँकि अब भी हिन्दी में प्रगतिशीलता एक मूल्य है और अपनी मूल विचारधारा के साथ इनके अकेले पड़ जाने, नकार दिए जाने का डर है तो कविता-कहानी में ये दाएं-बाएं करके काम चला लेते हैं, भाषा की पच्चीकारी कर लेते हैं, आयोजन करके वरिष्ठ कनिष्ठ प्रगतिशीलों को बुला लेते हैं, भैया-दीदी गैंग बना लेते हैं, पत्रिकाएं निकाल लेते हैं, कूद कूद कर समीक्षाएं लिखते हैं और इस तरह उनके क़रीब पहुँच जाते हैं जिनकी ईमानदारियाँ लगभग असंदिग्ध रही हैं. इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जाता है जिस पर लिखना बकौल सिन्हा साहेब, अशोभनिया होगा.
मुझे उनसे कोई समस्या नहीं. समस्या उनके नाटक से भी नहीं. समस्या है अपने उन सीनियर और समकालीन मित्रों से जो छोटी छोटी लालच में फंस कर या फिर ठकुरसुहाती के चलते इन्हें प्रमोट करते हैं, जबकि अनेक सचमुच के प्रतिबद्ध लेखक उपेक्षित होते हैं. मैं देख पा रहा हूँ साहित्य में ऐसे लोगों का बढ़ता प्रभाव.
फिर सोचता हूँ कि उनसे कोई उम्मीद करने की जगह वैकल्पिक मंच और संस्थान नहीं बनाए जाने चाहिए?
आप बताइए.