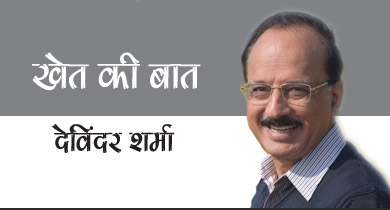निराशा की फसल क्यों उगा रहे किसान?
देविंदर शर्मा
ऐसे समय में जबकि थोक मूल्य मुद्रास्फीति पिछले तीन दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर है, यह कृषि क्षेत्र के लिए मुसीबत भरी खबर है. एक सप्ताह के भीतर, देश में तीन अलग-अलग स्थानों पर, तीन किसानों ने हताशा में अपनी खड़ी फसल अथवा उत्पाद को जला डाला है.
उनकी फसलें अलग थीं, लेकिन जलाने का कारण एक ही है- उचित मूल्य न मिलना, जिससे उत्पादन की वास्तविक लागत पूरी हो.
11 दिसम्बर को आंध्र प्रदेश के कृषक चकालू वेंकटेसव्रलू ने करनूल कृषि उत्पाद मंडी में बेचने के लिए लाये 25 बोरी प्याज (प्रत्येक में 50 किलोग्राम) को आग लगा दी, क्योंकि उसकी बोली महज 500 रुपये प्रति क्विंटल (5 रुपये प्रति किलो) लगी.
उन्हें जब यह समझ में आया कि इतनी कीमत से उपज-लागत, भाड़ा और मंडी फीस तक पूरी नहीं हो रही है तो हताश किसान ने पेट्रोल छिड़क कर अपना उत्पाद जला डाला.
चार दिन बाद आंध्र प्रदेश के धोने मंडल के मल्लिकार्जुन ने तीन एकड़ में लगी केले की फसल को जला दिया क्योंकि मंडी में भाव महज 2-3 रुपये प्रति किलो मिल रहा था.
उनका कहना है कि केला तैयार करने में 5 लाख रुपये की लागत आई, लेकिन तीसरी तुड़ाई होने तक कीमतें इतनी गिरीं कि हौसला टूट गया. बेचने पर महज 1.5 लाख रुपये मिलने थे, मायूसी में खड़ी फसल जलाने के सिवाय कोई चारा न रहा.
मध्य प्रदेश में देओली के कृषक शंकर सिरफिरा ने मंदसौर मंडी में बेचने के लिए लाये 160 किलोग्राम लहसुन को आग लगा दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ.
इसमें उन्होंने बताया कि लहसुन तैयार करने में कुल खर्च आया 2.5 लाख रुपये, पर मंडी में बोली लगी महज 1 लाख रुपये. इतने से तो बुवाई की कीमत तक नहीं निकलती. वह सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए.
ये तीन दुखदायी प्रसंग, जिनका जिक्र मैं यहां कर रहा हूं, असल में इक्का-दुक्का मामले भर नहीं हैं, बल्कि ये असल में यह उस गहरे कृषि संकट का नमूना भर है, जो आज व्याप्त है.
एक ही किस्म की फसल उगाने वाले लाखों किसान होते हैं और उनको भी मंडी में ठीक इसी किस्म के तगड़े झटके लगे होंगे, परंतु उनकी हताशा, लाचारी और नाउम्मीदी सुर्खियां नहीं बन पाई.
जब कीमतें गिरती हैं तब अर्थशास्त्री इसके पीछे ‘मांग-आपूर्ति वाला संतुलन सिद्धांत’ गिनाते हैं, लेकिन इसके एवज में इंसान पर क्या गुजरती है, यह देखने में वे असफल रहते हैं.
न केवल भारत बल्कि विश्व भर में मंडी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव ने किसानों की आजीविका को तहस-नहस किया है, परेशान हो चुके किसान खेती छोड़ने को मजबूर होकर अपनी जमीनें बेच, शहरों में छोटे-मोटे काम कर जिंदा रहने हेतु पलायन करते हैं. यह कोई कम आफत नहीं है.
अमेरिका को लें, वहां भी पिछले 150 साल से उपज की लगाई गई कीमत लगातार नीचे गई है, लिहाजा किसान धीरे-धीरे कृषि से किनारा कर गए.
ग्रामीण अंचल में अजीब-सी असहजता व्याप्त है, न सिर्फ किसानों की आत्महत्या में इजाफा हुआ है बल्कि मानसिक संताप में वृद्धि हुई है.
अमेरिका, जिसका असफल हुआ कृषि-सुधार मॉडल हम उधार ले रहे हैं, वहां 915725 किसान या उनके परिवार सदस्य देश भर के ‘पलायन मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों’ में अवसाद का इलाज करवा रहे हैं. जबकि कुल अमेरिकी आबादी का बमुश्किल 1.5 फीसदी कृषि क्षेत्र में बाकी बचा है.
बेशक इस मानसिक स्थिति के पीछे कुछ अन्य जटिल कारण भी होंगे, जिनका सामना कृषक और कृषि-मजदूरों को करना पड़ रहा है, परंतु ऊपर-नीचे होती उपज की कीमतें सबसे बड़ा कारक है.
लेकिन नीति-नियंताओं और मीडिया, खासकर आर्थिक मामलों के पत्रकारों को उथल-पुथल तभी दिखाई देती है, जब शेयर सूचकांक अचानक नीचे लुढ़के और स्टॉक मार्किट निचले स्तर पर बंद हो. यही वह सांचा है, जिसमें अर्थशास्त्र को ढाला गया है.
मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों का बड़ा तबका स्टॉक मार्किट में गिरावट आने पर तो शोक मनाता है किंतु कृषि उत्पाद को मिलने वाली कम कीमतों का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता. अंततः कृषि क्षेत्र में कर्ज बढ़ता है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा किसान खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन करते हैं.
कोई हैरानी नहीं कि किसानों को हर साल 23 फसलों पर घोषित सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देकर न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के संभावित कदम के विरुद्ध पहले ही उनके खंजर निकल आए हैं.
कुछ वरिष्ठ अर्थशास्त्री, जिन्हें खुद को हर महीने वेतन-महंगाई भत्ता जुड़कर- मिलने की गारंटी है, वे मुक्त कृषि मंडी व्यवस्था की पैरवी कर रहे हैं. उनके मुताबिक यह किसान को बेहतर कीमत खोजने में सहायक होगी.
मैंने पहले भी अपने लेखों में बताया है कि अत्यधिक प्रचलित पदार्थ जैसे कि चॉकलेट और कॉफी के मामलों में लैटिन अमेरिका के कोको बीन उत्पादक और अफ्रीका में कॉफी बीन उगाने वाले करोड़ों किसान अत्यंत गरीबी की हालत में जी रहे हैं.
केले की मूल्य-संवर्धन श्रृंखला से भी जिस तरह किसानों की आमदनी सिकुड़ी है, वह कम आंखें खोलने वाला नहीं है. एक अध्ययन बताता है कि यूरोपियन बाजारों में बिकने वाले लैटिन अमेरिकी केले के मूल उत्पादक तक उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए प्रत्येक यूरो का महज 5-9 प्रतिशत पहुंचता है.
भोजन श्रृंखला में यह मूल उत्पादक ही है, जिसकी भूमिका सबसे कठिन है, वही कड़ी मेहनत करता है, फिर भी मूल्य संवर्धन श्रृंखला से प्राप्त आमदनी में उसके पल्ले न्यूनतम पड़ता है, लागत तक नहीं निकलती.
यहां सनद रहे कि तीन महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों- कॉफी, केला और कोको पर न तो कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य है न ही किसी किस्म की कृषि उत्पाद खरीद मंडी व्यवस्था है, जिस पर हम इस स्थिति के लिए अंगुली उठा सकें. असल में ये प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो किसानों के हिस्से का पैसा चूसकर अमीर हो रही हैं.
ज़रा सोचें, यदि वैश्विक कृषि श्रृंखला ने उत्पादन लागत और उचित मुनाफा जोड़कर किसान को न्यूनतम खरीद मूल्य मिलना सुनिश्चित किया होता तो आज खेती भी एक लाभदायक व्यवसाय होता.
दोहन करने वाली मंडी शक्तियों को खुली छूट देने के बजाय, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सुबूत निर्णायक रूप में सिद्ध करते हैं, भारत के लिए यही समय है कि अपने बनाये खेती सुधारों का नया प्रारूप लागू कर सर्वप्रथम किसान को जीने लायक आमदनी सुनिश्चित करे.
देश की कुल जनसंख्या के लगभग 50 फीसदी हिस्से को आर्थिक रूप से व्यवहार्य एक आजीविका की गारंटी बनाना, आर्थिक असमानता में व्याप्त बड़े अंतर को पाटने का एक उपाय होगा.