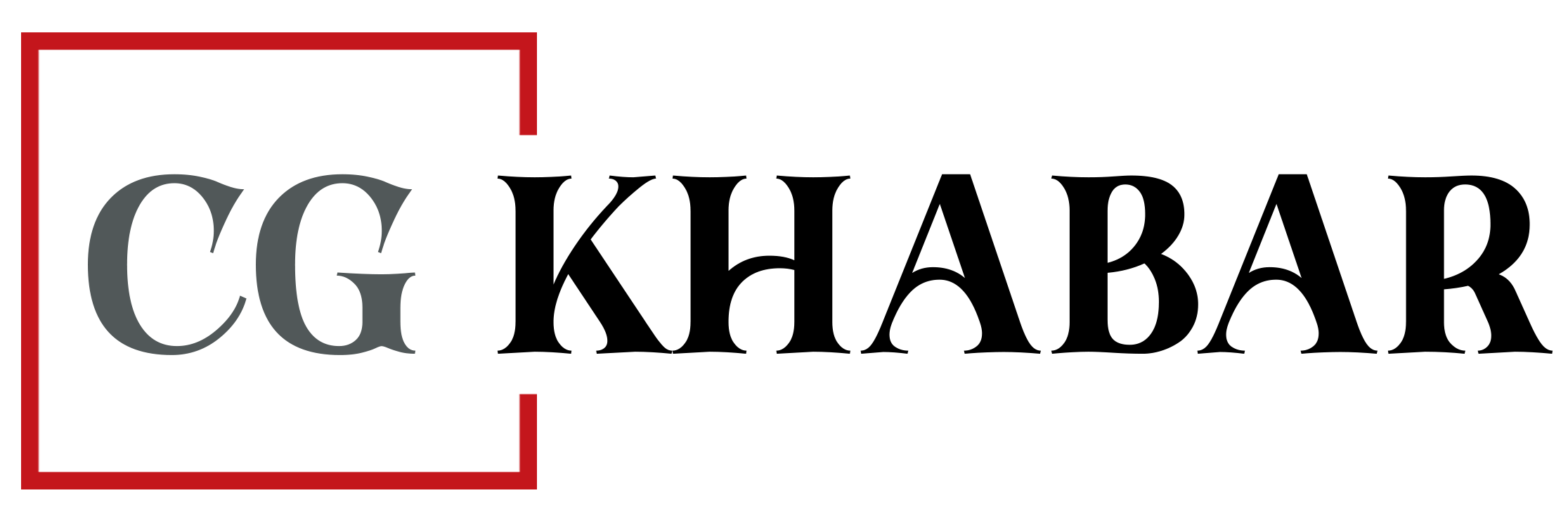पश्चिम में बुर्के के खिलाफ सोच
सुनील कुमार
ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पार्टी के एक भूतपूर्व मंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर एक बयान देकर अपनी पार्टी को दुविधा में डाल दिया है, और पार्टी ने इस बयान से किनारा भी कर लिया है. बोरिस ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बुर्का पहनी हुई महिलाएं लैटरबॉक्स की तरह लगती हैं (मानो आंखों की खुली जगह चिट्ठी डालने के लिए बनी हो), या बैंक डकैतों जैसी लगती हैं. इस बात को पार्टी की घोषित रीति-नीति के खिलाफ माना गया, और सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर यह बात भी चल रही है कि क्या अपने इस नेता की सोच को ठीक करने के लिए उसे किसी परामर्श केन्द्र भेजा जाए.
दूसरी तरफ कुछ दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि योरप के कुछ देशों ने बुर्के के खिलाफ कानून बना लिया है, और ब्रिटेन को भी ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए बोरिस जॉनसन को अपने बयान पर न अफसोस जाहिर करना चाहिए, न माफी मांगनी चाहिए.
मिस्टर बीन के किरदार के विख्यात एक कलाकार रोवान एटकिनसन ने बोरिस जॉनसन के बयान का समर्थन किया है, और कहा है कि अगर कोई लतीफा खराब है, तो ही आपको माफी मांगनी चाहिए, और उस पैमाने पर इस बुर्का-बयान के लिए बोरिस को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है. इस अभिनेता ने चिट्ठी लिखकर कहा है- पूरी जिंदगी मैं धर्म के बारे में लतीफे बनाने की आजादी का मजा लेते रहा, और मेरा कहना है कि बोरिस जॉनसन का बुर्के वाला लतीफा खासा अच्छा था. धर्म के बारे में सारे ही लतीफे लोगों को आहत करते हैं, इसलिए उनके बारे में किसी को माफी नहीं मांगनी चाहिए. माफी तो तब मांगनी चाहिए जब लतीफा खराब हो.
यह अभिनेता इसके पहले भी अभिव्यक्ति की आजादी के अभियान में शामिल रहा है, और बरसों तक उसने ऐसे एक कानून के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ था जो कि धार्मिक भावनाएं भड़काने को अपराध बनाने वाला था. उसका कहना था कि ऐसे कानून से बोलने की आजादी खत्म होती है. किसी धर्म की आलोचना एक बुनियादी अधिकार है.
इन बयानों की बात अगर छोड़ दें तो एक बुनियादी बात यह रह जाती है कि बुर्के पर रोक लगानी चाहिए या नहीं? योरप के कुछ देशों ने ऐसा किया है, और अपनी संसद से कानून बनाकर किया है, वहां की अदालतों में भी यह कानून जायज ठहराया गया है. इन देशों का तर्क है कि वहां की संस्कृति में सार्वजनिक जगहों पर बुर्के से एक अलग किस्म का भेदभाव पैदा होता है जो कि सामाजिक समरसता के खिलाफ है. कुछ देशों का यह भी तर्क है कि महिला पर ही लादे गए ऐसे नियम से महिलाओं का समानता का अधिकार खत्म होता है जो कि इन देशों में संविधान के तहत दी गई औरत-मर्द की समानता की गारंटी के खिलाफ है.
हाल के बरसों में, या यह कहें कि पिछले दो दशकों में दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोगों के रीति-रिवाज सहित उनकी धार्मिक मान्यताओं के दीगर पहलुओं पर बहस बढ़ती चली गई है क्योंकि बाकी दुनिया में बाहर से गए हुए मुस्लिमों का समाज में घुलना-मिलना इससे प्रभावित हो रहा था. बहुत से ईसाई या गोरे देशों में, पश्चिमी संस्कृतियों में बुर्के या हिजाब, नकाब या किसी और किस्म के पर्दे को लेकर वहां की स्थानीय बहुसंख्यक संस्कृति की नापसंदगी, शरणार्थियों या आप्रवासियों के लिए नापसंदगी की एक बड़ी वजह बन रही थी. दूसरी बात यह कि दुनिया में हो रहे बहुत से आतंकी हमलों के पीछे मुस्लिम आतंकी समूहों का हाथ होने से भी बहुत सी जगहों पर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा था.
मुस्लिमों या इस्लाम से दहशत की एक वजह यह भी थी कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, या पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में मुस्लिम आतंकी संगठन जिस दर्जे की हिंसा कर रहे थे, वैसी हिंसा इक्कीसवीं सदी में किसी और जगह पर देखी नहीं गई थी, इसलिए भी योरप और पश्चिम के देशों में इन देशों से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ दहशत और नापसंदगी का मिलाजुला प्रतिरोध सामने आ रहा था. कई जगहों पर मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम महिलाओं के हिमायती लोग भी यह चाहते थे कि मुस्लिम लोगों के बीच की इस पर्दा प्रथा को खत्म किया जाए, और मुस्लिम औरत को बराबरी के हक दिलवाए जाएं. इसी सोच के साथ योरप के कुछ देशों ने ऐसे कानून बनाए. 
यह बुनियादी सवाल आसान नहीं है कि बुर्का मुस्लिम महिला की अपनी पसंद की आजादी का प्रतीक है, या कि उसकी गुलामी का. अगर हम किसी धर्म के दायरे से बाहर निकलकर सोचें तो यह लगता है कि संभावनाओं को सीमित करने वाला ऐसा बोझ अगर केवल महिलाओं पर लादा गया है, और धर्म के बाकी रीति-रिवाजों, सामाजिक संस्कृतियों में भी केवल महिला के हक ही कम रखे गए हैं, तो यह गैरबराबरी की सोच से उपजा हुआ बोझ है, और यह किसी भी हालत में किसी महिला की पसंद नहीं हो सकता. मुस्लिम समाज के भीतर के कुछ लोग यह जरूर कह सकते हैं कि योरप के देशों में भी कानून बनाने के पहले यह सोचना चाहिए कि मुस्लिम महिला अगर अपनी पसंद से बुर्का पहनना चाहती है, तो उसे उसकी आजादी होना चाहिए.
अब सवाल यह उठता है कि एक वक्त भारत के हिन्दू समाज में महिला को सती होने की आजादी हासिल थी. लेकिन सामाजिक हकीकत यह थी कि महिला अपने गुजरे हुए पति की चिता पर खुद होकर चढऩा चाहे या नहीं, उसे पारिवारिक और सामाजिक दबाव के तहत चढ़ा दिया जाता था, और जला दिया जाता था. इसी तरह हिन्दू समाज में बाल विवाह कायम था, और इसे मां-बाप का हक माना जाता था कि वे अपने छोटे-छोटे बच्चों की शादी कर दें. लेकिन कानून बनाकर इन दोनों बातों को रोकना पड़ा क्योंकि समाज के रीति-रिवाज दकियानूसी और हिंसक अधिक रहते हैं, लोकतांत्रिक, मानवीय, और संवेदनशील कम रहते हैं. ऐसे रीति-रिवाज बहुत से समाजों में कायम हैं, और अभी-अभी जैन समाज के भीतर लगातार यह बात उठ रही है कि कमउम्र के बच्चों का सन्यास लेना तो बंद करना ही चाहिए, कमउम्र के बच्चों को छोड़कर सन्यासी बनने वाले मां-बाप के सन्यास पर भी रोक लगना चाहिए.
हिन्दुस्तान से फिलीस्तीन तक के महीने भर के सड़क सफर में मेरा यह देखना हुआ था कि ईरान, टर्की, सीरिया, इजिप्ट और फिलीस्तीन जैसे बहुत से देशों में छोटे-छोटे बच्चों को भी बुर्का या हिजाब पहनाकर स्कूल भेजा जाता है, और पोशाक के मामले में एक गैरबराबरी इन तमाम मुस्लिम देशों में कायम थी. धीरे-धीरे ऐसे सामाजिक माहौल में लड़कियों या महिलाओं को यह भी लग सकता है कि वे इसी में सुरक्षित हैं, और यह उन पर बोझ नहीं है, यह उनका हक है. लेकिन हकीकत तो यही है कि महज महिलाओं के लिए बनाए गए ऐसे पोशाक-नियमों से उनकी आगे बढऩे की संभावनाएं कम होती हैं, वे गैरबराबरी की वजह से पिछड़ती हैं.
लैटरबॉक्स या बैंक डकैत जैसी संवेदनाशून्य भाषा को अगर छोड़ भी दें, तो यह दुनिया के सभी समाजों की जिम्मेदारी है कि वे धार्मिक या सामाजिक आधार पर जहां-जहां औरत या मर्द में भेदभाव किया जाता है, उसे खत्म करने की कोशिश करें. इसके तौर-तरीके अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों का यह मानना हो सकता है कि इसे मुस्लिम महिला की निजी पसंद-नापसंद पर छोड़ दिया जाए, लेकिन जो देश समानता को राजनीतिक हौसले के साथ लागू करने की समझ रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे मुस्लिम महिला को इससे आजादी दिलाएं. बोझ किसी की पसंद नहीं हो सकता, और एक वक्त तो वह भी था जब अलग-अलग बहुत से धर्मों के समुदायों में तरह-तरह की हिंसा को कानूनी मंजूरी थी, और अमरीका जैसे देश में भी महिलाओं को वोट डालने का हक नहीं था. महज सामाजिक बदलाव से हालात नहीं सुधरते, उसके लिए कई बार कानून की भी जरूरत पड़ती है.
अभी जब यह कॉलम लिखा ही जा रहा है, तभी ब्रिटेन से एक खबर आई है कि वहां एक मुसाफिर बस में एक गोरे ड्राइवर ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे को ढांके हुए निकाब पर आपत्ति की, और उसे हटाने के लिए कहा. इस बात का भूतपूर्व ब्रिटिश मंत्री के छेड़े गए विवाद से सीधा-सीधा रिश्ता दिखता है कि उस बात की वजह से यह नया तनाव खड़ा हो रहा है.
इन तमाम बातों से परे, दुनिया के इतिहास में एक दिलचस्प मामला दर्ज है जिसे स्टॉकहोम सिन्ड्रोम कहते हैं. स्वीडन के स्टॉकहोम में 1973 में एक बैंक डकैती हुई, और डकैतों ने अपने एक साथी को जेल से रिहा कराने के लिए जेल के तिजोरी के भीतर ही कई लोगों को छह दिन तक कैद करके रखा ताकि उनकी जान की कीमत पर जेल से रिहाई कराई जा सके. डकैत इन लोगों को फांसी का फंदा और डायनामाइट दिखाकर-डराकर भी रख रहे थे. उसके बाद जब इन लोगों की रिहाई हुई, तो इनमें से किसी ने भी इन डकैतों के खिलाफ बयान देने से इंकार कर दिया, बल्कि उनके मुकदमे के लिए पैसे जुटाने में भी लग गए.
बाद में मनोवैज्ञानिकों ने उनकी दिमागी हालत का अध्ययन किया और पाया कि इस कैद के शिकार लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें कैद करके रखने वाले लोगों के साथ ऐसी हमदर्दी विकसित कर ली थी कि उनकी जान बच सके. और बाद में यह हमदर्दी रिहाई के बाद भी जारी रही. इसे ही तब से अब तक स्टॉकहोम सिन्ड्रोम कहा जाता है जिसमें कैद करके रखने वाले लोगों के साथ कैद किए गए लोगों की हमदर्दी हो जाती है. यह मिसाल कुछ अटपटी सी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ मामलों में लोगों को उनके साथ होती ज्यादती का अंदाज नहीं लगता, और वे ज्यादती के बावजूद अपने उस हाल को पसंद करने लगते हैं. महिलाओं के बारे में यह समझने की जरूरत है कि क्या वे बुर्का या हिजाब पहनने, या सती होने, या घूंघट निकालने को स्टॉकहोम सिन्ड्रोम की तरह अपने भले के लिए मानने लगी हैं!
* लेखक वरिष्ठ पत्रकार और शाम के अखबार छत्तीसगढ़ के संपादक हैं.