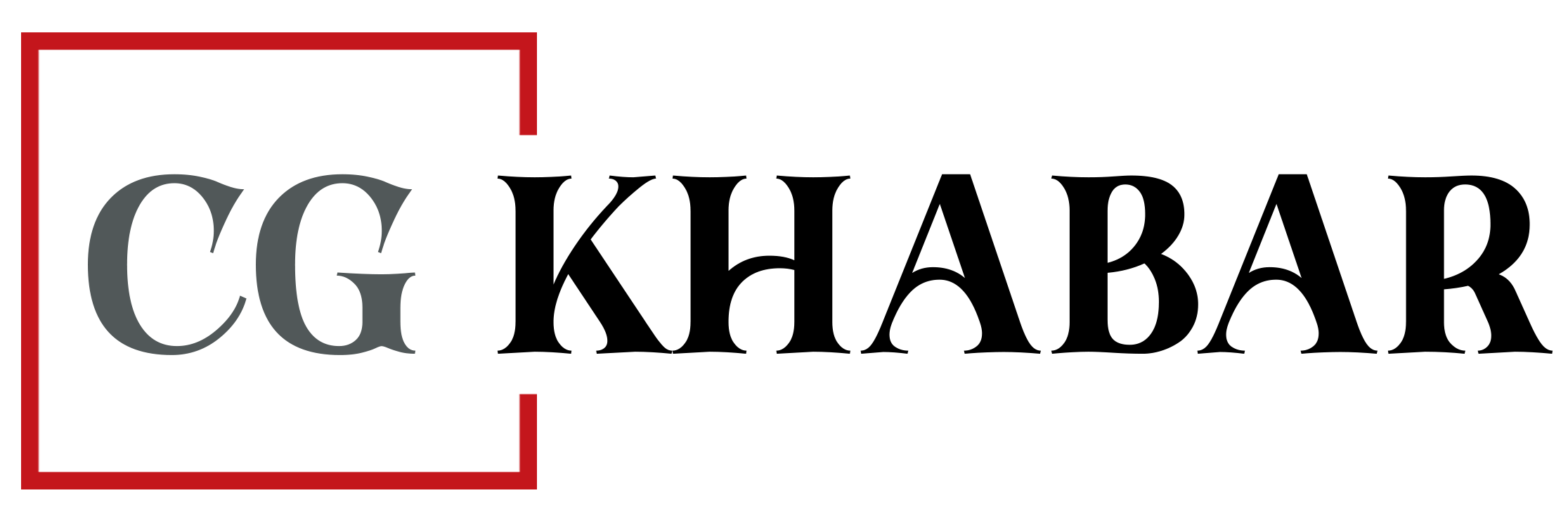वेलेंटाइन डे पर भगतसिंह की फांसी का झूठ
नई दिल्ली | संवाददाता: वेलेंटाइन डे पर क्या भगत सिंह को फांसी हुई थी या उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहस जारी है और दुष्प्रचार करने वालों अपढ़, कूपढ़ और शातिरों की एक पूरी फौज इसे सही साबित करने में जुटी हुई है.
हकीकत ये है कि भगत सिंह को न तो वेलेंटाइन डे के दिन फांसी हुई थी और ना ही उन्हें इस तारीख को फांसी की सजा सुनाई गई थी. लेकिन पिछले कुछ सालों से यह अफवाह फैला कर 14 फरवरी के दिन वेलेंटाइन डे का बहिष्कार करने और मातृ पितृ पूजन मनाने की अपील परवान चढ़ी हुई है.
दस्तावेज़ों की मानें तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ चलाये गये मामले का ट्रायल 5 मई 1930 को शुरु हुआ था और उन्हें 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी. इन तीनों नौजवानों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी.
हां, 13 फरवरी की तारीख के साथ भगत सिंह का एक रिश्ता जरुर है. इस दिन ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में 13 फ़रवरी, 1930 को उनका एक पत्र जरुर प्रकाशित हुआ है. पाठकों के लिये भगत सिंह का यह प्रासंगिक पत्र हम भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज़ से साभार प्रस्तुत कर रहे हैं.
स्पेशल मजिस्ट्रेट, लाहौर के नाम
द्वारा, सुपरिण्टेण्डेण्ट, सेण्ट्रल जेल, लाहौर
11 फ़रवरी, 1930
मिस्टर मजिस्ट्रेट,
4 फ़रवरी, 1930 के सिविल एण्ड मिलिट्री गजट में प्रकाशित आपके बयान के सम्बन्ध में यह ज़रूरी जान पड़ता है कि हम अपने अदालत में न आने के कारणों से आपको परिचित करवायें, ताकि कोई ग़लतफ़हमी और ग़लत-प्रस्तुति सम्भव न हो.
पहले हम यह कहना चाहेंगे कि हमने अभी तक ब्रिटिश अदालतों का बायकाट नहीं किया है. हम मि. लुइस की अदालत में जा रहे हैं, जो हमारे विरुद्ध जेल एक्ट धारा 22 के अधीन मुक़दमे की सुनवाई कर रहे हैं. यह घटना 29 जनवरी को आपकी अदालत में घटित हुई थी. लाहौर षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में यह क़दम उठाने के लिए हमें विशेष परिस्थितियों ने मजबूर किया है. हम शुरू से ही महसूस करते रहे हैं कि अदालत के ग़लत रवैये द्वारा या जेल के अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा हमारे अधिकारों की सीमा लाँघकर हमें निरन्तर जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है ताकि हमारी पैरवी में बाधाएँ डाली जा सकें. कुछ दिन पहले जमानत की दरख़्वास्त में हमने अपनी तकलीफ़ें आपके सामने रखी थीं, लेकिन उस दरख़्वास्त को कुछ क़ानूनी नुक्तों पर नामंज़ूर करते हुए आपने बन्दियों की तकलीफ़ों का ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं समझा, जिनके आधार पर जमानत की दरख़्वास्त दी गयी थी.
हम महसूस करते हैं कि मजिस्ट्रेट का पहला व मुख्य फ़र्ज़ यह होता है कि उसका व्यवहार निष्पक्ष व दोनों पक्षों के ऊपर उठा होना चाहिए. यहाँ तक कि उस दिन माननीय जस्टिस कोर्ट ने यह रूलिंग दी थी कि मजिस्ट्रेट को दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण बात अपने सामने रखनी चाहिए कि विचाराधीन क़ैदी को अपनी पैरवी के सम्बन्ध में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े और यदि कोई मुश्किल हो तो उसे दूर करना चाहिए, अन्यथा पूरा मुक़दमा एक मज़ाक़ बनकर रह जाता है. लेकिन ऐसे महत्त्वपूर्ण मुक़दमे में मजिस्ट्रेट का व्यवहार इससे उल्टा रहा है, जिसमें 18 नवयुवकों पर गम्भीर आरोपों जैसे हत्या, डकैती और षड्यन्त्र -के अधीन मुक़दमा चलाया जा रहा है, जिनसे सम्भव है उन्हें मृत्युदण्ड दिया जाये. जिन प्रमुख मुद्दों पर हम आपकी अदालत में न आने के लिए विवश हुए हैं, वे इस तरह हैं-
विचाराधीन क़ैदियों में से अधिकांश दूर-दराज प्रान्तों से हैं और सभी मध्य वर्गीय लोग हैं. ऐसी स्थिति में उनके सम्बन्धियों द्वारा उनकी पैरवी के लिए बार-बार आना न सिर्फ़ बहुत मुश्किल है, बल्कि बिल्कुल असम्भव है. वे अपने कुछ दोस्तों से मुलाक़ात करना चाहते थे, जिन्हें वे अपनी पैरवी की सभी ज़िम्मेदारियाँ सौंप सकते थे. साधारण बुद्धि का भी यही तक़ाज़ा है कि उन्हें मुलाक़ात करने का हक़ हासिल है, इस मक़सद के लिए बार-बार प्रार्थना की गयी, लेकिन सभी प्रार्थनाएँ अनसुनी रहीं.
श्री बी.के. दत्त बंगाल के रहने वाले हैं और श्री कमलनाथ तिवारी बिहार के. दोनों अपनी-अपनी मित्र कुमारी लज्जावती व श्रीमती पार्वती से भेंट करना चाहते थे. लेकिन अदालत ने उनकी दरख़्वास्त जेल-अधिकारियों को भेज दी और उन्होंने यह कहकर दरख़्वास्त रद्द कर दी कि मुलाक़ात सिर्फ़ सम्बन्धियों व वकीलों से ही हो सकती है. यह मामला बार-बार आपके ध्यान में लाया गया, लेकिन ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया गया, जिससे बन्दी पैरवी के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकते. बाद में उन्हें इनका वकालतनामा हासिल करने पर भी मुलाक़ात करने की आज्ञा नहीं दी गयी और यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट ने जेल-अधिकारियों को यह लिखने से भी इन्कार कर दिया कि बन्दी उसकी ओर से चलाये जा रहे मुक़दमे की पैरवी के सम्बन्ध में इन मुलाक़ातों की माँग कर रहे थे और इस प्रकार बन्दी ऊपर की अदालत में जाने योग्य नहीं रहे. लेकिन मुक़दमे की सुनवाई जारी रही. इन परिस्थितियों में बन्दी बिल्कुल विवश थे और उनके लिए मुक़दमा मज़ाक़ से अधिक कुछ नहीं था. यह बात नोट करने योग्य है कि दूसरे बन्दियों में भी अधिकांश की ओर से कोई वकील पेश नहीं हो रहा था.
मेरा कोई वकील नहीं है और न ही मैं पूरे समय के लिए किसी को वकील रख सकता हूँ. मैं कुछ नुक्तों सम्बन्धी क़ानूनी परामर्श चाहता हूँ और एक विशेष पड़ाव पर मैं चाहता था कि वे (वकील) कार्रवाई को स्वयं देखें, ताकि अपनी राय बनाने के लिए वे बेहतर स्थिति में हों, लेकिन उन्हें अदालत में बैठने तक की जगह नहीं दी गयी. हमारी पैरवी रोकने के लिए, हमें परेशान करने के लिए क्या सम्बन्धित अधिकारियों की यह सोची-समझी चाल नहीं थी? वकील अपने सायलों (प्रार्थियों) के हितों को देखने के लिए अदालत में आता है, जो न तो स्वयं उपस्थित होते हैं और न उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ होता है. इस मुक़दमे की ऐसी कौन-सी विशेष परिस्थितियाँ हैं, जिससे मजिस्ट्रेट वकीलों के प्रति ऐसा सख़्त रवैया अपनाने पर मजबूर हुए? इस प्रकार हर उस वकील की हिम्मत तोड़ी गयी जो बन्दियों को मदद के लिए बुलाये जा सकते थे. श्री अमरदास को पैरवी (डिफ़ेंस) की कुर्सी पर बैठने की इजाज़त देने की क्या तुक थी, जबकि वे किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे और न ही उन्होंने किसी को क़ानूनी परामर्श दिया. अपने मुख़्तारों से मुलाक़ातों के सम्बन्ध में मुझे क़ानूनी सलाहकार से विचार-विमर्श करना था और इसी नुक्ते को लेकर हाईकोर्ट जाने के लिए उनसे कहना था. लेकिन उनके साथ इस सम्बन्ध में बात करने का मुझे कोई अवसर ही नहीं मिला और कुछ न हो सका. इस सबका क्या मतलब है? यह दिखाकर कि मुक़दमा क़ानून के अनुसार चलाया जा रहा है, क्या लोगों की आँखों में धूल नहीं झोंकी जा रही? अपने बचाव का इन्तज़ाम करने के लिए बन्दियों को क़तई कोई अवसर नहीं दिया गया. इस बात के ख़िलाफ़ हम रोष प्रकट करते हैं. यदि सबकुछ उचित ढंग से नहीं किया जाता तो इस तमाशे की कोई ज़रूरत नहीं है. न्याय के नाम पर हम अन्याय होता नहीं देख सकते. इन परिस्थितियों में हम सभी ने सोचा कि या तो हमें अपनी ज़िन्दगी बचाने का उचित अवसर मिलना चाहिए, और या हमें हमारी अनुपस्थिति में चले मुक़दमे में हमारे ख़िलाफ़ दी सज़ाओं को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए.
तीसरी बड़ी शिकायत अख़बारों के बाँटने सम्बन्धी है. विचाराधीन क़ैदियों को कभी भी दण्ड प्राप्त क़ैदी नहीं माना जाना चाहिए और यह रोक उन पर तभी लगायी जा सकती जब उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हो. इससे अधिक इसे उचित नहीं माना जा सकता. जमानत पर रिहा न हो सकने वाले बन्दी को कभी भी दण्ड के तौर पर कष्ट नहीं देने चाहिए. सो प्रत्येक शिक्षित विचाराधीन क़ैदी को कम से कम एक अख़बार लेने का अधिकार है. अदालत में ‘एक्ज़ीक्यूटिव’ कुछ सिद्धान्तों पर हमें हर रोज़ एक अंग्रेज़ी अख़बार देने के लिए सहमत हुई थी. लेकिन अधूरी चीज़ें न होने से भी बुरी होती हैं. अंग्रेज़ी न जानने वाले बन्दियों के लिए स्थानीय अख़बार देने के अनुरोध व्यर्थ सिद्ध हुए. अतः स्थानीय अख़बार न देने के आदेश के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए हम दैनिक ट्रिब्यून लौटाते रहे हैं.
इन तीन आधारों पर हमने 29 जनवरी को अदालत में आने से इन्कार करने की घोषणा की थी. ज्यों ही ये मुश्किलें दूर कर दी जायेंगी, हम बाख़ुशी अदालत में आयेंगे.
भगतसिंह व अन्य