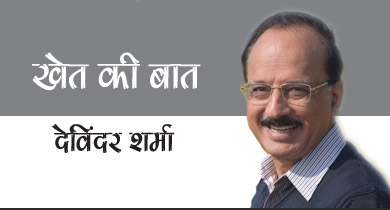सूखे का संकट और नीतियां
उत्सा पटनायक
देश के विशाल हिस्से और खासतौर पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, बुंदेलखंड तथा यहां तक कि पंजाब में भी विशाल हिस्से को जिस तरह से गंभीर सूखे ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उस का मीडिया में काफी व्यापक पैमाने पर कवरेज हुआ है. अनेक इलाकों में लगातार दूसरे साल गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है. इस साल के विपरीत, पिछले साल अनेक इलाकों को बेमौसमी बारिश के चलते फसलों के भारी नुकसान की समस्या का सामना करना पड़ा था. बहुत से इलाकों में तो इंसानों और मवेशियों, दोनों के ही खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जिसके चलते मुसीबत के मारे लोगों का पलायन आम दृश्य हो गया है.
सूखा और खेती का संकट
सूखे के सिलसिले में अब तक ज्यादातर बहस सरकार द्वारा उठाए गए राहत के कदमों की अपर्याप्तता और मनरेगा के दायरे का विस्तार करने की तो बात ही क्या है, उसकी मजदूरी के बकाया का भुगतान करने के प्रति भी सरकार की उदासीनता तक ही सीमित रही है. बेशक, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है, फिर भी यह समझना जरूरी है कि पिछले कुछ अर्से में सरकारों द्वारा सोचे-समझे तरीके से जो दीर्घावधि नीतिगत कदम उठाए गए हैं तथा आज भी अपना काम कर रहे हैं, व्यावहारिक मानों में उसी तरह के नतीजे सुनिश्चित करने वाले कदम थे, जैसे नतीजे हम आज देख रहे हैं.
हमारे देश में सूखा समय-समय पर पड़ता ही है. ग्रामीण आबादी इस सचाई से भली-भांति परिचित है. इसलिए, असली सवाल यह है कि क्यों और किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की इसकी सामर्थ्य को ही कमजोर किया गया है कि जब-तब पड़ने वाले सूखे से निपट पाती और उससे जुड़ी कामगार आबादी का सुरक्षित रहना तथा पुनरुत्पादन सुनिश्चित कर पाती, जो समूची अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है.
आज हमारे देश में ग्रामीण आबादी, स्वतंत्रता के समय रही भारत की कुल आबादी से दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है. तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इस बीच ग्रामीण आबादी, कुल आबादी के 83 फीसद से घटकर, 70 फीसद पर आ गयी है. कृषि पर निर्भर आबादी का हिस्सा भी घट गया है. इसके बावजूद भारत अब भी, ज्यादातर बड़े एशियाई देशों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रबलता के साथ कृषि-प्रधान बना रहा है. 1990 में आर्थिक सुधार तथा व्यापार उदारीकरण के शुरू होने के बाद से जो नया रुझान देखने को मिल रहा है, ग्रामीण आबादी के पहले के मुकाबले और तेजी से सर्वहाराकरण का ही रुझान है. जहां 1951 से 1991 तक के चार दशकों के दौरान, ग्रामीण श्रम शक्ति में मजदूरी पर काम करने वालों के अनुपात में 12 फीसद अंक की बढ़ोतरी हुई थी और यह 28 से बढक़र 40 फीसद पर पहुंच गया था, 1991 के बाद के दो दशकों में ही इसमें 15 फीसद अंक की और बढ़ोतरी हो गयी और मजदूरी करने वालों का हिस्सा ग्रामीण श्रम शक्ति में 55 फीसद हो गया.
संक्षेप में यह कि उजरती मजदूरों की संख्या और अनुपात, दोनों में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है. दूसरे सिरे पर, इसी हिसाब से काश्तकारों का हिस्सा घटता गया है. इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार, ग्रामीण श्रम शक्ति में मजदूरों की संख्या काश्तकारों की संख्या से आगे निकल गयी है और थोड़ी-बहुत नहीं काफी ज्यादा आगे निकल गयी है.
तूफानी रफ्तार से दरिद्रीकरण
कहने की जरूरत नहीं है कि तेजी से सर्वहाराकरण की इस प्रक्रिया को मुख्यत: दरिद्रीकरण की प्रक्रिया कहना ही ज्यादा सही होगा. यह दरिद्रीकरण, खेतिहर काश्तकारों पर उस चौतरफा हमले का नतीजा है, जो 1990 से लागू की जा रही नवउदारवादी सुधार की नीतियों में अंतर्निहित है. इस हमले का नतीजा यह हुआ है कि खेती के साथ लगे जोखिम में भारी बढ़ोतरी हुई है, किसानों के डूबे हुए कर्जों में भारी बढ़ोतरी हुई है. इसके चलते बड़ी संख्या में काश्तकारों ने अपनी जमीन गंवायी है. इस तरह हमारी अर्थव्यवस्था के इस सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक आधार की वहनीयता ही खतरे में पड़ गयी है.
ग्रामीण आबादी की हालत बदतर होने का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपभोग के आंकड़े का नीचे खिसकना. प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपभोग का मौजूदा स्तर, 1937-41 के दौर के उसके स्तर से भी नीचे चला गया है. सचाई यह है कि अब भारत की आबादी का कुल खाद्यान्न उपभोग, जिसमें भोजन, बीज, पशु-आहार, खराबा, प्रसंस्करण तथा औद्योगिक उपयोग, सब शामिल हैं, 176 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष के स्तर पर चला गया है, जो दुनिया भर में इसका सबसे निचला स्तर है. यह स्तर, अफ्रीका के 225 किलोग्राम के औसत से कम है और सबसे कम विकसित देशों के 212 किलोग्राम के औसत से भी नीचे है. एक और कुख्यात सूचकांक, आम आबादी की तुलना में, किसानों की आत्महत्याओं का अनुपात ज्यादा होना है. जाहिर है कि ये किसानों की ये आत्महत्याएं, ऋण के बोझ की वजह से हो रही हैं.
इस तरह के हालात हमारे देश के आर्थिक इतिहास के अध्येताओं को काफी जाने-पहचाने लगते हैं. इन हालात ने स्वतंत्रता से पहले पचास वर्षों की याद खासतौर पर ताजा कर दी है. उस दौर में भी प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपभोग में भारी गिरावट हुई थी. विश्व मंदी के दौर में खेती की पैदावार के दाम में गिरावट के चलते, काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज के बोझ के नीचे दब गए थे और बड़े पैमाने पर अपनी जमीनें खो बैठे थे. तब भी श्रमशक्ति में मजदूरों का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा था और आबादी का पोषण का स्तर तेजी से गिरा था. लेकिन अब, जबकि भारत को आजादी मिल चुकी है, वही सब क्यों दोहराया जा रहा है? इस सवाल का जवाब इस तथ्य में निहित है कि जिस तरह आजादी से पचास साल पहले तक का दौर, विकसित दुनिया की जरूरतें पूरी करने के लिए, भारतीय खेती के अंधाधुंध शोषण के जारी रखे जाने को दिखाता था, उसी तरह अब 1990 से अपनायी गयी नयी आर्थिक नीतियां भी, विकसित दुनिया के सुपरमार्केटों के शैल्फों को भरने के लिए, हमारी खेती पर नियंत्रण हासिल करने की नव-साम्राज्यवादी कोशिशों को ही दिखाता है. ये कोशिशें अब तक तो काफी सफल भी रही हैं.
दोनों में अंतर बस इतना है कि पहले वाला उदाहरण उस जमाने का है जब विकसित दुनिया को हमारे देश पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण हासिल था, जबकि आज हमारी अपनी सरकार बिना सोचे-विचारे तथा दासवृत्ति से, विकसित दुनिया की उन संस्थाओं के स्वार्थपूर्ण फरमानों को लागू करने में लगी हुई है, जो इसकी वकालत करती हैं कि राजकोषीय संकुचन के जरिए, आम जनता की आमदनियों को घटाया जाए और मुक्त व्यापार के लिए दरवाजे खोले जाएं ताकि उनकी कृषि-व्यापार कंपनियां, भारतीय उत्पादकों को सीधे अपने जाल में फांस सकें.
कृषि पर सार्वजनिक निवेश में कटौतियां
हमारी खेती की आय में भारी कमी करने वाले इन दीर्घावधि कदमों में, ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक खर्चों में कटौतियां भी शामिल हैं. याद रहे कि मौजूदा सरकार ने भी, ‘राजकोषीय अनुशासन’ के अंधमतवाद का अनुसरण करते हुए जो पहला कदम उठाया, ग्रामीण क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र पर खर्चो में भारी कटौतियां करने का ही था. सार्वजनिक खर्चों में कटौतियों का वैसा ही असर पड़ा है, जैसा असर पहले के जमाने में किसानों पर करों का भारी बोझ डाले जाने का हुआ था. विकसित देशों के नजरिए से यह जरूरी है कि आम जनता की क्रय शक्ति को घटाया जाए क्योंकि अगर आम जनता की क्रय शक्ति ‘ज्यादा तेजी से’ बढ़ रही होगी तो यह, हमारे जैसे विकासशील देशों में भोजन की स्थानीय जरूरतें पूरी करने के लिए ही जमीन को घेरे रखने को बढ़ावा देगा. इसका नतीजा यह होगा कि इन देशों की जमीनें ऐसी निर्यात फसलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगी, जिनकी विकसित देशों को बहुत भारी जरूरत है क्योंकि वे खुद इन फसलों को अव्वल तो पैदा ही नहीं कर सकते हैं और अगर पैदा कर भी सकते हैं, तो अपनी लंबी सर्दियों में तो किसी भी तरह से पैदा नहीं कर सकते हैं.
राजकोषीय संकुचन की ये नीतियां आम जनता की आमदनियां घटाने में इतनी ज्यादा कामयाब रही हैं कि जब 2011 से 2014 की त्रैवार्षिकी के दौरान जब खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी, जनता की क्रय शक्ति में कमी के चलते, इस बढ़े हुए खाद्यान्न को घरेलू स्तर पर खपाना ही संभव नहीं हुआ. इसके चलते ही 2013-14 तथा 2014-15 के दो वर्षों के दौरान, पूरे 4 करोड़ 70 लाख टन अनाज का निर्यात किया गया था. लेकिन, किसी भी अर्थशास्त्री ने और इसमें खुद को प्रगतिशील मानने वाले अर्थशास्त्री भी शामिल हैं, जनता के बढ़ते पैमाने पर भूखे रहने के बीच, इन बड़े पैमाने पर खाद्यान्न निर्यातों को, जनता के हाथों से क्रय शक्ति के छिनने के साथ जोडक़र देखने की कोशिश ही नहीं की. इसके बजाए उन्होंने खाद्य संकट की ऐसी सतही व्याख्याओं को ही फैलाने का काम किया, जो पश्चिमी विश्वविद्यालयों से निकली हैं और जिनमें विकसित दुनिया की गरीब आबादियों पर, आय संकुचन तथा निर्यात संवर्धन के प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह से अनदेखा ही कर दिया जाता है. अचरज ही बात नहीं है कि हमारे ग्रामीण उत्पादक, जो अपनी आजीविकाओं पर लंबे समय से जारी हमले झेल रहे हैं, सूखे की अतिरिक्त मार बर्दाश्त करने की स्थिति में ही नहीं रह गए हैं.
काश्तकारी पर चौतरफा मार
दो अन्य संबंधित नीति समूह और हैं, जिन्होंने काश्तकारों के लिए खेती के जोखिम को बहुत बढ़ा दिया है. इनमें से एक का संबंध, निर्यात की जाने वाली नकदी फसलों के मूल्य समर्थन के ही समाप्त किए जाने से है. दूसरे का संबंध मुक्त व्यापार के लिए कृषि का बाजार खोले जाने से है, जिसके चलते काश्तकारों को कीमतों में जो उतार-चढ़ाव झेलना पड़ता है, उसमें बहुत भारी बढ़ोतरी हो गयी है. पहले विभिन्न मालों के बोर्ड किसानों से मसाले, चाय, कहवा आदि की पैदावार, समर्थन मूल्य पर खरीदा करते थे. लेकिन, 1990 के दशक के मध्य में एक प्रशासनिक फरमान के जरिए इन बोर्डों से इन जिम्मेदारियों को छीन लिया गया और बहुराष्ट्रीय कृषि-व्यापार कंपनियों को खुली छूट दे दी गयी कि काश्तकारों को अपने कांट्रैक्ट के जाल में फांस लें.
काश्तकारों को विश्व बाजार में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के सामने अरक्षित छोडऩे के जिस तरह के नतीजे निकले हैं, उन्हें कपास उत्पादकों की बढ़ती ऋणग्रस्तता तथा आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या से आसानी से समझा जा सकता है. मोनसेंटो जैसी निर्मम कंपनियों ने अपनी जड़ें, हमारी खेती में गहराई तक फैला ली हैं. कपास उत्पादक किसानों की मुश्किलों का फायदा उठाकर उन्हें उच्च-प्रौद्योगिकी और ऋण का बंधुआ बनाकर रख दिया गया है. इस सब के बीच खुद को किसानों का ‘हितैषी’ बताने वाले कुछ लोग भी प्रौद्योगिकीय प्रगति के नाम पर, जैनेटिकली मॉडीफाइड कपास के लाए जाने पर तालियां बजा रहे हैं. ऐसे ‘हितैषियों’ की ऐसी बौद्धिक रूप से बचकानी दलीलों के बाद, काश्तकारों को दुश्मनों की जरूरत ही क्या रह जाएगी.
यह दिलचस्प है कि हाल ही में कुछ ऐसे प्रकटत: स्वार्थपूर्ण लेख आए हैं, जिनमें यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि किसानों की आत्महत्या के मामले को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर रखा जाता रहा है और वास्तव में गृहणियों के बीच आत्महत्या की दर कहीं ज्यादा है. इस तरह की बेतुकी दलीलें देने वाले, असली नुक्ते को अनदेखा ही कर देते हैं. सभी जानते हैं कि स्वीडन में आत्महत्याओं की रफ्तार कुख्यात रूप से ज्यादा है. लेकिन, क्या यह कोई कहता है कि इसके लिए स्वीडन की सरकार जिम्मेदार है. इसी प्रकार, भारत में एक पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रभुत्ववादी समाज में जी रही गृहणियों को बेशक, बहुत भारी दबाव झेलने पड़ते हैं. लेकिन, उनके बीच आत्महत्या की दर अपेक्षाकृत ज्यादा रहने के लिए सीधे-सीधे सरकार की नीतियों को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. इसके विपरीत, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि किसानों के बीच आत्महत्या की दर बढऩे में, सार्वजनिक नीतियों का सीधे-सीधे हाथ है. इसलिए, इस कारण से भी इन नीतियों का विरोध करना तथा उन्हें पलटे जाने की मांग करना उचित है.
साथ में दी गयी तालिका, 2013 में खेतिहर परिवारों की दशा पर, राष्ट्रीय नमूना सर्वे की रिपोर्ट से ली गयी है. इसमें दिए गए आंकड़ों में कृषि उत्पादित लागत सामग्रियों या उपभोग के लिए किन्हीं भी प्रक्षेपित मूल्यों को हिसाब में नहीं लिया गया है और ये आंकड़े आय की असमानताओं को वास्तव में कम कर के ही दिखाते हैं. इन आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि हालांकि संबंधित नमूने में भूमिहीन मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है, इस नमूने के आधे से ज्यादा परिवारों की खेती से जितनी आय थी, उससे ज्यादा आय मजदूरी से आ रही थी और वे वर्गीय लिहाज से गरीब किसानों की श्रेणी में आते हैं. 70 फीसद ग्रामीण परिवारों के लिए (जिसमें एक हैक्टेयर से कम जोत वाले सबसे गरीब तीन ग्रुप आते हैं), आय का स्तर दयनीय तरीके से नीचा था–5,500 रुपया से भी कम. आय का यह स्तर 540 रुपया या उससे भी कम निवेश की ही गुंजाइश देता था और वह भी ऋण के सहारे क्योंकि उनकी आय तो बुनियादी उपभोग की भरपाई के लिए भी काफी नहीं थी.
याद रहे कि 2012-13 का साल, खेती के लिहाज से एक अच्छा साल था. इससे साफ है कि काश्तकारों के विराट बहुमत के पास सूखे की मार से निपटने के लिए कोई आर्थिक गुंजाइश ही नहीं है. सबसे अमीर, दो श्रेणियों में आने वाले, सबसे ऊपर के 4 फीसद पास ही इतनी आय है कि खराब फसल के साल का सामना करने के लिए उनके हाथ में कुछ पैसा बच सकता है.
मनरेगा को लागू करने तथा उसका विस्तार करने की जरूरत स्वयंसिद्ध है और इसकी जरूरत सिर्फ सूखे के वर्ष में ही नहीं है. इसी तरह, खाद्य सुरक्षा कानून का गंभीर रूप से लागू किया जाना भी जरूरी है. 4 करोड़ टन अतिरिक्त अनाज, गरीब परिवारों की भूख मिटाने में लगाया जाना चाहिए था न कि उसका निर्यात किया जाना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण यह कि उन जहरीली नीतियों को उखाड़ फैंका जाना चाहिए जो जन-आमदनियों को घटाती हैं, किसानों के लिए मूल्य समर्थन व्यवस्था का सहारा खत्म करती हैं और देश के काश्तकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के सामने अरक्षित छोड़ देती हैं.
काश्त के आकार के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों के लिए हर खेतिहर परिवार पर सभी स्रोतों को मिलाकर औसत मासिक आय, उपभोग खर्च और उत्पादक परिसंपत्तियों में शुद्ध निवेश (रु0)
रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 फीसद
काश्त वार
श्रेणी (हैक्टेयर) मजदूरी से आय- खेती से आय- पशुपालन से आय- गैर-कृषि कार्यों से आय- कुल आय कुल उपभोग खर्च- उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश कुल खर्च कुल परिवारों का अंश
0.01 से कम- 2902- 30- 1181- 447- 4561- 5108- 55- 5163- 2.64-
0.01-0.4- 2386- 687- 621- 459- 4152- 5401- 251- 5652- 31.86-
0.41-1.0- 2011- 2145- 629- 462- 5247- 6020- 540- 6560- 34.92-
1.01-2.0- 1728- 4209- 818- 593- 7348- 6457- 422- 6879- 17.16-
2.01-4.0- 1657- 7359- 1161- 554- 10,730- 7786- 746- 8532- 9.31-
4.1-10.0- 2031- 15243- 1501- 861- 19,637- 10,104- 1975- 12,079- 3.72-
10.0 से ज्यादा- 1311- 35685- 2622- 1770- 41,388- 14,447- 6987- 21,434- 0.39-
औसत 2071- 3081- 763- 512- 6426- 6223- 513- 6736- —
स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 70वां चक्र, 2013. भारत में खेतिहर परिवारों के हालात के मुख्य संकेतक. स्टेटमेंट-12