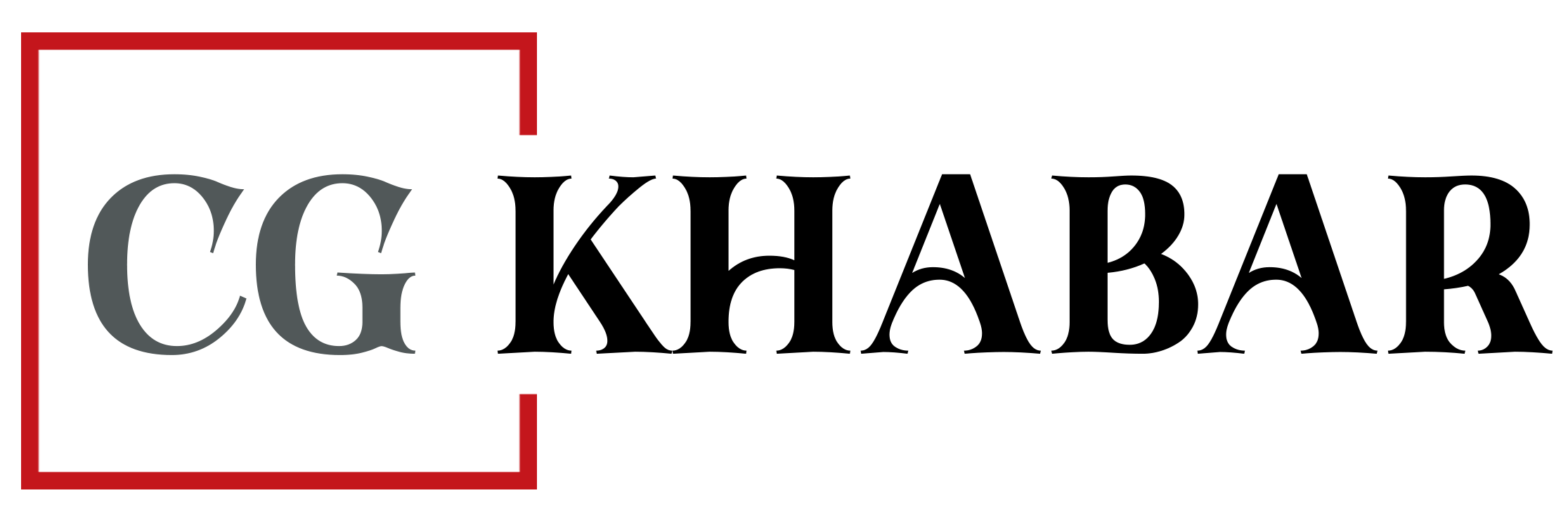ट्रंप के साथ भी, ट्रंप के बाद भी
ईश्वर सिंह दोस्त | फेसबुक
सवाल एक ट्रंप का नहीं है.
उसके पीछे लाखों श्वेत अमेरिकी खड़े हैं. सवाल श्वेत चौधराहट का भी नहीं है. उसके पीछे अमेरिका के शीर्ष कॉर्पोरेट पूँजीपतियों की ताकत खड़ी है. इसलिए अमेरिकी संसद भवन केपिटल पर हमले का खेल खत्म नहीं हुआ है.
यह अभी शुरू हुआ है. निश्चित ही अभी ट्रंप समर्थक एक कदम पीछे हो जाएंगे, ताकि भविष्य में लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए दो कदम बढ़ाने का मौका खुला रहे.
यह लंबे समय चलने वाली रस्साकशी होगी. लोकतंत्र के खेमे में जो अब हैं, उन्हें यह समझना होगा कि रस्सी के दूसरी तरफ सिर्फ ट्रंप का सनकीपन नहीं है, जिसे पिछले साल भर से अमेरिका के ही कुछ शीर्ष मनोवैज्ञानिक उनकी तेजी से गिरती हुई मानसिक स्थिति बता रहे हैं.
रस्सी के दूसरी तरफ सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, जो ट्रंप और उसके एजेंडे को सर आँखों पर बैठाए हुए थी. रस्सी के दूसरी तरफ सिर्फ पगलाई हुई श्वेत जनसंख्या नहीं है. जो पिछले चार सालों से नस्लीय नफरत और प्रतिहिंसा की आग में जल रही है. रस्सी के दूसरी तरफ सिर्फ अंधाधुंध मुनाफे के लालच में अंधे हो चुके चंद कॉर्पोरेट पूँजीपति नहीं हैं.
बल्कि देखना यह होगा कि रस्सी के दूसरी तरफ पूँजीवाद और लोकतंत्र की बढ़ती रार भी है. रस्सी के दूसरे तरफ महामंदी के भँवर में फँसी पूँजीवादी पद्धति भी है, जो नवउदारवादी भूमंडलीकरण के नाकाम होने के बाद से बौराई हुई है. रस्सी के दूसरी तरफ बढ़ती विषमता के बीच लोकतंत्र के असुरक्षित होने व अस्मिताओं की अफीम के सुलभ होने की दास्तान भी है.
ट्रंप तो मुफ्त में बदनाम है. हकीकत यह है कि ट्रंप के झूठ अकेले ट्रंप के झूठ नहीं हैं. वे अमेरिका की बहुसंख्यक श्वेत मानसिकता के झूठ भी हैं. वह झूठ सुनना चाहती है. वह झूठ दोहराना चाहती है. वह झूठ जीना चाहती है. वह कह रही है कि मैं जो कहूं वही कानून है और मैं जो करूं वही व्यवस्था है. तभी तो जो पुलिस कुछ महीनों पहले यहीं हुए फ्लायड लायड के समर्थन में हुई रैली के समय चाक-चौबंद थी, कैपिटल पर हुए हमले में अनमनी सी थी.
भीड़ के खत्म होने के बाद पुलिस नहीं है बल्कि भीड़ और पुलिस की विभाजक रेखा धुंधली हो गई है. अमेरिका की पुलिस इसके पहले भी चाहे लाख नस्लीय झुकाव वाली हो, मगर केपिटल के चौराहे पर उभरी यह नई पुलिस है, जिसके साथ बाइडन और हैरिस को अपना राज चलाना होगा.
यह सोचना भयंकर भूल होगी कि अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतिहास की काल गति से निरपेक्ष रहकर मजबूत बनी खड़ी रहेंगी. ये संस्थाएं जिस प्रतियोगी पूँजीवाद के दौर की उपज थी, वह अब नहीं है. ये संस्थाएं जिस पूँजीवादी उदारवाद के दौर की उपज थी, वह अब नवउदारवाद में तबदील हो चुका है.
उदारवादी लोकतंत्र की इबारतों की दुनिया भर में रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. दुनिया भर में देशों के संविधान कांप रहे हैं और डोल रहे हैं. बाइडन और हैरिस अमेरिकी संविधान को तब तक नहीं बचा पाएंगे, जब तक कि उनके पास लोकतंत्र से ऊब चले कार्पोरेट को खुश करने और साथ ही हावी न होने देने की रणनीति नहीं होगी.
यहां एक और लोकतंत्र भारत का ही उदाहरण लें. 2014 में मनमोहन सरकार ने जनता का विश्वास खोने से कहीं पहले भारत के कॉर्पोरेट जगत का विश्वास खो दिया था. वे मनरेगा, शिक्षा अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसे कदमों से बेचैन हो गए थे. उन्हें लगने लगा था कि देश के पैसे देश की जनता के लिए ही खर्च होंगे तो फिर हमारा क्या होगा. मनमोहन सरकार के एक हाथ में नवउदारवाद का फंडा और दूसरे में नव-नेहरूवाद का मिनी झंडा था. कॉर्पोरेट उद्विग्न था कि इसके दोनों हाथों में नवउदारवाद का फंडा क्यों नहीं है. बेचैन कॉर्पोरेट ने नफरत की राजनीति को समर्थन का दांव खेला.
यही अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों में हुआ था. अति दक्षिण यूं ही मजबूत नहीं हुआ है. यूं ही पिछले साल जर्मनी की संसद पर ऐसा ही हमला नहीं हो गया था.
दुनिया भर में तमाम देशों में जो पहचानें बहुसंख्या में हैं या आर्थिक व सामाजिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं, उनमें एक तरह का पीड़ितवाद पैदा कर दिया गया है. वे सोचने लगे हैं कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय उन्हें पीड़ित बनाए रखने के कायदे-कानून हैं. कॉर्पोरेट भी नए कानून चाहता है, नई व्यवस्था चाहता है. ये ताकतवर ‘पीड़ित’ भी नए कानून चाहते हैं, नई व्यवस्था चाहते हैं.
कॉर्पोरेट पूँजी का एजेंडा सिर्फ मेहनतकशों या किसानों के भविष्य को ही नहीं बल्कि छोटे पूँजीपतियों, मध्यवर्ग व व्यापारियों के भविष्य को भी नष्ट करता है, इसीलिए बिना नफरत के रसायन के उसके साथ भीड़ नहीं जुड़ती.
इसलिए जो बड़ा सवाल है वह यह है कि ताकतवरों के पीड़ितवाद से लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए.
सवाल यह है कि लोकतंत्र और नवउदारवाद की चूहा-बिल्ली जैसी दुश्मनी कैसे खत्म हो? अब या तो लोकतंत्र को झटका लगेगा या फिर नवउदारवाद को!
यह भी ख्याल रखना होगा कि कथित समाजवादी देशों का राजकीय पूँजीवादी मॉडल या सामाजिक पूँजीवादी मॉडल या फिर चीन जैसा अर्ध राजकीय- अर्ध नवउदारवादी मॉडल विकल्प नहीं है. लोकतंत्र में उसकी कोई रुचि नहीं है.
कथित समाजवादी देशों में औंधे मुँह पड़े मार्क्स को कोई सीधा करेगा या फिर कोई नई सोच आएगी? रास्ता कहाँ से मिलेगा? वाशिंगटन के कैपिटल से नवउदारवादी नफरत व लोकतंत्र की टक्कर की लाइव रिपोर्ट के बीच में ही यह सब भी सोचना समझना होगा.
#विमर्शवाचन 1: नवउदारवाद और लोकतंत्र