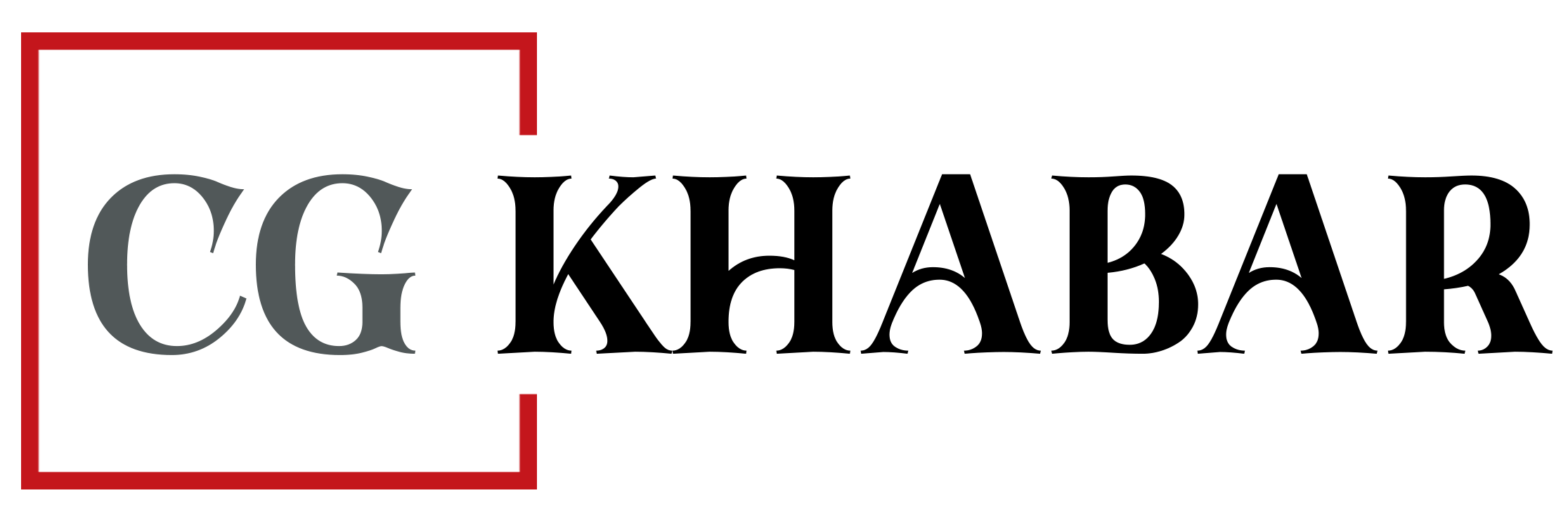बिक रहे हैं जंगल
सरकार भारत के जंगल की परवाह कम करती है और इन पर आधारित उद्योगों की ज्यादा. भारत सरकार सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों को कॉरपोरेट जगत के हवाले नहीं करना चाहती. सरकार चाहती है कि जंगल के तौर पर वर्गीकृत क्षेत्रों को भी उन्हें दे दिया जाए क्योंकि वे पर्याप्त ‘उत्पादक’ नहीं हैं. लाल किला जैसे ऐतिहासिक धरोहरों को कॉरपोरेट जगत को देने पर सोशल मीडिया में काफी चर्चा हुई लेकिन भारत के जंगलों को निजी कारोबारी घरानों को देने पर कहीं चर्चा नहीं दिख रही.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय वन नीति, 2018 के मसौदे पर दिए गए एक सुझावों और आपत्तियों पर पर विचार कर रहा है. इसे मार्च में जारी किया गया था. नई नीति 30 साल पुरानी नीति की जगह लेगी. जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हुए बदलावों को देखते हुए नई नीति प्रासंगिक लगती है. जंगल कार्बन उत्सर्जन को काबू में रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. वे कार्बन सोखते हैं. मसौदे में जलवायु परिवर्तन पर चिंता तो जताई गई है लेकिन इसके असली लक्ष्यों से पर्यावरणविदों और सिविल सोसाइटी समूहों को चिंता हो रही है.
1988 की वन नीति ने 1952 की नीति की जगह ली थी. पुरानी नीति में जंगलों को साम्राज्यवादी सोच यानी आर्थिक संसाधन के तौर पर देखा जा रहा था. लेकिन 1988 की नीति में जंगलों के पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित किया गया. यह माना गया कि जंगल का मतलब सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं है बल्कि यह जैव विविधता, मृदा और जल संसाधनों का पोषक भी है. इसमें यह भी माना गया कि जंगल की जमीन को दूसरे कामों में इस्तेमाल पर निगरानी होनी चाहिए और खास परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति देनी चाहिए. इस नीति के क्रियान्वयन में कई समस्याएं रहीं लेकिन फिर भी इसने पहले की सोच को बदला. इसका असर यह हुआ कि नीतियों के निर्माण में यह माना गया कि जंगल पर वहां रहने वाले लोगों का भी अधिकार है और वन संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. 2006 के वन अधिकार कानून ने इन अधिकारों को पक्का कर दिया. इसका असर ओडिशा के नियामगिरी में तब दिखा जब स्थानीय लोगों ने अपने जंगल में बॉक्साइट खनन के खिलाफ अपना निर्णय दिया.
2018 की नीति का मसौदा वैसे तो ठीक दिखता है लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर इसकी खामियां स्पष्ट होती हैं. इसमें प्राकृतिक जंगलों के योगदान का बखान तो है लेकिन फिर इसमें जंगल को आर्थिक संसाधन में सीमित कर दिया गया है. इसमें जलवायु स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला की बात की गई है और जंगलों की कम उत्पादकता पर चिंता जताई गई है. इसके समाधान के लिए इसमें कहा गया है कि जिन जंगलों में पेड़ों का कवर 40 फीसदी से कम हो, वहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल अपनाया जाए. पहले के ऐसे अनुभव बताते हैं कि इन प्रयोगों का नतीजा यह होता है कि तेजी से बढ़ने वाले औद्योगिक पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है और वहां के प्राकृतिक पेड़ धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं. ये स्थानीय लोगों को भी भगा देते हैं जबकि उनका वन पर अधिकार है. इस प्रयोग को यह कहकर सही ठहराया जा रहा है कि टिंबर लकड़ी की देश में कमी है और उसका आयात करना पड़ रहा है.
इसके अलावा प्रस्तावित नीति उन समस्याओं का समाधान भी नहीं कर रही जिससे जंगलों का नुकसान हो रहा है. जंगल विकास और अन्य परियोजनाओं की बलि चढ़ रहे हैं. पर्यावरण के मामलों पर वकालत करने वाले दो वकील रित्विक दत्ता अैर राहुल चैधरी ने सूचना का अधिकार के तहत 2013 में जो जानकारियां मांगी थीं, उनसे पता चलता है कि 135 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र हर रोज बांध, खदान और सड़क निर्माण जैसी विकास परियोजनाओं की वजह से नष्ट हो रहे हैं. जब नई नीति के मसौदे पर बहस चल रही है, उस वक्त भी संवेदनशील पश्चिमी घाट के कर्नाटक में 30,000 पेड़ काटने की योजना घोषित की गई है ताकि चिकमंगलुरु को दक्षिण कन्नड से जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर की सड़क बनाई जा सके. कोयला खनन के लिए जंगल सौंपे को लेकर चल रहा विवाद अब तक नहीं सुलझा.
इस तरह के कामों से जंगल बंट जाते हैं. इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता. अगर जंगल लगातार एक साथ हैं तो नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन होने पर उनके संरक्षण की उम्मीद होती है. लेकिन जब ये छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं तो उन पर कब्जा जमाना आसान हो जाता है. हमने यह खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में देखा है.
1988 की नीति में जंगलों को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने को लेकर सतर्कता दिखती है. लेकिन नई नीति के मसौदे में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है. अगर इसे मान लिया जाता है तो देश के प्राकृतिक जंगलों का 40 फीसदी हिस्सा निजी क्षेत्र के टिंबर कारखाने में तब्दील हो जाएगा. इससे न तो पर्यावरण का भला होगा और न ही इन जंगलों पर आश्रित 30 करोड़ लोगों का. लेकिन एक ऐसी सरकार के लिए यह बेहद उपयुक्त लगता है जो हर प्राकृतिक संसाधन से अधिक से अधिक राजस्व निकालना चाहती है चाहे वह जमीन हो, जंगल हो या पानी हो.
1966 से प्रकाशित इकॉनोमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली के नये अंक का संपादकीय