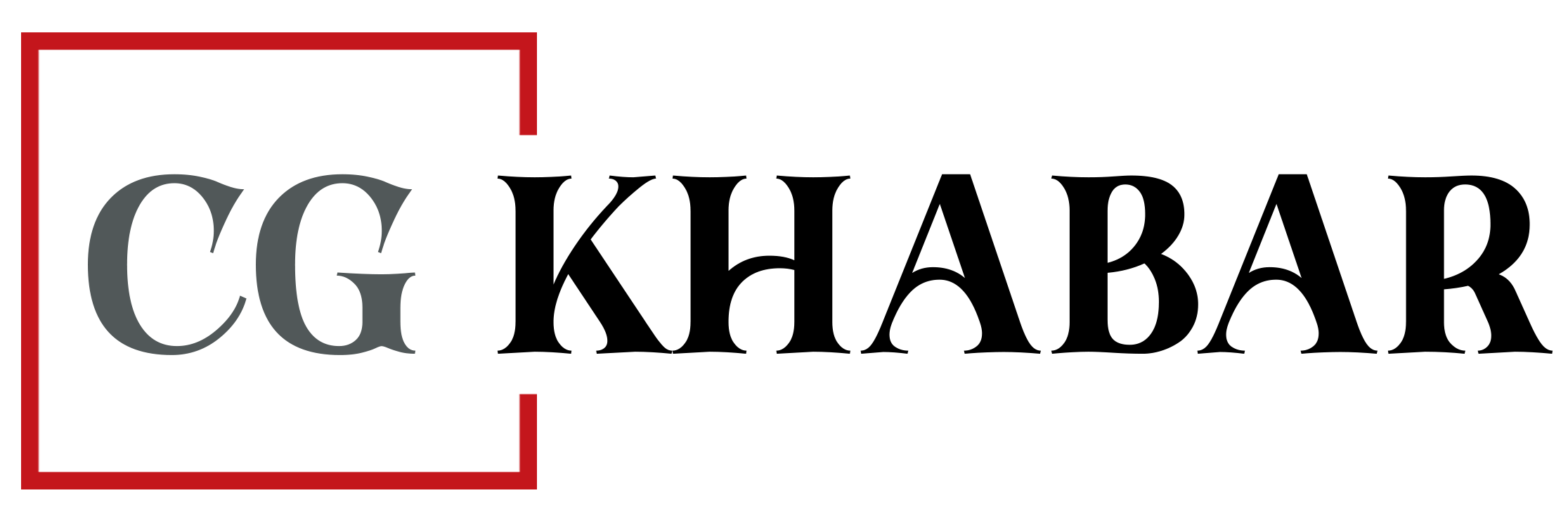वे कहीं गए हैं, बस आते ही होंगे
नयी शुक्रवारी के बारे में और ज्यादा कुछ याद नहीं. इतना जरुर है कि जाफरीनुमा कक्ष में बैठकें हुआ करती थी, चाय-पानी का दौर चलता था. बैठकों में शामिल होने वाले पिताजी के मित्रों में मुझे शैलेंद्र कुमार जी का स्मरण है. नागपुर नवभारत के संपादक. एक कारोबारी भी थे मोटेजी. विचारों से कामरेड. उनके यहाँ हमारा आना-जाना काफी था. उनकी पत्नी वत्सला बाई मोटे माँ की अच्छी सहेली थी. मुझे याद नहीं, स्वामी कृष्णानंद सोख्ता उस घर में आया करते थे. साप्ताहिक ‘नया खून’ के संपादक. विशाल व्यक्तित्व और दबंग आवाज. भैया बताते हैं – नयी शुक्रवारी की उस मकान में हमारे यहाँ आने वालों में प्रमुख थे सर्वश्री स्वामी कृष्णानंद सोख्ता, जीवनलाल वर्मा विद्रोही, प्रमोद वर्मा, शरद कोठारी, लज्जाशंकर हरदेनिया, के. के. श्रीवास्तव, श्रीकांत वर्मा, रामकृष्ण श्रीवास्तव, अनिल कुमार, मुस्तजर, भीष्म आर्य और नरेश मेहता.
स्वामी कृष्णानंद सोख्ता के बारे में याद हैं वे हमारे गणेशपेठ के मकान में अक्सर आया करते थे. जीवनलाल वर्मा व्रिदोही, प्रमोद वर्मा, रम्मू श्रीवास्तव, हरिशंकर परसाई, टी. आर. लूनावत, भाऊ समर्थ और प्रभात कुमार त्रिपाठी (जबलपुर) इन विद्वानों के चेहरे याद हैं. लेकिन कांतिकुमार जैन जिनके संस्मरण बहुचर्चित माने जाते हैं, घर कभी नहीं आए. न नागपुर के दोनों मकानों में आए न राजनांदगाँव में. बहरहाल घर में होने वाली साहित्यिक बहसों में और भी लोग शामिल रहते थे, पर अधिक कुछ स्मरण नहीं. सोख्ता जी का स्मरण इसलिए कुछ ज्यादा है क्योंकि वे आते ही हम लोग के साथ घुल मिल जाया करते थे. छोटे भाई दिलीप को कंधों पर बिठा लेते थे और इसी अवस्था में पिताजी के साथ चर्चा करते थे. चूंकि कच्ची उम्र दुनिया से बेखबर वाली होती है इसलिए साप्ताहिक ‘नया खून’ के बारे में हम विशेष कुछ जानते नहीं थे. यह उस समय का गंभीर वैचारिक साप्ताहिक पत्र था जिसकी महाराष्ट्र एवं महाराष्ट्र के बाहर, बुद्धिजीवियों की जमात में अच्छी पकड़ थी, प्रतिष्ठा थी.
गणेशपेठ निवास में दो घटनाएँ स्मृतियों में बेहतर तरीके से कैद है- पहली – मेरी छोटी बहन सरोज से जुड़ी हुई है. बहुत सुंदर थी, घुघराले बाल थे उसके. एक बार उसे बुखार आया. पता नहीं कितने दिन चला. लेकिन एक दिन माँ ने देखा वह बिस्तर पर नहीं थी. ढूंढा गया तो वह मकान से अलग-थलग, बाथरुम में फर्श पर दोनों घुटनों को मोड़कर, गठरीनुमा पड़ी हुई थी. शायद बुखार तेज था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सो वह शरीर को ठंडा करने गुसलखाने में पहुंच गई थी. वह नहीं रही. उसके न रहने का सदमा, कैसा और कितना गहरा था, मैं नहीं जानता था अलबत्ता माँ का रो-रोकर बुरा हाल था, और पिताजी गुमसुम से थे. अब सोचता हूं उन्होंने किस कदर अपने आपको संयमित रखा होगा, कैसे इस अपार दुख से उबरने की कोशिश की होगी.
दूसरा प्रसंग- प्रायमरी में पढ़ता था. कक्षा याद नहीं. एक दिन स्कूल से लौटा. माँ ने खाना खाने बुलाया. रसोई में मैं और माँ खाना खाने बैठे. खाते-खाते माँ ने मुझे दाल परोसने के लिए गंजी में बड़ा चम्मच डाला तो उसमें एक मरी हुई छिपकली आ गई जो फूलकर काफी मोटी हो गई थी. छिपकली को देखते ही माँ को मितली शुरु हो गई और भागकर गुसलखाने में चली गई और उल्टियां करने लगी. मुझे पर मरी छिपकली का कोई असर नहीं हुई. मैं मजे से कटोरी में परोसी हुई दाल खाता रहा जब तक माँ लौट न आई. मुझे उल्टियां नहीं हुई. कुछ भी विचित्र सा नहीं लगा. लेकिन तनिक स्वस्थ होने के बाद माँ हाथ पकड़कर उसी अवस्था में पैदल जुम्मा टैंक के निकट स्थित ‘नया खून’ के दफ्तर ले गई. पिताजी को बाहर बुलाया, बताया. और फिर मुझे मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया. शरीर से विष निकालने डाक्टरों ने क्या प्रयत्न किए नहीं मालूम. अलबत्ता मैं कुछ दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा. दिन-दुनिया से बेखबर.
माँ-पिताजी की चिंता से बेखबर. माँ को चूंकि उल्टियां हो गई थी इसलिए वे लगभग स्वस्थ थी. हालांकि वे भी अस्पताल में भर्ती थी. मेरी चिंता उन्हें खाए जा रही थी. उन्हें इस बात का अफसोस था अंगीठी पर रखी दाल की गंजी खुली क्यों छोड़ी. कैसे पता नहीं लगा कि छिपकली कब गिरी. कब से उबल रही थी. बहरहाल यह घटना दिमाग से कभी नहीं गई. छिपकली को देखता हूँ, तो वह दिन याद आ जाता है. अब उसे देख घिन आने लगती है लेकिन मारने की कभी कोशिश नहीं करता. छिपलियां तो घर की दीवारों पर चिपकी रहती ही हैं. इसलिए उन्हें भी जिंदगी के हिस्से के रुप में देखता हूँ क्योंकि वे यादें ताजा करती हैं. अच्छी-बुरी जैसी भी.
इसके पूर्व का एक और प्रसंग- मकान गणेशपेठ का ही. शुक्रवारी से कुछ बेहतर. पक्का खुला मकान. बड़ा सा ऑगन. ऊपर छत. पतंगें उड़ाने के लिए और कटी पतंग को पकड़ने के लिए लगभग पूरा दिन हम छत पर ही बिताते थे. पतंगबाजी में खूब मजा आता था. मैं और बड़े भैय्या रमेश. मेरा काम चक्री पकड़ने का रहता था, पतंगे वे उड़ाया करते थे, पैच लड़ाते, काटते-कटते. जब भी कोई कटी पतंग हमारे छत के ऊपर से गुजरती थी, हम धागा पकड़ने के फेर में रहते थे. मुझे याद है एक बार जब ऐसी ही कटी पतंग को पकड़ने की कोशिश की, कुछ बड़े लड़के अपशब्दों की बौछार करते हुए घर में लड़ाई करने आ गए. वे काफी उत्तेजित थे और मारने-पिटने पर उतारु थे. माँ ने किसी तरह समझाकर उन्हें बिदा किया. हमें जो डांट पड़ी, वह किस्सा तो अलग है. इस घटना ऐसा असर हुआ कि हम कुछ दिन तक छत पर ही नहीं गए. न मंजा पकड़ा और न ही पतंगे उड़ाई.
पिताजी आकाशवाणी में ही थे. नया मध्यप्रदेश बनने के बाद उनका भोपाल ट्रांसफर हो गया. इस ट्रांसफर को लेकर वे काफी पसोपेश में थे. क्या किया जाए. जाए या नहीं. इस बीच सोख्ताजी के चक्कर यथावत थे. वे घर आते थे और पिताजी की अवस्था देखते थे. अंतत: पिताजी ने भोपाल जाना तय किया. उनका बिस्तर बंध गया. एक छोटी पेटी के साथ रस्सी से बंधा उनका बिस्तर हाल में रख दिया गया. शायद दोपहर की कोई ट्रेन थी. हम सब हाल में इक_े थे. इस बीच सोख्ताजी आ गए. पता नहीं उनके बीच क्या बातचीत हुई. नतीजा यह निकला कि बिस्तर खोल दिया गया, पेटी अंदर चली गई और सामान फिर अपनी जगह पर रख दिया गया. पता चला पिताजी ने आकाशवाणी की नौकरी छोड़ दी और सोख्ताजी के अखबार में संपादक बन गए. लिखने-पढऩे के लिए उन्हें नया ठिकाना मिला. यह उनके मन के अनुकूल बात थी. अब यह कहने की जरुरत नहीं कि ‘नया खून’ को नई प्रतिष्ठा मिली और वैचारिक पत्रकारिता को नया आयाम. साहित्य के अलावा नया खून सहित समय-समय पर साप्ताहिक पत्रों के लिए उनके द्वारा किया गया लेखन उन्हें श्रेष्ठ पत्रकार के रुप में भी स्थापिता करता है.