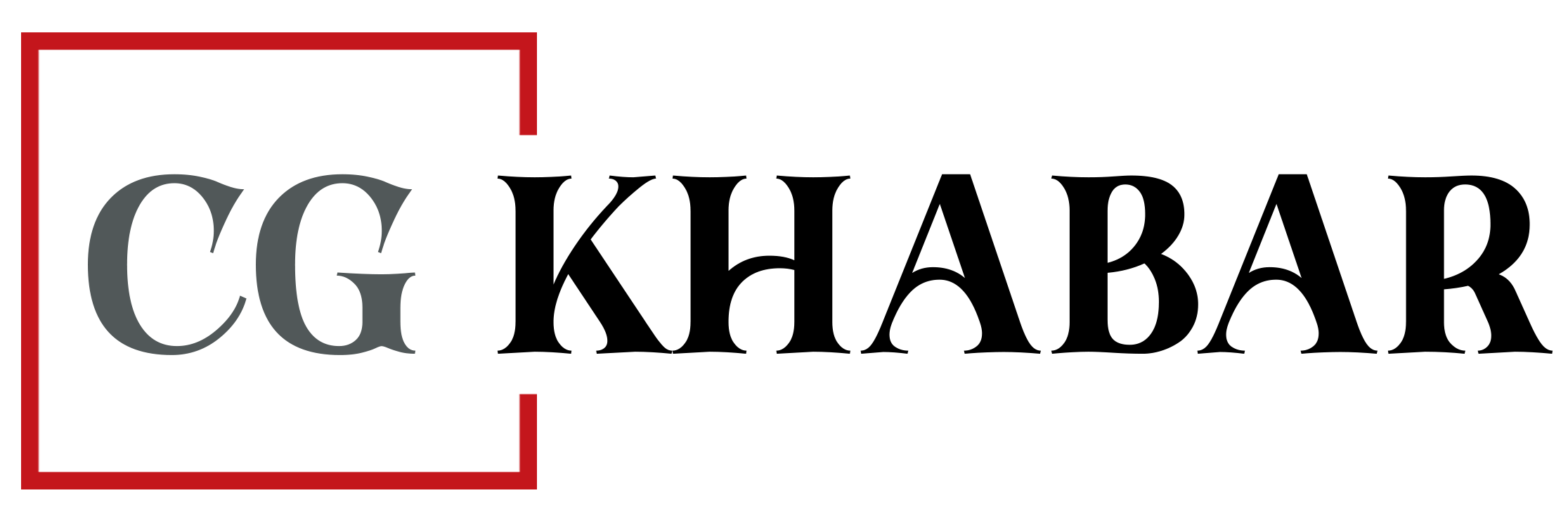पौष्टिक भोजन के बाद भी क्यों है कुपोषण ?
देविंदर शर्मा
कुपोषण सबसे अधिक कहां है? कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों के खान पान की विधियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि उनका खान पान पौष्टिक होता है पर वही क्षेत्र भयानक स्तर पर कुपोषण और अल्प पोषण से जूझ रहे हैं. जिस तरह का पौष्टिक भोजन इन क्षेत्रों में प्राप्य है और जिस प्रकार के दर्दनाक कुपोषण और भुखमरी से ये आदिवासी क्षेत्र ग्रसित हैं. ये विसंगति एक अजीब सी पहेली है और हमें इस बहुत बड़े विरोधाभास का उत्तर खोजना होगा.
पिछले सप्ताह मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके में स्थित बांसवाड़ा ज़िले के आनंदपुरी ब्लॉक के कुछ गावों का दौरा करने गया था. सबसे पहले मैं बांसवाड़ा से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोडिया तलाओ में 55 वर्षीय शंकर से मिलने गया. उसके पास 2.15 एकड़ भूमि है, तीन गाय, दो सांड और एक बकरी है. सभी जानवर देसी प्रजाति की हैं. गायें रोज़ाना मुश्किल से 500 ग्राम दूध देती हैं. जब उनसे पूछा कि फिर वो गाय क्यों रख रहे हैं तो वो बोले दूध के लिए नहीं खाद के लिए रखते हैं. वो मक्का, तुअर, धान, टमाटर, गेहूं, मिर्च और हल्दी की खेती करते है और बोले कि मैं नमक और चीनी के अलावा सब कुछ घर में ही उगाता हूँ.
फिर मैं उम्मीद पुरा गाँव के 35 वर्ष के चेतन पारगी से मिला. वो 4 बीघा ज़मीन पर खेती करने के साथ रस्सी की बुनाई का काम भी करते हैं. उन्होंने कहा कि वो ठीक ठाक कमा लेते हैं और उनकी ज़मीन से साल भर परिवार पालने योग्य उपज हो जाती है. उनकी सेहत देखकर इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था परन्तु वो अपनी बात पर अड़े रहे. वास्तव में तो अपने अल्प समय के दौरे में मैं जितने लोगों से मिला वो सभी अस्वस्थ दिख रहे थे. पर कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था और सभी कह रहे थे की उनकी ज़मीन से उन्हें साल भर पेट भरने योग्य उपज प्राप्त हो जाती है. पर क्या उनका ‘काफी’ वाकई में काफी होता है ? यही यक्ष प्रश्न है.
कुछ वर्ष पूर्व, 2014 में, मैं ओडिशा के रायगढ़ जनजातीय ज़िले में गया था. ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और महाराष्ट्र से एक दर्जन जनजातियाँ अपने अपने खानपान का प्रदर्शन करने एक आदिवासी फ़ूड फेस्टिवल में आये थे. इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य खेती के प्राचीन तरीकों से जुड़े पारम्परिक खानपान, जो प्रकृति की देन की संरक्षा करते हुए उन्हें सुनिश्चित पोषण देता था, उस संस्कृति को बढ़ावा देना था. मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों के 300 गाँवों से कोंध, कोया, दिधाई, संथाल, जुआंगा, बैगा, भील, पहाड़ी कोरवा, पौड़ी भुइयां और भिरहोर जनजाति के लोग अपने खान पान का प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें 5 किलो गेहूं, चावल या बाजरा उपलब्ध कराने की कवायद से खेती के पारम्परिक तरीकों को बचे रखने के उपायों पर चर्चा करने आये थे.
जब दक्षिण ओडिशा की जनजाति की लक्ष्मी पीडिकका ने मुझे रायगढ़ ज़िले के मुंडा गाँव में हाल ही में आयोजित आदिवासी फ़ूड फेस्टिवल में प्रदर्शित 1582 खाद्य प्रजातियों का महत्व और आवश्यकता के बारे में समझाया तो मैं न केवल हमारे आसपास मौजूद खाद्य पदार्थों की समृद्ध वैविध्यता से प्रभावित हुआ बल्कि मुझे ये भी पता चला कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता के बारे में मैं कितना कम जानता हूँ. 1582 खाद्य प्रजातियों, जिनमे कुछ जनजातियों के रोज़मर्रा के खानपान में शामिल विविध प्रकार की मछलियां, केंकड़े और पक्षी शामिल हैं, में से 372 उगाये नहीं जाते. जी हाँ, उगाये नहीं जाते.

काटलीपादार गाँव की मिनाती तूईका ने मुझसे कहा, ”हमें आपकी खाद्य सुरक्षा प्रणाली नहीं चाहिए. आप हमारे गाँवों में जितनी ज्यादा राशन की दुकानें खोलेंगे उतना ही आप हमे मजबूर कर देंगे कि हम अपने पूर्वजों द्वारा जी तोड़ मेहनत से बनाये गए सदियों पुराने खाद्य सुरक्षा उपायों को छोड़ दें. कृपा करके हमें हमारे हाल पर छोड़ दें.” पर जिसे अधिकतर नीति निर्धारक और नियोजक विकास समझते हैं उस बात से वो इतनी नाराज़ क्यों थी? क्या अधिकांश आभिजात्य वर्ग ये नहीं सोचता है कि जनजातियां अपढ़ और असभ्य हैं, अतः उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिए?
हमें मत सिखाइए कि विकास क्या है. हमने सदियों से अपने पौधों, अपनी मिटटी, अपने जंगलों और अपनी नदियों को संरक्षित रखा है. अब आप इन सब को हम से छुड़ा कर इन्हे नष्ट कर देना चाहते हो. इसे आप विकास कहते हो. ये कहकर उसने अपना चेहरा छिपा लिया. जब मैंने उससे मुझे ये समझाने का अनुरोध किया कि आदिवासी किस तरह प्रकृति के साथ तादात्म्य बना कर रहते हैं, कैसे आधुनिक शिक्षा उन्हें उनके पारम्परिक तौर तरीकों और संसाधनों पर समुदाय के नियंत्रण से दूर कर रही है तो पहले वो मुझे कुछ पौधे दिखाने के लिए तैयार हुई जिनके कई उपयोग होते हैं और किस प्रकार जनजातीय समुदाय पारम्परिक तरीकों से उन्हें संरक्षित करता है, उनका उपयोग करता है पर उन्हें विलुप्त होने नहीं होने देता.
उसने मुझे सियाली की फली दिखाई. ये काफी बड़ी फली होती है जिसके बीजों को उबालकर या सेंक कर खाया जाता है, इसकी टहनिओं से रस्सी बनायीं जाती है और पत्तों से पत्तल. कुसुम कोली के पत्तों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फल कच्चे खाये जाते हैं, लकड़ी ईंधन का काम करती है और बीज से तेल निकला जाता है. इस बीज का तेल मच्छर रोधी होता है तथा चमड़ी के रोगों के इलाज में भी काम आता है. लोक मानस में जिस महुआ को प्रसिद्धि मिली हुई है उसके भी एकाधिक उपयोग हैं. पत्तों का चारा बनता है, फूलों से गुड़, शराब और दलिया बनता है. फूलों को यूँ भी खाया जाता है और ये बाजार में बिकते भी हैं. फलों से सब्ज़ी भी बनती है और ये चारे का भी काम देते हैं, बीज से तेल निकलता है. दुर्भाग्यवश इन सब को कृषि की भाषा में जंगली पौधे माना गया है इसलिए इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है.
लिविंग फार्म्स के देबजीत सारंगी, जिसने आदिवासी फेस्टिवल का आयोजन किया, ने कहा कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य आदिवासी समाज के मिलजुल कर रहने की परंपरा तथा उनके साझा ज्ञान की प्रणाली को मज़बूती प्रदान करना है. इस आयोजन के माध्यम से खाना उगाने के वहनीय तरीकों और उनकी इकोलॉजी यथा भूमि, पौधे, जानवर और जंगलों के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डाला जाएगा. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कार्य बीते समय का भावनात्मक दोहन मात्र नहीं है तो उन्होंने रुखाई से कहा, ”हमारी गलती यही है. ये लोग प्रकृति के साथ पूर्ण तादात्म्य में हैं. इन्हे असभ्य कहकर नकारने की जगह हमें इनसे सीखना है. हमें अच्छा लगे या न लगे, मनुष्य जाति का भविष्य जनजातीय संस्कृति में ही छिपा है.”
अतः जिस विरोधाभास की मैंने शुरुआत में ही बात की थी वही अब सामने है. ऐसा क्यों कि इतनी समृद्ध खाद्य परम्परा के रहते भी जनजातीय क्षेत्र भयावह कुपोषण से जूझ रहे हैं? इसका सीधा सा उत्तर है. हमे जनजातीय क्षेत्रों में पारम्परिक तौर तरीकों पर आधारित बहु स्तरीय विकेन्द्रीकृत खाद्य सुरक्षा प्रणाली की संरक्षा करने की ज़रुरत है. जनजातीय आबादी को मासिक आधार पर पांच किलो गेहूं/चावल/बाजरा उपलब्ध करने के स्थान पर हमें मौजूदा खाद्य प्रणाली को सुदृढ़ करने पर बल देना चाहिए.
ऐसा तभी संभव होगा जब हम अपने पारम्परिक तरीकों पर नाज़ करने की भावना को प्रोत्साहित करेंगे. हमारी खाद्य परंपरा प्राकृतिक संसाधनों को रखने से जुड़ी है और यहीं से हमें शुरुआत करनी है. पता नहीं हमारे कृषि विश्वविद्यालय इस बारे में क्यों बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों हमारे फ़ूड मैगज़ीन और फ़ूड शो कभी भी पारम्परिक भोजन नहीं दिखातें हैं, और मुझे बिलकुल भी आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग को जनजातीय संस्कृति का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं. एक ऐसे आर्थिक मॉडल को तैयार करने की महती आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत जनजातीय लोगों को पारम्परिक खाद्य प्रणाली को बचाये रखने के लिए पुरस्कृत किया जाये. आखिरकार जनजातीय फ़ूड कल्चर को बचाये रखने के लिए ये एक छोटी सी कीमत समाज को देनी होगी क्योंकि संभव है कि यही मनुष्य जाति का भविष्य बचाने की कुंजी साबित हो.
* लेखक देश के शीर्ष कृषि और खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं.