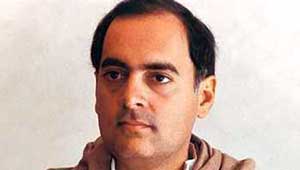उच्चतम न्यायालय से परे
सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वह ‘प्याली में तूफान’ और ‘आपसी पारिवारिक विवाद’ से कहीं अधिक है. 12 जनवरी, 2018 को शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा की गई प्रेस वार्ता से यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी संस्था सुधार और सवालों से परे नहीं है. न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरीयन जोसफ द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को नवंबर, 2017 में लिखा गया पत्र यह बताता है कि इन लोगों के बीच किस तरह की असहमति है. इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं. मीडिया को सिर्फ जज बीएच लोया की अचानक 2014 के दिसंबर में हुई मौत का मामला दिखा.
हालांकि, कुछ लोगों ने चार वरिष्ठ जजों के प्रेस वार्ता करने के निर्णय पर सवाल उठाया है. लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत के सबसे बड़े अदालत के कामकाज में सुधार की जरूरत है. इन चार जजों द्वारा लिखी गई चिट्ठी में अगर तनिक भी सच्चाई है तो फिर यह चिंता का विषय है. इसमें उठाया गया सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मसलों को एक खास पीठ के पास भेजा जा रहा है ताकि खास तरह का निर्णय आ सके. इन जजों का कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट का एक संस्था के तौर पर काफी नुकसान हुआ है और अभी और नुकसान होगा.
अभी यह देखना बाकी है कि मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम चार जजों के बीच का अविश्वास कैसे दूर होता है. लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम से इस संस्था पर लोगों का विश्वास कम हुआ है. जस्टिस चेलमेश्वर ने प्रेस वार्ता में कहा कि उच्चतम न्यायालय और अन्य संस्थाओं की विश्वसनीय बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अनिवार्य है.
विधायिका के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है. समय के साथ कानून बनाने के लिए जरूरी बहस करने की संसद की भूमिका सिमटती जा रही है. हालिया शीतकालीन सत्र 15 दिनों से भी कम का था. महत्वपूर्ण कानूनों पर काफी कम बहस हुई. यह चीज बेहद आम हो गई है. अगर संसद में कानूनों पर चर्चा नहीं होती है तो फिर जनता के पैसे पर चुने गए प्रतिनिधियों और इस पैसे से चल रहे इस संस्था का क्या मतलब रह जाता है.
संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है. इसके बावजूद मौजूदा कार्यपालिका ने विधायिका को बाईपास करके काम करने का तरीका निकाल लिया है. महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों को राज्यसभा की बहस से बचाने के लिए मनी बिल के तौर पर पारित कराया जा रहा है. यह कहना कि पिछली सरकार भी यही काम करती थी, कहीं से भी इस रुख को सही नहीं ठहराता. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए उच्चतम न्यायालय के आदेश और कानून में इस आशय का प्रावधान होने के बावजूद सरकार ने आम लोगों पर आधार थोपने की कोशिश की और संसद और उच्चतम न्यायालय यह तमाशा देखते रहे.
एक संस्थान के तौर पर प्रेस ने भी राजनीतिक विमर्श को गड़बड़ करने का काम किया है. हर मामले का पक्ष या विपक्ष में समेट दिया जा रहा है. संवाद और बीच के रास्ते की कोई जगह नहीं बची. मीडिया ने खुद को इन मामलों का अंतिम मध्यस्थ घोषित कर दिया है. मीडिया से यह उम्मीद की जाती है कि वह ताकतवर लोगों की जिम्मेदारी तय करे. लेकिन ऐसा कभी-कभार ही होता है.
चुनाव आयोग ने एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी. लेकिन हाल के कुछ निर्णयों से इसकी साख भी घटती जा रही है. आयोग गुजरात विधानसभा चुनावों को टालने के लिए तैयार हो गई थी. इससे सत्ताधरी पार्टी को वस्तु एवं सेवा कर में जरूरी बदलाव करके कारोबारी समाज का गुस्सा कम करने और इसे अपने साथ लाने में मदद मिली.
भारत में लोकतंत्र को बचाए रखने का खतरा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता में कमी तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य संस्थाओं की विश्वसनीयता में गिरावट तब बेहद व्यापक है.
1966 से प्रकाशित इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल विकली के नये अंक का संपादकीय