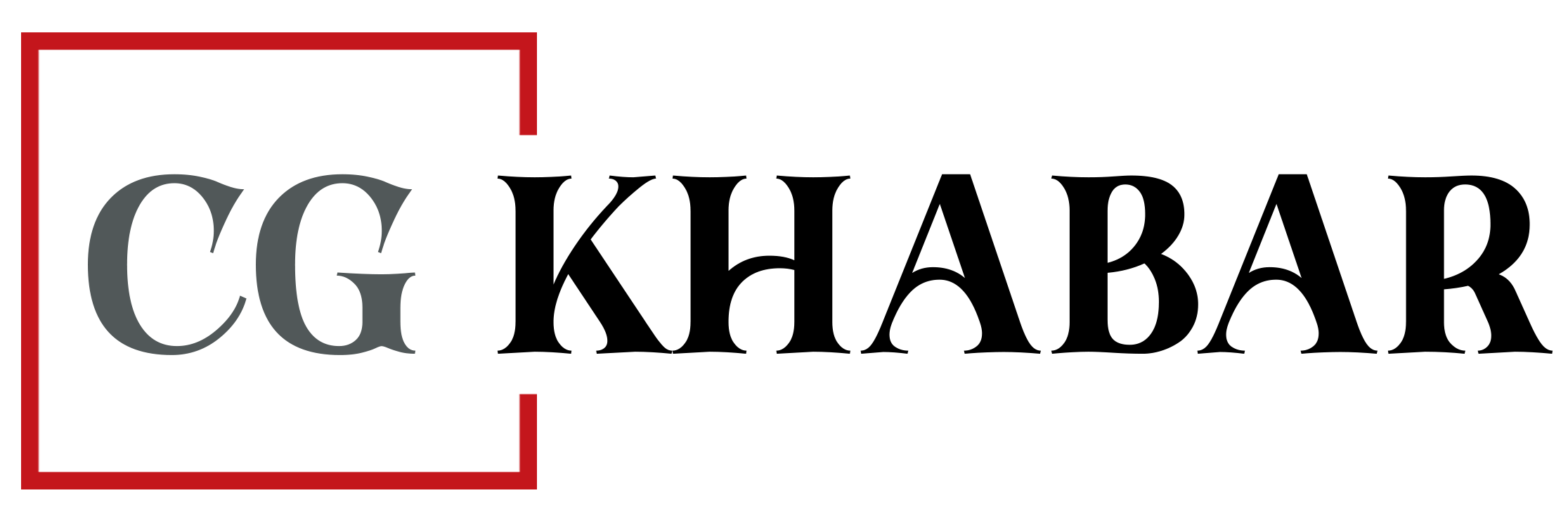‘लौहपुरुष’ को लगा जंग
ऩई दिल्ली | बीबीसी: कभी-कभी सोचता हूँ कि लालकृष्ण आडवाणी जी आजकल क्या सोचते होंगे? वह अतीत और यह वर्तमान! क्या किया और क्या पाया? और अगर यात्रा के अंत में यहीं पहुँचना था कि हार्डलाइन हिंदुत्व के लौहपुरुष को ज़ंग लगा कबाड़ बना कर फेंक दिया जाए, तो देश की छाती चीर देनेवाली विषबुझी भगवा हुँकारों और उन्मत्त कोलाहलों वाली उन रथ यात्राओं का महारथी बनना व्यर्थ ही नहीं चला गया क्या?
एक वह जन्मदिन था दीनदयाल उपाध्याय का, आज से 25 साल पहले का. जब 1990 में 25 सितंबर के दिन सोमनाथ मंदिर से लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी ‘राम रथ यात्रा’ शुरू की थी और समूची बीजेपी, समूचे संघ परिवार के लिए आडवाणी हिंदुत्व के उद्धारक प्राणवाहक भगवा भगवान के रूप में अवतरित हुए थे. और एक इस 25 सितंबर का दिन था, जब बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष के समारोहों का श्रीगणेश किया, तो आडवाणी को इस लायक़ भी नहीं समझा गया कि उन्हें समारोह में कम से कम बुला ही लिया जाए.
तो जब आडवाणी बुलाने लायक़ भी नहीं समझे गए तो बीजेपी में आज भला किसकी हिम्मत कि उनकी रथयात्रा के 25 साल पूरे होने को कोई याद भी कर ले.
संघ में निष्ठुरता की परंपरा
बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं कि संघ इस मामले में कितनी निष्ठुरता से अपनी परंपरा का निर्वाह करता है कि तंबू से किसी का अँगूठा भी बाहर निकलता दिखे, तो उसे ही बाहर फेंक दो, चाहे वह कोई हो!
आडवाणी न होते तो बीजेपी आज जाने कहाँ होती, कैसी होती और देश की राजनीति में उसकी कोई जगह होती भी या नहीं, कौन कह सकता है?
लेकिन यह कहा जा सकता है कि आडवाणी न होते तो बीजेपी और आरएसएस को शायद वह दिशा भी नहीं मिली होती, जिसने बीजेपी और संघ दोनों को आज इस मुक़ाम पर पहुँचा दिया है कि आज बीजेपी समूचे भारत पर भगवा फहराने, और संघ अगले पच्चीस-तीस वर्षों में वैदिक राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का सपना देख पा रहे हैं.
और आडवाणी की वह रथयात्राएँ न होतीं, तो संघ परिवार के उग्र हिंदुत्व को न नेतृत्व मिला होता, न भाषा मिली होती और न अपील.
गांधीवादी समाजवाद
याद कीजिए, समाजवादियों से पटी पड़ी जनता पार्टी से बाहर निकल कर जनसंघ घटक ने 1980 में जब बीजेपी का चोला ओढ़ा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने ‘गाँधीवादी समाजवाद’ की माला जप कर सबको चौंका दिया था.
कारण यह कि समाजवाद उन दिनों ‘लेटेस्ट फ़ैशन’ था. इंदिरा गाँधी ‘ग़रीबी हटाओ’ और समाजवाद के नारे पर देश और काँग्रेस दोनों पर पकड़ बनाए रखने का सफल प्रयोग इसके पहले कर चुकी थीं. और जनता पार्टी के बिखराव के बाद सत्ता फिर से इंदिरा गाँधी के पास पहुँच गई थी. इसलिए बीजेपी ने इंदिरा के समाजवाद के मुक़ाबले ‘गाँधीवादी समाजवाद’ को उतारने की चाल चली. लेकिन जनता पर बीजेपी के ‘समाजवाद का छद्म’ बिलकुल चला नहीं.
आडवाणी का करिश्मा
यह ठीक है कि आज यह कह सकते हैं कि इंदिरा की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर की वजह से ही 1984 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ़ दो सीटें जीत सकी थी, लेकिन सच यह है कि ऐसी कोई घटना न भी होती तो भी बीजेपी कोई चमत्कारिक प्रदर्शन कर पाने की स्थिति में नहीं थी.
यह आडवाणी थे, जिन्होंने 1984 की हार के बाद जब बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, तो बीजेपी को समाजवाद के गड्ढे से निकाल कर हार्डलाइन हिंदुत्व की तरफ़ मोड़ा.
1985 में इधर शाहबानो का मामला हुआ, जिससे हिंदू सामान्य तौर पर उत्तेजित थे, उधर 1986 में फ़ैज़ाबाद की एक अदालत ने ‘राम जन्मभूमि’ का ताला खोलने का आदेश दे दिया.
संघ परिवार की तरफ़ से गाँव-गाँव रामशिला पूजन शुरू हुआ और आडवाणी ने बीजेपी को पूरी तरह इस आंदोलन में झोंक दिया. फिर 1990 की रथयात्रा और 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक की यात्रा का वह दौर था, जब संघ में आडवाणी की तूती बोल रही थी, उनकी मर्ज़ी के बिना संघ में कोई फ़ैसले नहीं होते थे.
वाजपेयी थे मुखौटा!
वाजपेयी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने कि संघ उन्हें बनाना चाहता था. वह इसलिए प्रधानमंत्री बने कि आडवाणी के नाम पर बहुत-से सहयोगी दल समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे.
वाजपेयी चाहे जितने बड़े नेता रहे हों, संघ ने मजबूरी में बस उन्हें बर्दाश्त किया और हमेशा आडवाणी के ज़रिए उन पर लगाम लगाए रखी.
बीच-बीच में नियोजित तौर पर वाजपेयी के ‘रिटायरमेंट’ तक की चर्चाएँ हवा में उछाली जाती रहीं और आख़िर थक-हार कर वाजपेयी को कहना पड़ा, ‘न टायर्ड, न रिटायर्ड, अब आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय प्रस्थान!’
आडवाणी की ग़लती
वाजपेयी जैसे क़द्दावर नेता की उपयोगिता संघ में क्या थी, इसकी पोल गोविंदाचार्य उन्हें ‘मुखौटा’ कह कर खोल ही चुके थे. लेकिन शायद आडवाणी ने गोविंदाचार्य की बात पर ध्यान नहीं दिया और यहीं ग़लती कर बैठे.
उन्हें लगा कि गठबंधन की राजनीति के कारण ‘हार्डलाइनर’ बने रह कर उनका प्रधानमंत्री बन पाना मुश्किल है, तो उन्होंने वाजपेयी बनने की कोशिश की. उत्साह में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए और जिन्ना को सेकुलर बता देना उन्हें महँगा पड़ गया. वहीं से संघ में उनका इंडेक्स गिरने की शुरुआत हुई.
आडवाणी को उसके बाद से हिंदुत्व की बात करते सुना भी नहीं गया. वह राजनीति में अपनी जगह तलाशने का संघर्ष करते रहे.
वह इस स्थिति में कभी आ नहीं पाए कि बीजेपी को अपने नेतृत्व से सत्ता दिला पाते, नरेंद्र मोदी के राज्याभिषेक का विफल विरोध कर वह संघ के कोपभाजन और बन गए.
संघ के लिए अब उनकी कोई उपयोगिता बची ही नहीं, न मुख की और न मुखौटे की. फिर वह आडवाणी को चिपकाये-चिपकाये क्यों घूमे?
और संघ की लिस्ट में आडवाणी न पहले हैं, न आख़िरी. किसी ज़माने में जनसंघ का मतलब था बलराज मधोक. संघ के बिदकते ही वह निठल्ले हो गये. संघ के लिए राजनेता कारतूस हैं, दाग़ दीजिए. फिर ख़ाली खोखे का क्या काम?
(क़मर वहीद नक़वी, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम से)