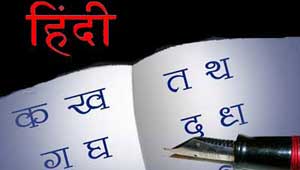अपनी भाषा पर आत्ममुग्ध लोग….
सुनील कुमार
पिछले दिनों भोपाल में विश्व हिन्दी सम्मेलन भी हुआ जिसमें हिन्दी पर हावी हिन्दू को लेकर बहस छिड़ी. कहीं कुछ लोग हिन्दी की दशा और दिशा पर बात कर रहे हैं, तो कहीं यह चर्चा कर रहे हैं कि सरकार से लेकर बाजार तक हिन्दी के साथ किस कदर का भेदभाव है. एक-दो हफ्ते पहले मैंने भी इसी कॉलम में शुद्ध हिन्दी के लिए लोगों की शुद्धतावादी जिद के नुकसान लिखे थे, लेकिन हिन्दी को लेकर कुछ और पहलुओं पर लिखा जाना जरूरी है.
आज एक सवाल आम लोगों के मन में यह उठता है कि अगर वे किसी तरह खींचतान कर अपने बच्चों को किसी सतही ही सही, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो क्या इसके बावजूद उन्हें अपने बच्चों को हिन्दी स्कूल में भेजना चाहिए? या फिर हिन्दी महज मजबूरी की जुबान है? स्कूल में बच्चे हिन्दी पढ़ भी लें, तो उसके बाद उनका कॉलेज का भविष्य क्या है? कॉलेज के आगे की और ऊंची पढ़ाई में उनकी संभावना क्या रहेगी, और दुनिया के कारोबार में उनकी क्या गुंजाइश रहेगी?
दरअसल कोई भी भाषा भावनाओं से अगर संपन्न हो सकती होती, तो हिन्दी एक खासी रईस जुबान होती. इसने भावनाओं का इस कदर सम्मान किया कि कभी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया, तो कभी भारत की ही दूसरी भाषाओं के शब्दों के इस्तेमाल का हौसला पस्त करते हुए लोगों को संस्कृत की तरफ ठेलने की अंतहीन कोशिश की. हिन्दी तो इससे पता नहीं कहां पहुंची, लेकिन महज हिन्दी पर टिके हुए लोग बड़े बाजार से बाहर हो गए. अपने आपको राष्ट्रभाषा का भक्त, या हिन्दी का सेवक कहने वाले लोग हिन्दी का उतना ही बुरा करते चले गए जितना बुरा एक आक्रामक हिन्दुत्व के त्रिशूलधारी लोग हिन्दू धर्म का कर चुके हैं.
हिन्दी को लेकर एक धर्मान्ध कट्टरता जैसी सोच ने इस जुबान का भारी नुकसान किया है. मेरे एक पुराने अखबारनवीस साथी विनोद वर्मा ने कल ही अमर-उजाला के इंटरनेट संस्करण के संपादक की कुर्सी से हिन्दी की दशा में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने हिन्दी बोलने वालों की आबादी, और इंटरनेट पर उस अनुपात में ज्ञान और जानकारी के हिन्दी पेज के आंकड़े गिनाए हैं. किस तरह दुनिया के अलग-अलग जुबान बोलने वाले लोगों की गिनती और उनकी जुबान में मौजूद ज्ञान और तकनीकी सूचना के पैमाने पर हिन्दी और हिन्दी वालों का बुरा हाल है, यह बात उन्होंने लिखी है.
यह नौबत आई इसलिए है कि हिन्दी के झंडाबरदार लोगों ने इस भाषा में काम करने के बजाय इसकी सेवा करने को अपना जिम्मा समझ लिया था. और जिस तरह सेवा में एक कट्टरता को काफी मान लिया जाता है, उसी तरह की कट्टरता हिन्दी जुबान को गड्ढे में डालने के लिए काफी साबित हुई. आज सरकार से लेकर कारोबार तक हिन्दुस्तान में हिन्दी एकदम ही गरीब जुबान बन चुकी है, गरीबों की जुबान बन चुकी है, छोटे खरीददार की जुबान बन चुकी है, और इसके महत्व को बढ़ाने के बजाय इसके नाम पर नेतागिरी करने वाले लोग इसे माता का दर्जा दिलाने में लगे रहे. नतीजा यह हुआ कि पिछले दस दिनों में दस ऐसे कार्टून मीडिया में आए जिसे हिन्दी को मां कहा गया, और यह भी कहा गया कि इस मां को औलाद वृद्धाश्रम में छोड़ आई है.
हिन्दी के साथ एक बड़ी दिक्कत आज यह है कि हिन्दुस्तान कोई टापू नहीं रह गया है जहां के हिन्दीभाषी राज्यों की संभावनाएं बाकी दुनिया से कटकर चल सकती हैं. बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दें, हिन्दुस्तान के ही बाकी गैरहिन्दी राज्यों से कटकर हिन्दी-राज्य नहीं चल सकते. बहुत से मामलों में हिन्दी के राज्य अहिन्दी राज्यों के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकते. कारोबार के मामले में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक का हाल हिन्दी राज्यों के मुकाबले आसमान पर है. महाराष्ट्र में और आन्ध्र में किसानों की आत्महत्या जरूर हो रही है, लेकिन उससे इन राज्यों के गैरकिसानी कारोबारों पर फर्क नहीं पड़ा है. आज इन राज्यों का कम्प्यूटरों से जुड़ा हुआ कारोबार आसमान पर है, और हिन्दी राज्य इस मामले में जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं. और इस फर्क की एक बड़ी वजह अंग्रेजी और हिन्दी का फर्क है. यही हाल कन्नड़ वाले कर्नाटक का है, यही हाल मलयालम वाले केरल का है, और यही हाल तमिल वाले तमिलनाडू का है. इन तमाम राज्यों में अपनी क्षेत्रीय भाषा में स्कूली शिक्षा को खूब मजबूत किया, लेकिन इन्होंने दुनिया की आज और आने वाले कल की जरूरतों को समझते हुए न सिर्फ अपीनई पीढ़ी को अंग्रेजी सिखाई, बल्कि तरह-तरह के हुनर भी सिखाए, और यही वजह है कि दुनिया भर के देशों में इन्हीं राज्यों के कामगार जाकर अधिक काम कर रहे हैं.
अमरीका में हाईवे के किनारे के मोटल अब उनके पटेल-मालिकों की वजह से पोटेल कहे जाते हैं. इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में गुजराती कारोबारियों ने छोटे से लेकर बड़े तक कई किस्म के कारोबार किए, और इनमें न हिन्दी उनके काम आई है, और न गुजराती. उनके काम एक कारोबारी-नजरिया आया, और अंग्रेजी की मामूली जानकारी आई. इसी तरह बिना मजबूत अंग्रेजी के, पंजाब से निकलकर लाखों लोग अंग्रेजों के घर ब्रिटेन में बसे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और अमरीका में बसे. वहां खूब मेहनत की, और कामयाब हुए. उन्होंने अंग्रेजी न जानने को दिक्कत नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत खूब की. अब भाषा का एक विकल्प कुछ लोगों ने मेहनत को बना लिया, कुछ लोगों ने एक कारोबारी-सूझबूझ को बना लिया, और कुछ लोगों ने हुनर को बना लिया, जैसा कि केरल से जाकर पूरी खाड़ी पर छा गए मलयाली कारीगर और कामगार हैं. इस तरह भाषा का इस्तेमाल कुछ हद तक है, और उस हद के बाद भाषा के बिना भी काम लोग निकाल लेते हैं. लेकिन भाषा के विकल्प के रूप में उनको कुछ न कुछ खूबी आना जरूरी होता है, और दक्षिण के राज्यों से लेकर गुजरात और पंजाब तक ने यह साबित किया है.
हिन्दी के साथ दिक्कत यह रही कि वह राष्ट्रभाषा होने के अपने आत्मसम्मोहन से परे ही नहीं निकल पाई. और भाषा होती दरअसल एक औजार है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों के बीच बातचीत के लिए होता है. अब इस बातचीत को कुछ लोग साहित्य तक खींचकर ले जाते हैं, जो कि भाषा के कई किस्म के इस्तेमाल में से है महज एक इस्तेमाल है. ऐसे में जिन लोगों के दिमाग पर साहित्य का अहंकार होता है, वैसे लोग उस भाषा को लेकर भी एक झूठे अहंकार में खुद भी फंसते हैं, और दूसरों को भी फांस लेते हैं. नतीजा यह होता है कि भाषा की राजनीति में, भाषा के अहंकार में, भाषा के दुराग्रह और पूर्वाग्रह में, साहित्य तो चौपट होता ही है, उस भाषा के गैरसाहित्यिक आम इस्तेमाल वाले लोग भी चौपट होते हैं. जब दुनिया के रोज के कामकाज में अपनी भाषा की संभावना बनाने के बजाय उस भाषा की आरती उतारते चले जाने को ही उस भाषा की बढ़ोत्तरी मान लिया जाता है, तो इस धर्मान्धता से वह भाषा पत्थर की एक प्रतिमा की तरह हो जाती है.
आज की दुनिया में कम्प्यूटरों के साथ तालमेल बिठाकर चलना सीखने के बजाय हिन्दी के लोग भाषा के अहंकार में जीते चले गए. जिस तरह आज भारत के इतिहास से परे की कहानियों को लेकर बहुत से लोग एक झूठे अहंकार में जीने को राष्ट्रगौरव मानकर चलते हैं कि किस तरह दुनिया में विज्ञान की तमाम चीजें बाकी देशों से हजारों बरस पहले भारत में बन चुकी थी, उसी तरह भाषा का अहंकार लोगों को मातृभाषा की सेवा, राष्ट्रभाषा का दर्जा, ऐसी बातों में उलझाकर रख देता है. आज दुनिया में इंटरनेट और कम्प्यूटर, टेक्नालॉजी और साईंस, इनकी भाषा की जरूरतों के हिसाब से हिन्दी ने न अपने को ढाला, न अपनी शब्दावली को दरियादिल बनाया, और न ही यह सोचा कि हिन्दी की देवनागरी लिपि की संभावनाओं के सीमित होने से उबरने का क्या रास्ता आज के वक्त निकाला जा सकता है.
हिन्दी में अपने आपको हिन्दीभाषी इलाकों की बोलियों से भी ऊपर उठाकर एक शास्त्रीय भाषा की तरह एक ऐसी खड़ी बोली बनाकर उसे क्षेत्रीय बोलियों पर लादने का काम किया, जिससे कि क्षेत्रीय बोलियों की अपनी मौलिक अनोखी बात कुचलती चली गई. ऐसा करके हिन्दी ने अपने आपको अधिक आबादी की जुबान तो साबित किया, लेकिन पिछले सौ-दो सौ बरस में ही जो खड़ी बोली प्रचलित हुई, उसने क्षेत्रीय बोलियों की खूबियों को भी इस हिकारत से देखा कि वे एक देहाती सी हों, और इस नाते सस्ती हों, सतही हों, और गैरजरूरी हों. ऐसे में हिन्दी की बुनियाद में जिन क्षेत्रीय भाषाओं के पत्थर लगे हैं, वे भी हिन्दी की खड़ी बोली से जुडऩे के बजाय या तो अपनी बोली के साथ रहे, या फिर उन्होंने भी अंग्रेजी के विकल्प को ढूंढने की कोशिश शायद की होगी.
अब आज हिन्दी एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है कि जहां वह अपने पीछे अपनी जुबान के लोगों को या तो एक अनिश्चित भविष्य की राह पर ले जा सकती है, और उस राह का कोई भविष्य दिखता नहीं है. दूसरा रास्ता यह है कि हिन्दी अपने आपको हिन्दीभाषी इलाकों में संपर्क की एक भाषा रखते हुए, पढ़ाई-लिखाई, खासकर ऊंची पढ़ाई-लिखाई की जुबान अंग्रेजी को अपरिहार्य मानकर उसको जगह दे, उसका इस्तेमाल करे, और अपनी अगली पीढ़ी को भाषान्धता का शिकार न बनाए. तीसरा विकल्प यह है कि देश और हिन्दीभाषी प्रदेशों की सरकारें हिन्दी में उच्च शिक्षा तक को इतना मजबूत बनाए कि लोग उच्च शिक्षा अपनी मातृभाषा में करें, और फिर अंग्रेजी या कोई और अंतरराष्ट्रीय जुबान सीखकर दुनिया के मुकाबले में उतर जाएं, जैसा कि आज चीन कर रहा है. लेकिन इसकी संभावना हमको शून्य दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य से अपना हाथ खींचना जारी रखा है, और उच्च शिक्षा में तो सरकारी हिस्सेदारी खत्म सी हो चली है. चौथा रास्ता टर्की की तरह का कोई क्रांतिकारी रास्ता हो सकता है, जहां पर कि दशकों पहले एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने अपने देश की भाषा वही रखते हुए उसकी लिपि अंग्रेजी रोमन लिपि कर दी थी, ताकि किसी दिन यह देश योरप का हिस्सा बनने का दावा कर सके. इस मिसाल को देने का मतलब हिन्दी की लिपि बदलने का सुझाव बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन किसी तरह की कोई क्रांतिकारी सोच शायद हिन्दी को एक बेहतर कामकाजी भाषा बना सके.
हिन्दी का हो-हल्ला अगर हिन्दुत्व के हो-हल्ले की तरह ही चलता रहेगा, तो इस भाषा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई भविष्य नहीं होगा, और इसमें अपना भविष्य ढूंढने वाले लोग, अपने बच्चों के लिए बहुत आश्वस्त न रहें. भाषा का आविष्कार लोगों के बीच संवाद के लिए एक औजार की तरह हुआ था. इस औजार को कुछ लोगों ने आत्ममुग्ध होने के लिए आईने की तरह बना लिया, और कुछ लोगों ने इसे दूसरी भाषाओं के खिलाफ एक हथियार की तरह बना लिया. यह नौबत किसी भी भाषा के लिए ठीक नहीं है.
* लेखक हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार और रायपुर से प्रकाशित शाम के अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक हैं.