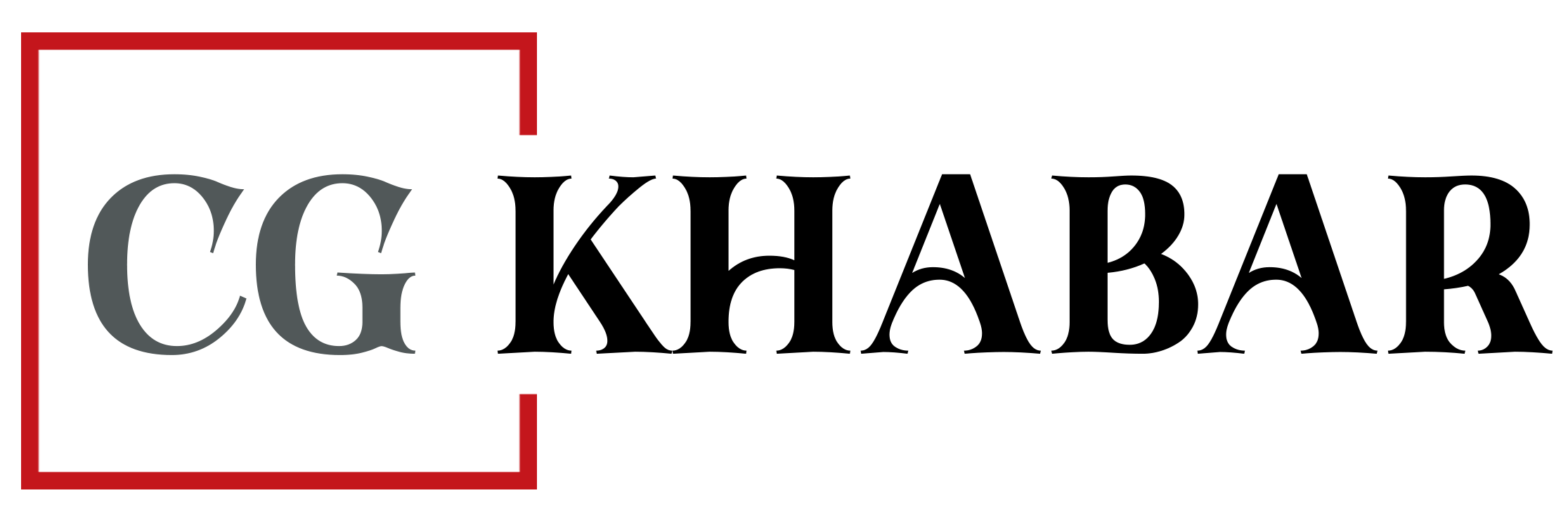1977 से आगे
सुनील
कुछ साल पहले की बात है. दिल्ली जाने पर मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक से मिलने गया था. चरचा के दौरान मैंने कहा कि पांचवें-छठे वेतन आयोग ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों और प्रोफेसरों के वेतन बहुत बढ़ाये हैं, जिससे समाज में गैरबराबरी और उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा मिला है. उन्होंने तुरंत उनका बचाव करते हुए कहा कि यह जरूरी है, नहीं तो विश्वविद्यालय में अच्छे लोग टिकेंगे ही नहीं. वे प्रगतिशील और समाजवादी रुझान के अर्थशास्त्री माने जाते हैं और वैश्वीकरण-बाजारीकरण की नीतियों के आलोचक हैं. इसलिए मेरे लिए यह थोड़ी हैरानी की बात थी.
दूसरी ओर दिवंगत समाजवादी चिंतक किशन पटनायक जैसे लोग और देश के किसान संगठन लगातार इन वेतन आयोगों की सिफारिशों का विरोध करते रहे हैं. महाराष्ट्र के किसान नेता और एक वक्त किसान संगठनों की अंतरराज्यीय समन्वय समिति के अध्यक्ष रहे विजय जावंधिया ने हाल ही में एक लेख में लिखा है कि इन वेतन आयोगों ने कर्मचारियों-अफसरों के वेतन जितने बढ़ाये हैं, उसी अनुपात में किसान की आमदनी बढ़ाना है, तो गेहूं का मूल्य 2,835 रुपये और कपास का 20,240 रुपये प्रति क्विंटल करना होगा. क्या देश इसे मंजूर करेगा?
दोनों तरफ के तर्को में दम है. दरअसल, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसको महत्व देती है. दूसरे शब्दों में कहें, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी लॉबी तगड़ी है और सत्ता में किसकी ज्यादा चलती है. हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद कई द्वंद्वों में से यह एक है. अमीर-गरीब, गांव-शहर, खेती-उद्योग, सवर्ण-दलित, स्त्री-पुरुष, विकसित-पिछड़े राज्य, पूंजीपति-मजदूर जैसे कई द्वंद्व हमारे वर्तमान समाज में मौजूद हैं.
एक दूसरा उदाहरण लें. विश्व व्यापार संगठन बनने के बाद मुक्त व्यापार की जय-जयकार के बीच भारत सरकार ‘निर्यात-आधारित विकास’ की नीति पर चलती रही है. लेकिन निर्यात बढ़ाने के लिए और दुनिया की गलाकाट अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए जरूरी है कि भारतीय कारखानों में पैदा होनेवाले माल की लागत कम रखी जाये. इसके लिए जरूरी है कि मजदूरी कम रहे, मजदूर आंदोलन को दबा कर रखा जाये और मजदूर-हितैषी नियम-कानूनों को शिथिल किया जाये. यह भी जरूरी है कि प्रदूषण रोकने पर जोर न दिया जाये, क्योंकि इससे कंपनियों की लागत बढ़ती है. तो आप मजदूर और पूंजीपति दोनों को खुश नहीं रख सकते. एक तरफ निर्यात बढ़ाने और राष्ट्रीय आय की वृद्घि दर बढ़ाने और दूसरी तरफ पर्यावरण या मजदूरों के हितों की रक्षा करने के काम एक साथ नहीं हो सकते. मानेसर, गुड़गांव में मारुति कंपनी के मजदूरों का जिस तरह से दमन हुआ, वह इस विकास नीति में अंतर्निहित है.
और देखें. पिछले दो दशकों से तकरीबन देश के हर राज्य और हर पार्टी की सरकारें प्रदेश के विकास के लिए कंपनियों को बुलाती रही हैं. वे बार-बार ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ आयोजित करती हैं. लेकिन इन कंपनियों के आने से जल-जंगल-जमीन को लेकर कई झगड़े खड़े हो गये हैं. दरअसल, तीव्र औद्योगीकरण के लिए खनिज, जमीन और पानी की बड़े पैमाने पर जरूरत होती है. लेकिन ये चीजें बहुतायत में जहां मिलती हैं, वहां इन्हीं संसाधनों पर आदिवासियों, किसानों, मछुआरों आदि की जिंदगी टिकी हुई है. इन संसाधनों के दोहन से आंदोलन खड़े हो जाते हैं. अब या तो औद्योगीकरण किया जाये या प्रकृति और प्रकृति से जुड़े समुदायों को बचाया जाये. जो सरकार दोनों करने का दावा करती है, वह एक तरह से झूठ बोलती है. आधुनिक विकास में इस तरह के द्वंद्व और अंतर्विरोध नीहित है. इनको हल करने का एक ही तरीका है कि एक नये तरह के वैकल्पिक विकास के बारे में सोचा जाये.
देश की मौजूदा पार्टियां अगर इस बारे में नहीं सोचती हैं, तो इसके दो कारण हैं. एक तो विकास का स्वरूप बदलने के लिए काफी बड़े बदलाव की जरूरत होगी, जिसका साहस इनमें नहीं है. दूसरा, इन पार्टियों के नेताओं के नीहित स्वार्थ मौजूदा विकास नीति में हैं. वे जिस तबके से आते हैं, उसका हित इसी में है.
हैरानी की बात यही है कि इस वक्त देश में वैकल्पिक राजनीति का दावा करनेवाली जो नयी पार्टी उभर कर आयी है, वह भी इन मुद्दों पर मौन है. उसने भ्रष्टाचार और पानी-बिजली का मुद्दा तो सफलतापूर्वक उठाया है. उसने राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता, सादगी और वादापूर्ति पर जोर दिया है तथा पूंजी-माफिया-राजनीति के गठजोड़ को तोड़ने का साहस दिखाया है. इसलिए राजनीति की चहुंमुखी गिरावट से त्रस्त भारतीय जनता का ध्यान उसने आकर्षित किया है. लेकिन मौजूदा व्यवस्था के कई बुनियादी सवालों और द्वंद्वों पर वह या तो चुप है या फिर अस्पष्ट है. खास तौर पर उसकी आर्थिक नीति और विकास नीति बिल्कुल भी साफ नहीं है.
दिल्ली और देश में फर्क है. यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सफलता को देश के स्तर पर दोहराना चाहती है, तो केवल भ्रष्टाचार की बात करने से काम नहीं चलेगा. देश की जनता के सामने बहुत सारे सवाल हैं. जैसे गरीबी कैसे दूर होगी? मौजूदा ‘रोजगारहीन’ विकास चलता रहा, तो बेरोजगारी दूर होगी या यह और बढ़ेगी? विस्थापन का सिलसिला कैसे रुकेगा? गांव कैसे बचेगा? पर्यावरण कैसे बचेगा? केवल जनलोकपाल बन जाने या ईमानदार लोग चुन कर आ जाने से ये सभी समस्याएं हल हो जायेंगी, ऐसा मानना नितांत भोलापन है और इतिहास के अनुभव के खिलाफ है.
व्यक्तिगत रूप से ईमानदार तो मनमोहन सिंह भी हैं, मोरारजी देसाई भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन उनकी गलत नीतियों, विकास की गलत सोच और आर्थिक-सामाजिक ढांचों को बदलने की अनिच्छा ने देश को मौजूदा हालत में पहुंचा दिया है. यदि इन अनुभवों से सबक नहीं लिया, तो कहीं इतिहास फिर अपने को दोहराने न लगे. 2014 में एक बार फिर 1977 जैसा माहौल बन रहा है. लेकिन यदि हम 1977 से आगे न बढ़े और हमने पुरानी कमियों को दुरुस्त नहीं किया, तो खतरा इस बात का है कि युवाओं की यह ऊर्जा और मेहनत बेकार चली जायेगी और देश एक बार फिर लंबी निराशा के गर्त में चला जायेगा.