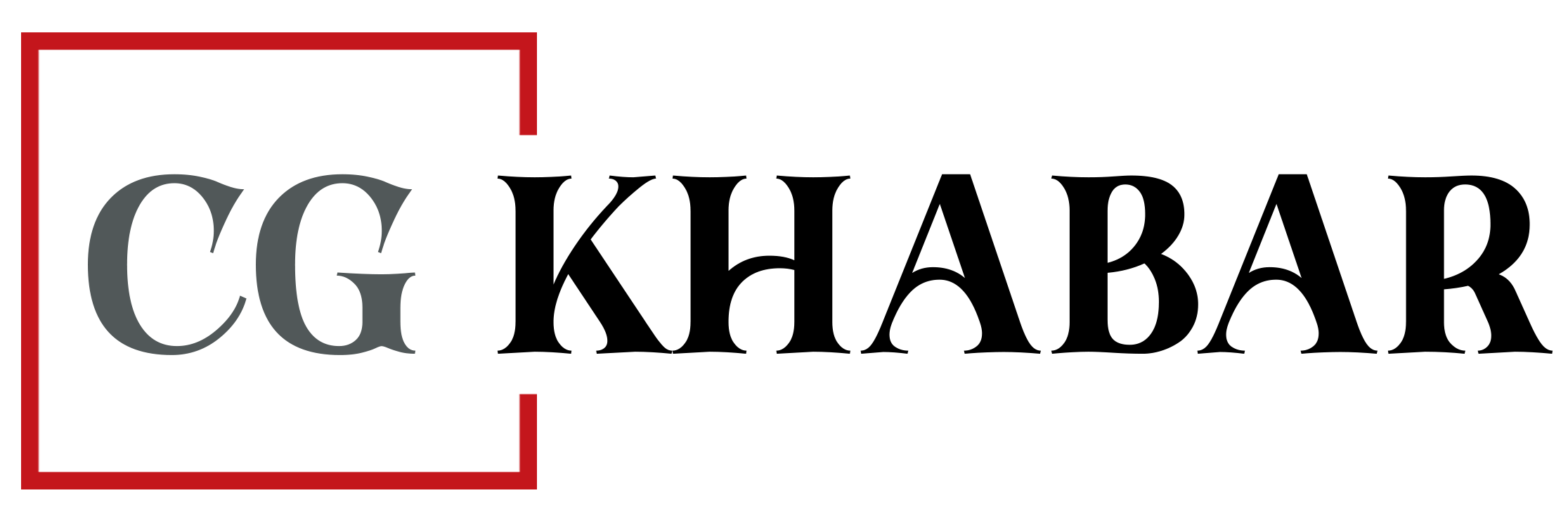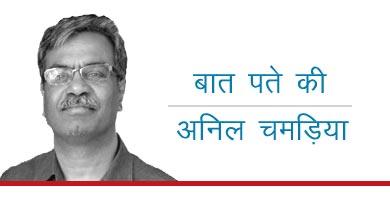अदालत क्यों बने सांस्कृतिक संघर्ष के केन्द्र
अनिल चमड़िया
अदालतों का चरित्र तेजी के साथ बदलता दिखाई दे रहा है. इसे कई तरह से महसूस किया जा रहा है. यहां उन पहलूओं की चर्चा की जा रही है जो अदालतों के भीतर पेशेवराना समूह के साथ घटित हो रही है. पचास वर्ष के एक वकील ने बताया कि भारतीय अदालतों में कान्वेंट यानी अभिजात्य वर्ग की संस्कृति को पुख्ता करने वाले स्कूलों से पढ़-लिखकर आने वाले लोग न्यायाधीश के पद पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं. स्कूल को बच्चों को तैयार करने का कारखाना कहा जाता है. बच्चों को जैसे ढालना चाहें, उस प्रयास का असर उन बच्चों पर रहता है. स्कूल और परिवार दोनों की जोड़ी बैठ जाए तो बच्चे को एक खास ढांचे में पुख्ता किया जा सकता है. कान्वेंट एक खास तरह की आर्थिक सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को तैयार करते हैं. उनकी भाषा अंग्रेजी होती है. वहां यदि किसी ने बिहारी, मद्रासी, गुजराती, पंजाबी लहजे में अंग्रेजी बोली तो उसका मजाक उड़ाया जाता है.
इस तरह कान्वेंट और सरकारी स्कूल की पृष्ठभूमि का एक टकराव अदालतों में दिख रहा है. जो वकील सरकारी स्कूलों यानी वैसे स्कूलों जो सार्वजनिक चिंताओं के बीच से निकला शिक्षण संस्थान है, से पढ़कर लिखकर आए हैं वे भाषा को एक माध्यम भर मानते हैं. वे उसे सांस्कृतिक वर्चस्व के औजार के रुप में इस्तेमाल करने के हुनर के साथ नहीं आए हैं. वकील बता रहे थे कि न्यायिक पदों पर नए तरह के लोग जो आ रहे हैं, वे वकीलों को अंग्रेजी भाषा नहीं आने पर झाड़ पिलाते हैं. अंग्रेजी को बेहतर करने के लिए दबाव बनाते हैं. उन्हें इस तरह जलील किया जाता है जैसे वे न्यायाधीश की तरह की अंग्रेजी न जानने का अपराध करके अदालत के कटघरे में खड़े हैं.
भारतीय अदालतें इस समय सांस्कृतिक आग्रहों के लिए चर्चा में आ रही है. पहले मी लॉर्ड कहने की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष की घटनाएं सुनने को मिलती थी. यह ब्रिटिश सत्ता विरोधी आंदोलन से निकली संस्कृति की पक्षघरता के लिए होता था. इस संघर्ष के आयाम अब बदल गए हैं. कौन किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, किस तरह अदालतों में आने वालों को व्यवहार करना चाहिए और किस तरह बातें करनी चाहिए.
मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत होने वाली मंजुला चेल्लुर ने बताया कि वे कैसे सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को पसंद करती हैं. उनका जोर हमेशा अदालतो में आने के लिए खास तरह के रंगों और खास तरह के कपड़े पहनने पर रहा है. वे अदालतों को मंदिर मानती हैं, लिहाजा वहां खास तरह के रंगों और पहनावे पर जोर देती हैं. वे भद्रलोक वाले कोलकाता में पली बढ़ी हैं और अपने उन्नतीस वर्ष के अनुभव के बारे में बताती हैं कि उन्होंने अपने साथ के कर्मचारियों को जिंस नहीं पहनकर आने के लिए कहा था. वे कहती हैं कि अदालतों में काम करने वालों की तो जरुर और यहां आने-जाने वालों के लिए भी पहनावे की एक मर्यादा होनी चाहिए. उनका यह पूरा सांस्कृतिक दृष्टिकोण 21 दिसंबर 2017 के द इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर छपा है.
सेवानिवृत न्यायाधीश के बयान को एक तो अपवाद नहीं माना जा सकता है. यह अदालतों में चलने वाले सांस्कृतिक संघर्षों के सतह पर आने वाले कुछेक उदाहरणों में एक जरुर हैं. भारतीय अदालतों के सांस्कृतिक संघर्ष बेहद सपाट नहीं हैं. बल्कि उन्हें एक तरफ का अभिजात्य व ब्राहम्णवादी संस्कृति के बीच के संघर्षो के रुप में देखा जा सकता है तो दूसरी तरफ अभिजात्य-ब्राहम्णवादी संस्कृति और विविधता के संघर्षों के रुप में देखा जा सकता है. कई सतहें दिखती है.
न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर के बयान के अनुसार उनके सांस्कृतिक निर्माण में जो अंतर्विरोध दिखता है उसका विश्लेषण किया जा सकता है. एक भारतीय ढांचे की सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति और दूसरा पश्चिमी असर के साथ घुला मिला अभिजात्यपन एक खास तरह के भारतीय को निर्मित करता है. पहले धोती कुर्ते पर टाई पहनकर भारतीय तैयार हुए थे. यह मंदिर की पवित्रता पर विशेष जोर देता है लेकिन इसके लिए ड्रेस कोड की अनिवार्यता बताता है. भारतीय समाज में हमने ये महसूस किया है कि भारतीय विविधता को नाकारने के ब्राहम्णवादी संस्कृति के अपने लिए कुछ रुप हैं तो अभिजात्य वर्ग के लिए अपने कुछ रुप है. एक के नकार का जोर सामाजिक स्तर के रुपों पर होता है तो दूसरा का स्तर भाषाई और देखने सुनने के स्तर पर होता है. ये एक जगह पहुंचकर एक जैसे दिखने लगते हैं. विविधता को अपने अनुकूल तैयार करने की संस्कृति वास्तव में वर्चस्ववादी संस्कृति होती है. स्वभाविक विविधता की स्वीकार्यता की संस्कृति ही वास्तविक लोकतांत्रिक विचारधारा होती है.
इन संघर्षों का एक उदाहरण सबसे बड़ी अदालत में भी देखने को मिला. सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश के बारे में ये खबरें प्रकाशित हुई कि उन्होंने अदालत में उंची आवाज में बात नहीं करने की चेतवानी दी है. उन्होंने ये चेतावनी उन वकीलों को दी, जो कि अपने मुकदमों को अपनी चिंताओं की ताकत से लड़ते हैं. दो तरह के वकील होते हैं. एक जो किसी मुकदमें को मुकदमें की तरह लड़ते हैं. यानी उनमें एक साथ एक ही मामले में पक्ष और विपक्ष का वकील बनने का हूनर होता है. दूसरे वकील वे होते हैं जो कि अदालत को समाज के भीतर विभिन्न स्तर पर चल रहे संघर्षों, समाज की अपेक्षाओं, समाज में उनकी तकलीफें जो कि कही-सुनी जा रही है, उन्हें अदालतों के सामने लाने वाले होते हैं.
दूसरे तरह के वकीलों की भाषा में अदालती मर्यादा होती है लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि स्वर की मात्रा भी मर्यादा के दायरे में आती है. चिंता, उपेक्षा से उपजी निराशा, गुस्से की भाषा स्वर में ही घुली मिली होती है. गांव घरों में उंचे पदों पर विराजमान लोग अक्सर उन्हें उंची आवाज में बात करने से बाज आने की चेतावनी देते हैं जो कि उनके पदों को सांस्कृतिक रुप से आहत करती है. पिता बेटे से कहते हैं तो सास बहु से कहती है. सामाजिक रुप से बड़ी कहलाने वाली जाति के लोग नीची कहलाने वाली जाति के लोगों से कहते हैं. मालिक नौकर से कहता है कि उंची आवाज में बात नहीं करें. कभी बेटा पिता से, बहू सास से, नौकर मालिक से नहीं कहता है कि उंची आवाज में यानी तेज वाल्युम में बात नहीं करें. मतलब स्पष्ट है कि ऊची आवाज में बात नहीं करने की चेतावनी देना केवल ऊंचे पदों का सांस्कृतिक औजार है.
भारतीय अदालतें संविधान के तहत बनी हैं, जहां समाज में विभिन्न स्तरों पर समानता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित है. अदालत की अवधारणा में ऊंचा-नीचा नहीं है. वह एक ढांचा है, जिनमें समानता है. वकील जज बन सकता है और जज अपनी नौकरी छोड़कर वकालत कर सकता है. न्याय की तलाश करने वाला एक ढांचे के सदस्य हैं. यदि वहां ऊंची आवाज में बात नहीं करने की चेतावनी आती है तो इसका अर्थ है अदालतें बदल रही हैं. वहां के सांस्कृतिक संघर्ष उल्टी तरफ मुड़ रहे हैं.