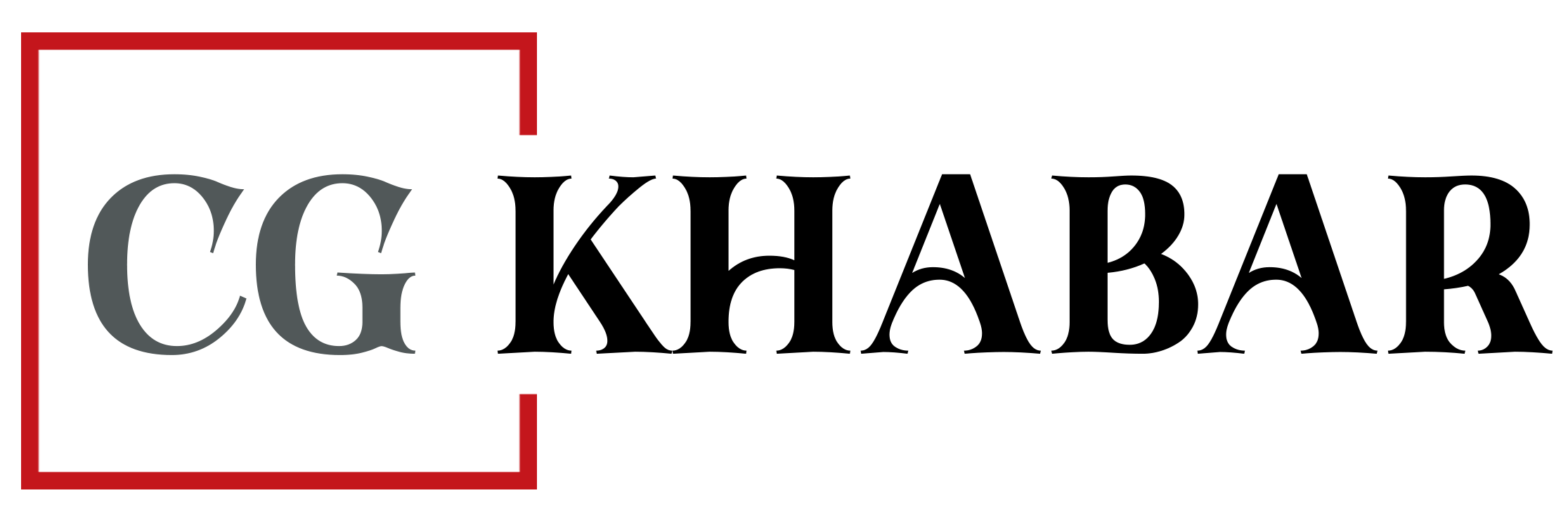न्यायपालिका बनाम विधायिका
देश के राजनीतिज्ञ जब-तब चिंतित होते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं. आज एक बड़ा राजनीतिक तबका बहुत चिंतित है. सरकारें बदल जाती है, चिंता वही रहती है. लेकिन जब राजतंत्र और लोकतंत्र में एक ही बात को लेकर दो धुरी बन जाएं तो विषय गंभीर लगने लगते हैं. बस कुछ ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में विधायिका और न्यायपालिका में जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा?
इन सबके बीच यह क्यों भुला दिया जाता है कि अदालतों के वो आदेश, जो सरकारों के फैसलों में रोड़े बनते हैं, जनहित याचिका के जरिए ही अदालतों के संज्ञान में लाए जाते हैं.
जनहित के मायने क्या हैं, सबको पता है. हां, कई बार दृश्य, श्रव्य, विश्वनीय मुद्रित माध्यमों या फिर एक अकेली चिट्ठी पर भी अदालतें जनहित का स्वत: संज्ञान ले, सरकारों की तंद्रा भंग कर, उनके कामकाज को कटघरे में खड़ा कर देती हैं.
स्वाभाविक है कि किसी भी सरकार को यह भला क्यों लगेगा? बस यही स्थिति जब-तब बनती रहती है. लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि अब टकराव हुआ कि तब, क्योंकि अब तक जितने भी ऐसे अदालती आदेश हुए हैं, सरकारों को नसीहतें मिली हैं और फैसलों को व्यापक जनसमर्थन मिला है.
इसका सीधा मतलब यह हुआ कि उसी लोकतंत्र ने न्यायतंत्र को सदैव सर्वोपरि माना है जिसने विधायिका को पर्याप्त हैसियत दी है. यही भारतीय न्याय प्रणाली की सर्वोपरिता है, सर्वस्वीकारिता है और न्यायालयों के प्रति अगाध विश्वसनीयता है.
इस सबके बावजूद भारत में न्यायापलिका और विधायिका में टकराव की चिंता नई नहीं है. पहले भी दर्जनों बार ऐसी स्थिति बनी और खुद-ब-खुद खत्म भी हुई.
बड़ा सवाल यह कि ऐसी स्थिति बनती क्यों है? इस विषय में कभी चिंतन हुआ या संसद में हमारे लोकतंत्र के भगवानों ने खुले मन से विचार विमर्श किया? या फिर महज औपचारिकता या झुंझलाहट से ज्यादा कुछ नहीं?
अगर बिना किसी पूर्वाग्रह के अब तक के सभी घटनाक्रमों पर ध्यान दिया जाए तो कभी यह सिद्धांत की लड़ाई लगती है तो कभी अहं की और राजनीति के चश्मे से देखें तो यह बहुमत के हुंकार की लड़ाई भी लगने लगती है. इन सबके बीच बड़ा सवाल यही कि कौन बड़ा, न्यायपालिका या विधायिका? उत्तर क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है.
12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर छह वर्षो तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. लेकिन इंदिरा गांधी ने मानने से ही इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करवा दिया. यह टकराव काफी चर्चित रहा.
मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया था. लेकिन चार साल बाद राज नारायण ने उच्च न्यायालय में चुनाव परिणाम को चुनौती दी. उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने, गलत तरीकों का इस्तेमाल किया. अदालत ने आरोपों को सही ठहराया लेकिन इंदिरा गांधी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा.
भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच खींचतान को लेकर वर्ष 2007 में भी एक जबरदस्त प्रसंग सामने आया जब भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश वाई.के. सब्बरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत जाने वाले कानूनों की समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है भले ही वह कानून 9वीं अनुसूची का हिस्सा क्यों न हो.
संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी. इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया और प्रावधान किया गया कि इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती.
इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है.
दरअसल, 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन करके नौवीं अनुसूची का प्रावधान किया था ताकि भूमि सुधारों को अदालत में चुनौती न दी जा सके.
विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराहट का एक और ऐतिहासिक प्रसंग बीते वर्ष 16 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में दिखा जिसके लिए सभी उत्सुक थे. इस दिन संविधान के 99वें संशोधन 2014 को असंवैधानिक करार देकर निरस्त घोषित किया गया.
इस तरह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून 2014 अस्तित्वहीन हो गया और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रू्व प्रचलित ‘कॉलेजियम प्रणाली’ को जारी रखने का फैसला दिया.
यह फैसला 31 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने दिया. इस फैसले के बाद सरकार फिर सकते में आ गई और विधि मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने जहां इस फैसले पर हैरानी जताई, वहीं वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हुए इसे अनिर्वाचितों की तानाशाही बताया.
ताजे घटनाक्रम में जेटली के बजट सत्र के दूसरे सोपान के आखिरी दिन के बयान ‘विधायिका और कार्यपालिका के कामों में न्यायपालिका का दखल बढ़ रहा है. केंद्र सरकार का काम सिर्फ बजट बनाना और टैक्स लेना रह गया है’ से ऐसा लगता है कि न्यायपालिका की दखलंदाजी से सरकार नाखुश है.
उत्तराखंड का घटनाक्रम, दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार को फटकार, सूखे पर सर्वोच्च अदालत की लताड़, जेएनयू विवाद में राजद्रोह के आरोप पर सवाल यानी हर बार निशाने पर सिर्फ सरकार!
कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और लोकोपयोगी बनाने की पूरी जिम्मेदारी सरकारों की होती हैं. इसके लिए उसके पास पर्याप्त अधिकार और पूरा तंत्र होता है. लेकिन जब इसमें ही सरकारें नाकाम होने लगती हैं तो अंततोगत्वा उसी कानून को अपना डंडा चलाना पड़ना है जिसका अधिकार हमारे उसी संविधान ने दिया है जिसकी पवित्रता और सर्वोच्चता की शपथ को अपने लोकतंत्र के संस्कार और गरिमा समझते हैं.
न्यायपालिका भी तो इसी गरिमा के ‘चीरहरण’ को रोकने के लिए कड़े फैसले सुनाती है और वह भी अपनी सीमाओं में रहकर. इसके बाद भी यदि राजनीतिज्ञ इसे टकराहट कहें तो यह दुनिया के सबसे लोकतंत्र के साथ कैसा इंसाफ?