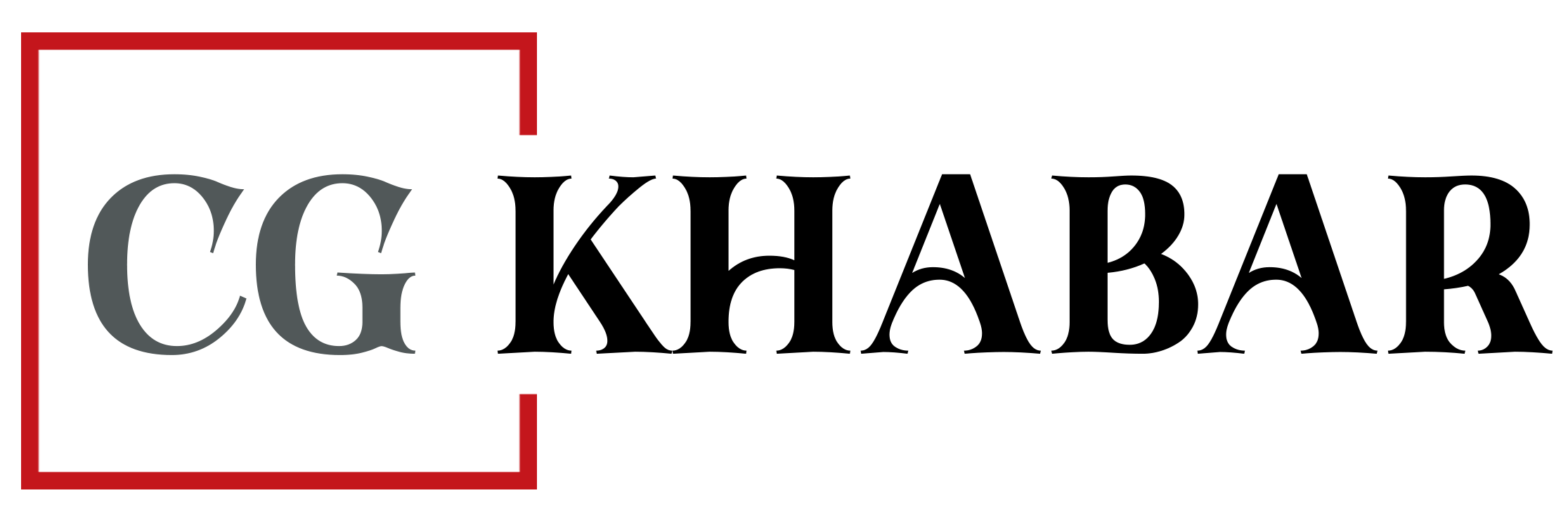इतिहास के आयने में डोली
‘चलो रे डोली उठाओ कहार..पिया मिलन की ऋतु आई…’ यह गीत जब भी बजता है, कानों में भावपूर्ण मिसरी सी घोल देता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें छिपी है किसी बहन या बेटी के उसके परिजनों से जुदा होने की पीड़ा के साथ-साथ नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की अपार खुशी! जुदाई की इसी पीड़ा और मिलन की खुशी के बीच की कभी अहम कड़ी रही ‘डोली’ आज आधुनिकता की चकाचौंध में विलुप्त सी हो गई है जो अब ढूढ़ने पर भी नहीं मिलती.
एक समय था, जब यह डोली बादशाहों और उनकी बेगमों या राजाओं और उनकी रानियों के लिए यात्रा का प्रमुख साधन हुआ करती थी. तब जब आज की भांति न चिकनी सड़कें थीं और न ही आधुनिक साधन. तब घोड़े के अलावा डोली प्रमुख साधनों में शुमार थी. इसे ढोने वालों को कहार कहा जाता था.
दो कहार आगे और दो ही कहार पीछे अपने कंधो पर रखकर डोली में बैठने वाले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे. थक जाने की स्थिति में सहयोगी कहार उनकी मदद भी करते थे. इसके लिए मिलने वाले मेहनताने व इनाम इकराम से कहारों की जिंदगी की गाड़ी चलती थी. यह डोली आम तौर पर दो और नामों से जानी जाती रही है.
आम लोग इसे ‘डोली’ और खास लोग इसे ‘पालकी’ कहते थे, जबकि विद्वतजनों में इसे ‘शिविका’ नाम प्राप्त था. राजतंत्र में राजे रजवाड़े व जमींदार इसी पालकी से अपने इलाके के भ्रमण पर निकला करते थे. आगे आगे राजा की डोली और पीछे-पीछे उनके सैनिक व अन्य कर्मी पैदल चला करते थे.
कालांतर में इसी ‘डोली’ का प्रयोग शादी विवाद के अवसर पर दूल्हा-दूल्हन को ढोने की प्रमुख सवारी के रूप में होने लगा. उस समय आज की भांति न तो अच्छी सड़कें थीं और न ही यातायात के संसाधन. शादी विवाह में सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी और दूल्हा-दूल्हन के लिए ‘डोली’ का चलन था. शेष बाराती पैदल चला करते थे.
कई-कई गांवों में किसी एक व्यक्ति के पास डोली हुआ करती थी, जो शान की प्रतीक भी थी. शादी विवाह के मौकों पर लोगों को पहले से बुकिंग के आधार पर डोली बगैर किसी शुल्क के मुहैया होती थी. बस ढोने वाले कहारों को ही उनका मेहनताना देना पड़ता था.
यह ‘डोली’ कम वजनी लकड़ी के पटरों, पायों और लोहे के कीले के सहारे एक छोटे से कमरे के रूप में बनाई जाती थी. इसके दोनों तरफ के हिस्से खिड़की की तरह खुले होते थे. अंदर आराम के लिए गद्दे बिछाए जाते थे. ऊपर खोखले मजबूत बांस के हत्थे लगाए जाते थे, जिसे कंधों पर रखकर कहार ढोते थे.
प्रचलित परंपरा और रश्म के अनुसार शादी के लिए बारात निकलने से पूर्व दूल्हे की सगी संबंधी महिलाएं डोल चढ़ाई रश्म के तहत बारी-बारी दूल्हे के साथ डोली में बैठती थी. इसके बदले कहारांे को यथाशक्ति दान देते हुए शादी करने जाते दूल्हे को आशीर्वाद देकर भेजती थी. दूल्हे को लेकर कहार उसकी ससुराल तक जाते थे.
इस बीच कई जगह रुक-रुक थकान मिटाते और जलपान करते कराते थे. इसी डोली से दूल्हे की परछन रस्म के साथ अन्य रस्में निभाई जाती थी. अगले दिन बरहार के रूप में रुकी बारात जब तीसरे दिन वापस लौटती थी, तब इस डोली में मायके वालों के बिछुड़ने से दुखी होकर रोती हुई दुल्हन बैठती थी और रोते हुए काफी दूर तक चली जाती थी. उसे हंसाने व अपनी थकान मिटाने के लिए कहार तमाम तरह की चुटकी लेते हुए गीत भी गाते चलते थे.
विदा हुई दुल्हन की डोली जब गांवों से होकर गुजरती थी, तो महिलाएं व बच्चे कौतूहलवश डोली रुकवा देते थे. घूंघट हटवाकर दुल्हन देखने और उसे पानी पिलाकर ही जाने देते थे, जिसमें अपनेपन के साथ मानवता और प्रेम भरी भारतीय संस्कृति के दर्शन होते थे. समाज में एक-दूसरे के लिए अपार प्रेम झलकता था जो अब उसी डोली के साथ समाज से विदा हो चुका है.
डोली ढोते समय मजाक करते कहारों को राह चलती ग्रामीण महिलाएं जबाव भी खूब देती थीं, जिसे सुनकर रोती दुल्हन हंस देती थी. दुल्हन की डोली जब उसके पीहर पहुंच जाती थी, तब एक रस्म निभाने के लिए कुछ दूर पहले डोली में दुल्हन के साथ दूल्हे को भी बैठा दिया जाता था. फिर उन्हें उतारने की भी रस्म निभाई जाती थी. इस अवसर पर कहारों को फिर पुरस्कार मिलता था.
यह भी उल्लेखनीय है कि ससुराल से जब यही दूल्हन मायके के लिए विदा होती थी, तब बड़ी डोली के बजाय खटोली (छोटी डोली) का प्रयोग होता था. खटोली के रूप में छोटी चारपाई को रस्सी के सहारे बांस में लटकाकर परदे से ढंक दिया जाता था. दुल्हन उसी में बैठाई जाती थी. इसी से दुल्हन मायके जाती थी. ऐसा करके लोग अपनी शान बढ़ाते थे. जिस शादी में डोली नहीं होती थी, उसे बहुत ही हल्के में लिया जाता था.
तेजी से बदलकर आधुनिक हुए मौजूदा परिवेश में तमाम रीति-रिवाजों के साथ डोली का चलन भी अब पूरी तरह समाप्त हो गया. करीब तीन दशक से कहीं भी डोली देखने को नहीं मिली है. अत्याधुनिक लक्जरी गाड़ियों के आगे अब जहां एक ओर दूल्हा व दूल्हन डोली में बैठना नहीं चाहते, वहीं अब उसे ढोने वाले कहार भी नहीं मिलते.
ऐसा शायद इसलिए, क्योंकि अब मानसिक ताकत के आगे शारीरिक तकत हार सी गई है. दिनभर के रास्ते को विज्ञान ने कुछ ही मिनटों में सुलभ कर दिया है. वह भी अत्यधिक आरामदायक ढंग से. ऐसे में डोली से कौन हिचकोले खाना चाहेगा. ..और कौन चंद इनाम व इकराम के लिए दिनभर बोझ से दबकर पसीना बहाते हुए हाफना चाहेगा.
कभी डोली ढोने का काम करते रहे सत्तर वर्षीय सोहन, साठ वर्षीय राम आसरे, व बासठ वर्षीय मुन्नर तथा साठ वर्षीय बरखू का कहना है कि अच्छा हुआ जो डोली बंद हो गई, वरना आज ढोने वाले ही नहीं मिलते. अब के लोगों को जितनी सुख सुविधाएं मिली हैं, उतने ही वे नाजुक भी हो गए हैं.
ऐसे में डोली ही नहीं, तमाम अन्य साधनों व परंपराओं का अस्तित्व इतिहास बनना ही है.